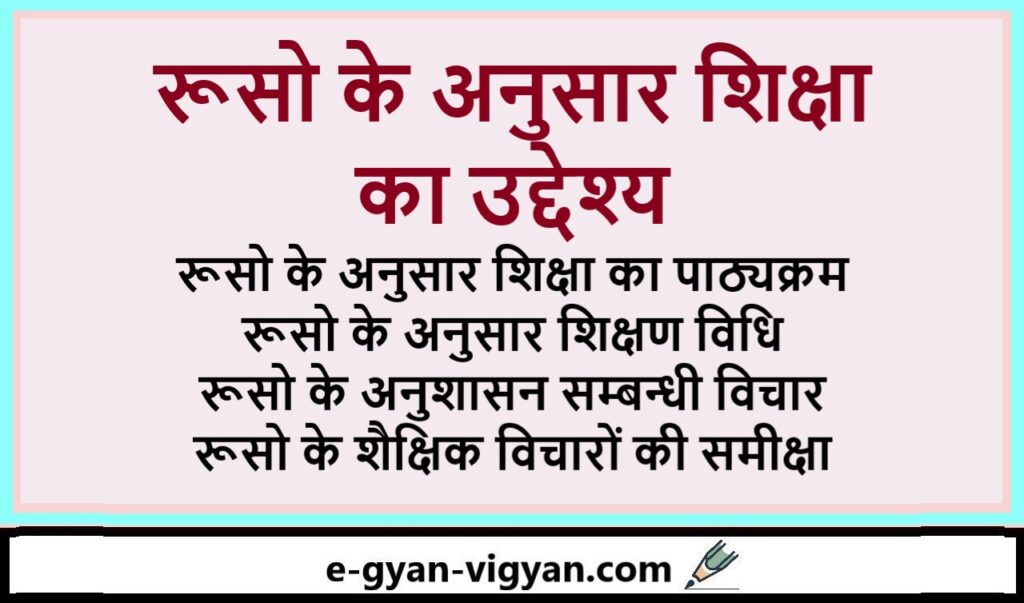
रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य | रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम | रूसो के अनुसार शिक्षण विधि | रूसो के अनुशासन सम्बन्धी विचार | रूसो के शैक्षिक विचारों की समीक्षा | The purpose of education according to Rousseau in Hindi | Curriculum of Education according to Rousseau in Hindi | Method of teaching according to Rousseau in Hindi | Rousseau’s Disciplinary Thoughts in Hindi| A review of Rousseau’s educational ideas in Hindi
रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य
रूसो व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थक था; अतः उसने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के ऊपर अधिक बल दिया है। रूसो के समय में शक्ति मनोविज्ञान तथा बालक को लघु प्रौढ़ मानकर चलने वाले विचार प्रचलित थे। इन्हीं विचारों के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। किन्तु रूसो ने तत्कालीन प्रचलित शिक्षा का विरोध किया और शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम को बालक के विकास की अवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया। उसने शिक्षा के जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया वे निम्नलिखित हैं-
- शारीरिक विकास- रूसो के अनुसार व्यक्ति के आन्तरिक अंगों तथा शक्तियों के स्वाभाविक विकास में योगदान करना शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है। रूसो ने यह उद्देश्य शैशवावस्था (जन्म से 5 वर्ष तक) की शिक्षा के लिए निर्धारित किया है। उसका विचार है कि शिशु को लघु-प्रौद्ध समझकर प्रौद्धों की भाँति शिक्षा नहीं देना चाहिए। शैशवावस्था में बालक के अंग-प्रत्यंग इतने कोमल होते हैं कि उससे प्रौढ़ों का कार्य नहीं लिया जा सकता। अतएव उन्हें खेल-कूद, व्यायाम आदि का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिसमें उनका उचित शारीरिक विकास संभव हो सके। बालक जब स्वस्थ और बलवान होगा तो वह कोई भी दुराचर्ण नहीं करेगा।
- इन्द्रिय प्रशिक्षण- शैशवावस्था के पश्चात् बाल्यावस्था आती है। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष तक रहती हैं। इस अवस्था के लिए रूसो ने शिक्षा का उद्देश्य-ज्ञानेन्द्रियों का विकास करना बतलाया है। इस अवस्था में उसकी शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों का उचित प्रयोग करना सीख सके। इस सम्बन्ध में रूसो ने लिखा है-“शरीर को व्यायाम कराओ, अंगों और ज्ञानेन्द्रियों को अभ्यास कराओ किन्तु आत्मा को जितनी देर तक हो सके आराम करने दो।”
- उपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान- बालक के विकास की तीसरी अवस्था किशोरावस्था का है जो बारह से पन्द्रह वर्ष तक रहती है। रूसो का मत है कि इस अवस्था तक बालक के शरीर तथा ज्ञानेन्द्रियों का विकास हो सकता है, अतः अब उसकी नियमित शिक्षा प्रारम्भ की जा सकती है। इस अवस्था में बालक को उन बातों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों। शिक्षा प्राप्ति की अवधि में उसे परिश्रम, निर्देश और अध्ययन का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार इस अवस्था की शिक्षा का उद्देश्य बालक को उपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देना है जो कि व्यावहारिक जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उसके काम आ सके।
- भावात्मक विकास- बाल-विकास की चौथी अवस्था युवावस्था है जो पन्द्रह से बीस वर्ष तक रहती है। रूसो के अनुसार इस अवस्था की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का भावात्मक विकास करना है। इस सम्बन्ध में उसका कथन है-“हमने उसके शरीर, ज्ञानेन्द्रियों तथा बुद्धि का विकास कर लिया है, अब उसे केवल हृदय प्रदान करना शेष हैं।” इस प्रकार रूसो इस अवस्था में बालक में सामाजिक, नैतिक और धार्मिक भावनाएँ जाग्रत करना चाहता है।
- जीने की कला का ज्ञान- युवावस्था प्राप्त कर लेने पर ही बालक हमारे सामने पूर्ण प्राकृतिक मानव के रूप में आता है; अतः इस अवस्था में उसे जीवित रहने की कला का ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। “जीवित रहने का तात्पर्य साँस लेने से नहीं वरन् कार्य करने से है। कार्य करना, शरीर के विभिन्न अंगों, ज्ञानेन्द्रियों तथा विभिन शक्तियों का विकास करना एवं उनका उचित प्रयोग करना ही जीवन है।” शिक्षा द्वारा बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना नहीं वरन् सर्वप्रथम पूर्ण रूप से मनुष्य बनाना चाहिए। रूसो ने स्वयं लिखा है- “मैं उसे (एमील को) जीवन-शैली की शिक्षा देना चाहता हूँ।” इस प्रकार जंगल के निवासी एमील को शहरों में रहने के योग्य बनाता है। उसके पश्चात् चाहे वह मजिस्ट्रेट बने, चाहे सिपाही, चाहे पादरी, लेकिन रहेगा वह एक मानव ही।
- वर्तमान सुखों की प्राप्ति- रूसो का विचार है कि बालक को अपने वर्तमान जीवन के सुखों का भरपूर आनन्द उठाने देना चाहिए। उनकी शिक्षा ऐसी न हो जो इस आनन्द में बाधक हो। उसके अनुसार भावी सुखों के लिए वर्तमान के सुखो का बलिदान नहीं करना चाहिए। रूसो ने लिखा है- “हे पितरो! इन अबोध बालकों की उन खुशियों को क्यों छीनते हो जो कि बहुत तेजी से बीत जाने वाली हैं। इन्हें जीवन का आनन्द लेने दो जिससे जब ईश्वर उन्हें बुलावे तो वे जीवन का आनन्द लिए बिना ही न मर जायें।”
- स्वतन्त्रता की प्राप्ति- रूसो स्वतन्त्रता के सिद्धांत का पोषक था। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वालक के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास में सहायता देना है। इसके लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक की स्वाभाविक इच्छाओं, प्रवृत्तियों एवं भावनाओं को स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित होने का अवसर प्रदान करे। उसकी शिक्षा में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक या अन्य किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम
रूसो ने जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण बाल-विकास की आवश्यकताओं के आधार पर किया है, ठीक उसी प्रकार और उसी आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण की भी संस्तुत करता है। उसके पाठ्यक्रमसंबंधी विचार भी हमें उसके प्रसिद्ध ग्रंथ ‘एमील’ से प्राप्त होते हैं। उसने भिन्न-भिन्न अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम का निम्नलिखित स्वरूप निर्धारित किया है-
- शैशवावस्था के लिए पाठ्यक्रम (जन्म से 5 वर्ष तक)- रूसो ने शैशवावस्या में प्रचलित विषयों की शिक्षा को अनावश्यक एवं अनुपयोगी बतलाया है। उसका मत है कि बालक को बालक समझकर शिक्षा दी जाये, ‘छोटा प्रौढ’ समझकर नहीं। उसे प्रौढ़ों के कार्य की शिक्षा देना भारी भूल है। बालक को बालक ही रहने दिया जावे जब तक कि वह स्वयं बड़ा न हो जाय; अतः इस अवस्था में सामान्य विषयों का कोई निश्चित ज्ञान न देकर बालक के शारीरिक विकास एवं ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बालक की शिक्षा में खेलने-कूदने, दौड़ने-धूपने और प्राकृतिक वातावरण का अनुभव कराने वाली क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।
- बाल्यावस्था के लिए पाठ्यक्रम (5 से 12 वर्ष तक)– इस अवस्था की शिक्षा पाठ्यक्रम रूसो की ‘निषेधात्मक शिक्षा’ के सिद्धांत पर आधारित है। अतः बालक को इस अवस्था की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसकी ज्ञानेन्द्रियों के विकास में सहायक हो। ज्ञानेन्द्रियों के उचित विकास एवं प्रशिक्षण के बिना मानसिक विकास की चेष्य करना लाभप्रद न होगा। इसके लिए खेलना-कूदना, तैरना, उठना-बैठना, देखना-सुनना तथा विभिन्न अंगों और ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस अवस्था में उसे पुस्तकों के बोझ से लादकर स्वानुभव द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए।
- किशोरावस्था के लिए पाठ्यक्रम ( 12 से 15 वर्ष तक )– रूसो का विचार है कि किशोरावस्था प्राप्त होने तक बालक के अंग-प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं और उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ विकसित हो जाती हैं; अतः अब उसके मानसिक विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। इस अवस्था में उसे परिश्रम, निर्देश और अध्ययन के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए उसकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विषय, संगीत, ड्राइंग, लकड़ी का काम तथा किसी व्यवसाय को सम्मिलित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसमें परस्पर निर्भरता का अनुमान करने, कर्त्तव्य पालन करने, उत्तरदायित्व को निभाने और सहयोग के साथ कार्य करने की योग्यता का भी विकास करना चाहिए।
- युवावस्था के लिए पाठ्यक्रम ( 15 से 20 वर्ष तक )- इस अवस्था की शिक्षा का उद्देश्य बालक का भावात्मक विकास करना है। इस दृष्टि से उसकी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो उसमें सामाजिक, नैतिक और धार्मिक भावनाओं को जागृत करे। इसके लिए बालक को इतिहास, पौराणिक कथाएँ तथा हितोपदेश की कहानियाँ पढ़ानी चाहिए। इन विषयों के अतिरिक्त इस अवस्था के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला तथा यौन- शिक्षा को भी स्थान दिया जाना चाहिए।
- स्त्री-शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम- रूसो स्त्रियों को पुरुषों की भाँति शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। उसके अनुसार स्त्री-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पुरुष के सुख-साधनों में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई की शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चित्रकारी, संगीत, पाक-विज्ञान और बच्चों के पालन-पोषण की कला आदि को स्थान देना चाहिए। रूसो स्त्रियों को दर्शन, गणित और विज्ञान-जैसे गूढ़ विषयों की शिक्षा देने का समर्थन नहीं करता है।
रूसो के अनुसार शिक्षण विधि
रूसो ने बालक की शिक्षा हेतु जिन शिक्षण-विधियों का जोरदार समर्थन किया है उनमें भी उसकी प्रकृतिवादी विचारधारा की पुष्टि होती है। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं-
- स्वानुभव द्वारा सीखना- रूसो ने पुस्तकीय शिक्षा का घोर विरोध किया है। वह चाहता है कि बालक अपने अनुभव से सब कुछ सीखे। जहाँ तक संभव हो 12 वर्ष की अवस्था तक बालक को यह भी न पता चले कि पुस्तक होती कौन-सी वस्तु है। क्योंकि पुस्तकें हमें उसी वस्तु के विषय में बतलाती हैं जिसे हम नहीं जानते। इस प्रकार पुस्तकीय शिक्षा अस्थायी होती है। स्वानुभव कराने के लिए रूसो वास्तविक वस्तुओं द्वारा शिक्षा देने की पद्धति की संस्तुति करता है।
- करके सीखना- रूसो ने प्रचलित शिक्षा-विधियों का, जिनमें रटने की क्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, विरोध किया है और उसके स्थान पर क्रिया द्वारा सीखने का समर्थन किया है। उसका विचार है कि बालक जो ज्ञान स्वयं करके सीखता है वह अधिक स्थायी एवं उपयोगी होता है। यह बालक की विवेक-शक्ति का विकास करना चाहता है, स्मरण-शक्ति का नहीं।
- अन्वेषण द्वारा सीखना- रूसो का विचार है कि बालक को निर्देश नहीं देना चाहिए अपितु उसके स्थान पर उसे ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह स्वयं सोच-विचार कर अपने अनुभव का परिणाम निकाले। उसका कथन है कि बालक को कुछ सीधे बतलाने की अपेक्षा उसमें जिज्ञासा उत्पन्न की जाय, जिससे वह स्वयं तथ्य को ढूँढ निकाले। इस प्रकार उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। रूसो के इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चलकर ‘स्वयं खोज प्रणाली’ का आविष्कार हुआ।
- निरीक्षण द्वारा सीखना- रूसो शाब्दिक शिक्षा का विरोधी था। उसका कथन है कि बालक व्याख्यान से कुछ भी नहीं सीख सकता। क्योंकि वह शिक्षक के लम्बे-चौड़े भाषणों और व्याख्यानों को पसंद नहीं करता है। बालक के अन्दर जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति पायी जाती है। वह वस्तुओं में अधिक रुचि लेता है। अतएव बालक की जिज्ञासा-प्रवृत्ति को जागृत करके उसे वस्तुओं के निरीक्षण का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए।
इस प्रकार स्पष्ट है कि रूसो पुस्तकीय अथवा शाब्दिक ज्ञान और रटने की विधि का घोर विरोधी था और क्रिया-विधि, अनुभव, निरीक्षण और अन्वेषण की विधि का समर्थक था।
रूसो के अनुशासन सम्बन्धी विचार
रूसो के समय प्रचलित शिक्षा में दमनात्मक अनुशासन का बोलबाला था। उसने इस प्रकार अनुशासन का कड़ा विरोध किया और इसके स्थान पर उसने स्वाभाविक या प्राकृतिक अनुशासन की स्थापना के लिए कहा है। अनुशासन के लिए उसने निम्नलिखित दो सिद्धांत निर्धारित किये-
- स्वतन्त्रतां का सिद्धांत- इस सिद्धांत के अनुसार रूसो मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थक था। उसका विचार था कि अनुशासन के सम्बन्ध में बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पर स्वतन्त्रता का अर्थ स्वच्छन्दता अथवा उच्छृंखलता नहीं है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि बालक अपने ढंग से कार्य करे तथा बिना किसी बाह्य बन्धन के अपना विकास करे। इसके साथ ही साथ वह नियमों और व्यवस्थाओं के अधीन रहना भी सीखे। स्वतन्त्रतापूर्ण परिवेश में बालक के नैसर्गिक गुणों को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। इसमें बालक को आत्मानुभूति एवं आत्म-प्रशासन का अवसर मिलता है जिससे वह बहुत कुछ सीखता है और उसकी इच्छाओं की संतुष्टि होती है। इसके परिणामस्वरूप बालक में आत्म-नियंत्रण की शक्ति उत्पन्न होती है जो आगे चलकर आत्मानुशासन को जन्म देती है।
- प्राकृतिक परिणामों का सिद्धान्त- रूसो का विचार है कि अनुशासन की स्थापना हेतु अथवा बालक द्वारा किसी भी बुरे कार्य के करने पर उसे दण्ड नहीं देना चाहिए। बालकों को अपने बुरे व्यवहार का दण्ड स्वाभाविक परिणाम के रूप में ही मिलना चाहिए। प्रकृति के नियमों में एक क्रम पाया जाता है। सभी को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रकृति द्वारा स्वयं तुरन्त दण्ड मिल जाता है। इस प्रकार स्वाभाविक दंड मिलने पर वे अपने-आप समझ जाते हैं कि कौन-सा कार्य अच्छा है और कौन-सा कार्य बुरा अथवा किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए। रूसो के इस सिद्धांत का पालन हमारी ग्रामीण अशिक्षित स्त्रियाँ तक, करती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गाँवों में एक कहावत प्रसिद्ध है-“ऐ बहिनी, तोहार पुतवा डेंड्रवार डॉकत बा, डेड़बरवा अपुनै सिखाय देई।” अर्थात् एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा कि “हे बहन! तुम्हारा पुत्र दीवाल फाँद रहा है” (कहीं गिर कर चोट न खा जाय) तो दूसरी ने जवाब दिया कि “बहन! रहने दोः दीवाल उसे स्वयं ही सिखला देगी” (गिर कर चोट खायेगा तो स्वयं ही कभी नहीं चढ़ेगा)। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो बालक को अनुशासन की स्थापना के लिए दंड का विरोध करता था और प्राकृतिक परिणामों द्वारा दण्ड में विश्वास करता था।
रूसो के शैक्षिक विचारों की समीक्षा
रूसो के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन करने के लिए हमें उनके गुण-दोषों पर विचार करना होगा। रूसो के विचारों की अनेक विद्वानों ने कड़ी आलोचना की है। किन्तु यह भी सत्य है कि आज की वर्तमान शिक्षा पर रूसो के विचारों का पर्याप्त प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि यदि उसके विचारों में कहीं दोष है तो गुणों की भी कमी नहीं है। इसकी जानकारी के लिए हम सबसे पहले उसके शैक्षिक विचारों की आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में फिर यह देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा पर उसके विचारों का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है।
रूसो के शैक्षिक विचारों में निम्नलिखित दोष दिखाई पड़ते हैं-
(1). ‘प्रकृति’ शब्द के अर्थ में भेद- रूसो प्रकृतिवाद का जन्मदाता कहा जाता है। उसके शैक्षिक विचारों में भी प्रकृतिवाद की ही पूरी छाप दिखलाई पड़ती है। किन्तु उसके ‘प्रकृति’ शब्द के प्रयोग में एकरूपता का नितांत अभाव है। रूसो ने स्वयं ही इस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अर्थों में किया है। एक स्थान पर वह ‘प्रकृति’ का अर्थ ‘सामाजिक प्रकृति’ (समाज का स्वाभाविक रूप) से लगाता है तो दूसरे स्थान पर ‘मनोवैज्ञानिक प्रकृति’ (मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ, योग्यताएँ, क्षमताएँ आदि) से और तीसरे स्थान पर इसका अर्थ ‘बाह्य प्रकृति’ या ‘भौतिक प्रकृति’ के रूप में लेता है। यह एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात है।
(2) परस्पर-विरोधी विचार- रूसो के विचारों में परस्पर विरोध दिखलाई पड़ता है। उदाहरण के लिए एक तरफ तो वह पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है और दूसरी तरफ बाल्यावस्था में ‘राबिन्सन क्रूसो’ नामक पुस्तक पढ़ने की संस्तुति करता है। प्रारम्भ में वह समाज का घोर विरोध करता है और ‘एमील’ को समाज से दूर एकांत में प्रकृति के बीच शिक्षा प्रदान करता है। परन्तु वह उसी ‘एमील’ को किशोरावस्था में भावात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास के लिए समाज में लाता है और समाज के सदस्यों से परिचय कराता है।
(3) समाज-विरोधी- रूसो के शैक्षिक विचार समाज-विरोधी हैं। उसने बालक की शिक्षा में समाज एवं परिवार को कोई महत्व न देकर प्रकृति को ही सब कुछ पाना है। वह बालक ‘एमील’ की शिक्षा समाज से दूर एकांत में करता है। वास्तव में यह उपयुक्त नहीं है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसका सर्वागीण विकास समाज में रह कर ही हो सकता है।
(4) बालकसम्बन्धी ज्ञान दोषपूर्ण- ग्रेब्स तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि रूसो ने बालकों के विकाससम्बन्धी जो विचार प्रकट किये हैं वे अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं। ग्रेब्स ने तो लिखा भी है-“रूसो का बालकसम्बन्धी ज्ञान दोषपूर्ण है।”
(5) स्त्री-शिक्षासम्बन्धी संकीर्ण दृष्टिकोण- रूसो के स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी विचार अत्यन्त ही संकीर्ण और अनुदार हैं। वह स्त्रियों को पुरुषों की भाँति शिक्षा नहीं देना चाहता। उसके अनुसार स्त्री पुरुष की प्रसन्नता का साधन है; अतः उसे केवल ऐसी शिक्षा प्रदान की जाय जिससे वह अपने पति को प्रसन्न रख सके। इसके लिए उसे गृह-विज्ञान, संगीत, कला, स्वास्थ्य-रक्षा आदि की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें विज्ञान, गणित, दर्शन आदि विषयों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यह विचार वर्तमान युग की दृष्टि से अनुपयुक्त है।
(6) निषेधात्मक शिक्षा का दोषपूर्ण सिद्धांत- रूसो का निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धान्त दोषपूर्ण है। क्योंकि यह समाज, परिवार, शिक्षक, शिक्षालय और पुस्तक की पूर्ण अवहेलना करता है और पूर्व संचित अनुभवों को कोई महत्व नहीं प्रदान करता है।
(7) गरीबों के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं- रूसो ने गरीबों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझा है। उसने लिखा है-“गरीबों को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।” उसका यह विचार जनतांत्रिक भावना के प्रतिकूल है।
(8) प्राकृतिक अनुशासन का सिद्धांत दोषपूर्ण- रूसो प्राकृतिक अनुशासन में विश्वास करता है। उसके अनुसार बालक को प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड भोगने दिया जाना चाहिए। किन्तु प्राकृतिक दंड कभी-कभी अत्यन्त भयानक एवं प्राणघातक भी हो सकते हैं; अतएव यह सिद्धान्त उचित नहीं प्रतीत होता।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- व्यक्तित्व का अर्थ | व्यक्तित्व की परिभाषायें | व्यक्तित्व के तत्व या लक्षण | अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएँ
- व्यक्ति के प्रकार या भेद | युंग का वर्गीकरण | आधुनिक वर्गीकरण
- व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक | समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता
- व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ | व्यक्तियों के गुणों के मापन की विधि
- सर सैयद का व्यक्तित्व और कार्य | मुसलमानों के प्रति वैज्ञानिक शिक्षा की सोच
- सर सैयद अहमद का राजनैतिक दृष्टिकोण | Political outlook of Sir Syed Ahmed in Hindi
- अलीगढ आंदोलन | अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में सर सैयद अहमद खां के योगदान
- स्वामी विवेकानन्द का जीवन-वृत्त | स्वामी विवेकानन्द के दार्शनिक विचार | स्वामी विवेकानन्द की शैक्षिक विचारधारा | स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान
- गांधीजी का जीवन-वृत्त | गांधीजी के दार्शनिक विचार | गांधीजी की शैक्षिक विचारधारा | गांधीजी के शिक्षासम्बन्धी अन्य विचार | गांधीजी के शिक्षादर्शन की समीक्षा | शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी का योगदान
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







