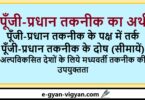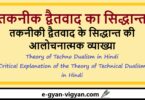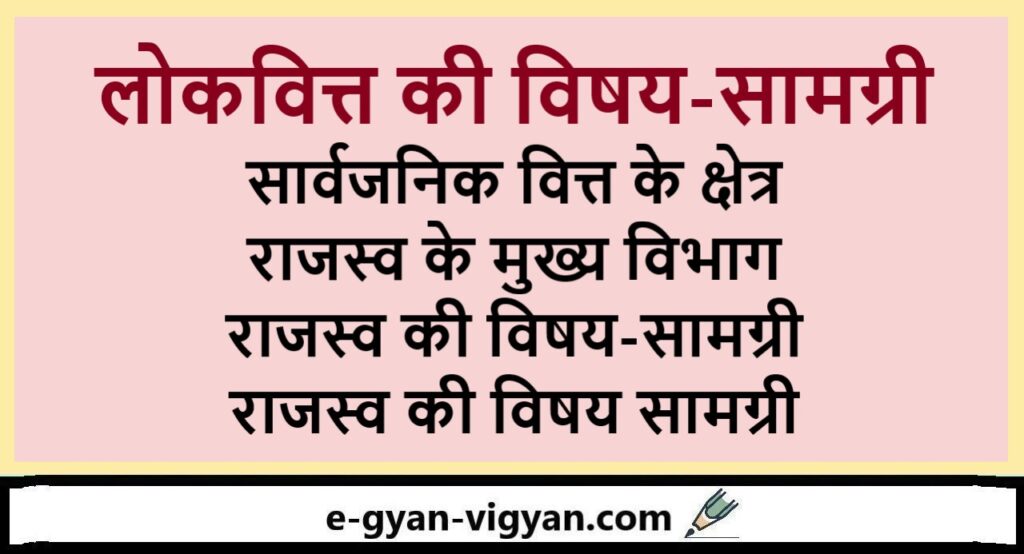
लोकवित्त की विषय-सामग्री | सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र | राजस्व के मुख्य विभाग | राजस्व की विषय-सामग्री | राजस्व की विषय सामग्री
लोकवित्त/राजस्व की विषय-सामग्री (मुख्य विभाग) एवं क्षेत्र
राजस्व का विषय सरकारों की आय और व्यय तथा इनका समायोजन है। अन्य शब्दों में, सरकारों की वित्त-व्यवस्था किस प्रकार होती है इसका अध्ययन राजस्व में किया जाता है। डाल्टन ने राजस्व के क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा है, “राजस्व (लोकवित्त) राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र की सीमा पर स्थित है।” इसका आशय यह है कि सरकार को राज्य का शासन चलाने के लिये एक और राजनीतिशास्त्र में सिद्धान्तों का सहारा लेना पड़ता है तथा दूसरी ओर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिये उसे अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का पालन करना पड़ता है। आधुनिक युग में राजस्व का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा है।
राजस्व के मुख्य विभाग (Main Division)-
हैरोल्ड ग्रोव्ज के अनुसार, “आजकल राजस्व में लोक आय, लोक-व्यय, लोक-ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति सम्मिलित होती है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व की विषय-सामग्री को पाँच भागों में विभाजित किया जाता है-(1) लोक (सार्वजनिक) व्यय, (2) लोक (सार्वजनिक) आय, (3) लोक (सार्वजनिक) ऋण, (4) वित्तीय प्रशासन, (5) आर्थिक स्थायित्व।
(1) लोक-व्यय-
लोक-आय का राजस्व में वही महत्व है जो अर्थशास्त्र में उपयोग का है। जिस प्रकार उपभोग आर्थिक क्रियाओं (उत्पादन, विनिमय तथा वितरण) का आदि और अन्त है उसी प्रकार लोक-व्यय राज्य की अन्य वित्तीय क्रियाओं (लोक-व्यय की प्राप्ति, लोक-ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति) का आदि और अन्त है।
लोक-व्यय के मुख्य विषय- लोक-व्यय के अन्तर्गत निम्न प्रमुख बातों का अध्ययन किया जाता है-(i) किन-किन मदों पर लोक-व्यय होना चाहिये (ii) लोक-व्यय करते समय किन- किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिये, (iii) लोक-व्यय का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (उत्पादन, वितरण, उपयोग, रोजगार आदि) पर क्या प्रभाव पड़ता है, (iv) लोक-व्यय की क्या समस्यायें हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है?
- सार्वजनिक लोकवित्त का अर्थ एवं परिभाषा | राजस्व की परिभाषाएँ
- लोक वित्त की प्रकृति | लोक वित्त विज्ञान है या कला | राजस्व विज्ञान है अथवा कला
लोक-व्यय ‘उद्देश्य’ है। इस कारण सर्वप्रथम यह निश्चय करना पड़ता है कि लोकसत्ता कितना व्यय करना चाहती है। यह निर्णय समाज की महत्वपूर्ण माँगों को देखकर ही किया जाता है।
(2) लोक-आय-
लोक-आय ही वह साधन है जिसके द्वारा साध्य की पूर्ति हो सकती है। यह निर्धारित करने के पश्चात् कि लोकसत्ता को कुल कितना व्यय करना है शासनाधिकारी इस धनराशि को विभिन्न प्रकार के स्रोतों द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।
लोक-आय के मुख्य विषय- इसके अन्तर्गत निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है- (i) सार्वजनिक आय के कौन-कौन से स्रोत हैं? (ii) कर कितने प्रकार के होते हैं? (iii) करारोपण करते समय कौन से सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये ताकि कर-प्रणाली न्यायोचित हो। (iv) करदान क्षमता क्या है तथा इसको निर्धारित करने वाले घटक कौन-से हैं? (v) करापात कराघात एवं कर विवर्त से सम्बन्धित समस्यायें तथा निर्धारित घटक क्या हैं? (vi) कर के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग आदि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इन सब बातों का अध्ययन ही लोक-आय में किया जाता है।
(3) लोक-ऋण-
आजकल सरकार के कार्यों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। सरकार को करों द्वारा इतनी आय प्राप्त नहीं होती जिससे सार्वजनिक व्यय की पूर्ति की जा सके। अतः सरकारों को समय-समय पर देश और विदेश से ऋण लेने पड़ते हैं। कभी-कभी आर्थिक विकास की योजनाओं की पूर्ति के लिये भी ऋण लेने पड़ते हैं।
लोक-ऋण के मुख्य विषय- इसके अन्तर्गत निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है-(i) सरकार को कब और किन कार्यों के लिये ऋण लेने चाहिये? (ii) लोक-ऋण के प्रकार, (iii) आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, (iv) ऋण प्राप्त करने की रीतियाँ, (v) ऋण के भुगतान करने की रीतियाँ, (vi) ऋणों के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
(4) वित्तीय प्रशासन-
आय, व्यय, ऋण एवं ब्याज की प्राप्ति अथवा व्यय की उचित व्यवस्था करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक बजट विभाग होता है जो आगामी बजट तैयार करने तथा उसकी स्वीकृत मदों का नियमित हिसाब-किताब रखने की व्यवस्था करता है। आजकल वित्तीय प्रशासन का महत्व बहुत बढ़ गया है बैस्ट्रेबिल के अनुसार, “हमें केवल विधियों का अध्ययन ही नहीं करना चाहिये बल्कि उन सिद्धान्तों का परीक्षण भी करना चाहिये जिनके अनुसार उन विधियों को अपनाया गया है। जब तक वित्तीय शासन और बजट की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, तब तक वित्त की पुस्तक को पूर्ण नहीं कहा जा सकता।”
मुख्य विषय- (i) बजट का निर्माण, इसका पारित और कार्यान्वित होना, (ii) जनता के सूचनार्थ बजट को प्रकाशित करना, (iii) कर एकत्र करने की व्यवस्था करना, (iv) व्यय व्यवस्था का संचालन करना, (v) लोकवित्त सम्बन्धी लेखों की जाँच अंकेक्षण व नियन्त्रण करना।
(5) आर्थिक स्थायित्व-
लोक वित्त की एक पृथक् साखा के रूप में ‘आर्थिक स्थायित्व’ का विषय अपेक्षाकृत नया है। इसका विकास विशेष रूप से 1930 की महामन्दी के बाद हुआ है। इस शाखा को कार्यात्मक वित्त भी कहते हैं। इस विभाग के अन्तर्गत देश में पूर्ण रोजगार बनाये रखने, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण लगाने और मूल्य उच्चावचनों पर अंकुश लगाने के लिये राज्य की वित्त एवं अन्य समष्टिपरक आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।
आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मुख्य यन्त्र राजकोषीय नीति है। यह नीति देश में उत्पत्ति के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने, उत्पादन क्रियाओं का नियमन करने, राष्ट्रीय आय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाने तथा कीमतों में स्थिरता बनाये रखने में सहायक सिद्ध हुई है।
उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त पाँचों विभाग एक दूसरे से पृथक् न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। फिर, आधुनिक युग में लोक वित्त का क्षेत्र स्थिर न होकर प्रावैगिक रूप धारण कर चुका है जो राज्य के आर्थिक-सामाजिक उत्तरदायित्वों में होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलता रहता है।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- तुलनात्मक लागत सिद्धान्त | तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के लाभ | तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की मान्यताएँ | तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की आलोचनायें | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्दर्भ में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त
- लागत में तुलनात्मक अन्तर का आशय | लागतों में अन्तर के प्रकार | लागतों में पूर्ण या निरपेक्ष अन्तर | लागतों में समान अन्तर | लागतों में तुलनात्मक या सापेक्षिक अन्तर
- तुलनात्मक लागत सिद्धान्त एवं विकासशील देश | तुलनात्मक लागत सिद्धान्त विकासशील देशों में कहाँ तक लागू है?
- हैबरलर का अवसर लागत सिद्धान्त | अवसर लागत सिद्धान्त की मान्यतायें | अवसर लागत सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- पारस्परिक माँग का सिद्धान्त | पारस्परिक माँग का सिद्धान्त की मान्यतायें | मार्शल का प्रस्ताव वक्र | मिल के पारस्परिक माँग सिद्धान्त का महत्व | मिल के सिद्धान्त की आलोचनायें
- व्यापार को शर्ते | वस्तु व्यापार की शर्ते | वस्तु व्यापार की शर्तों की सीमाएं
- सकल वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्ते | व्यापार की आय शर्ते | इसकी आलोचनाएँ
- मुक्त व्यापार सन्धि | Free trade agreement in Hindi (FTA)
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com