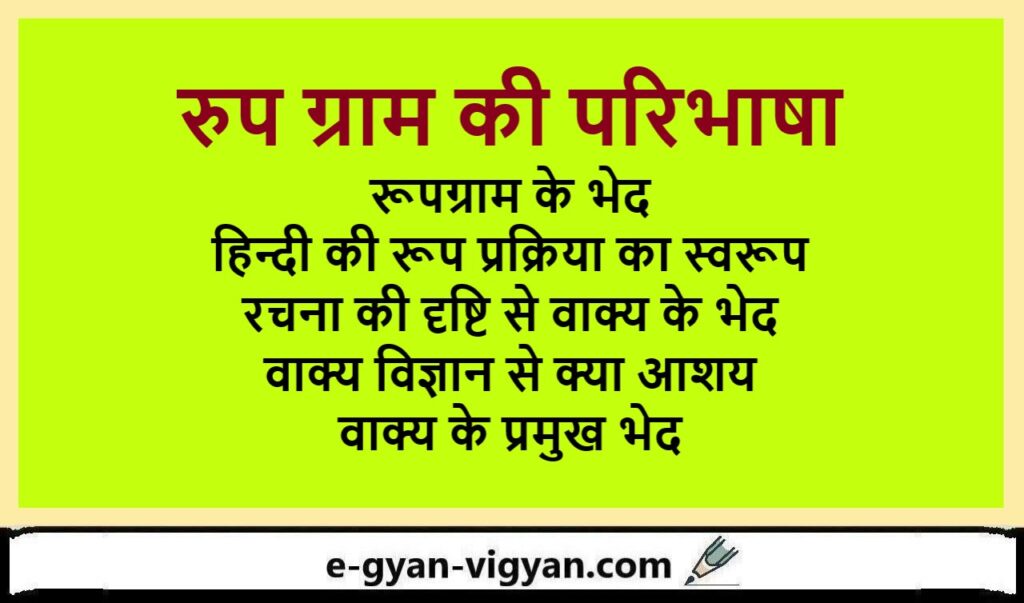
रुप ग्राम की परिभाषा | रूपग्राम के भेद | हिन्दी की रूप प्रक्रिया का स्वरूप | रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद | वाक्य विज्ञान से क्या आशय | वाक्य के प्रमुख भेद
रुप ग्राम की परिभाषा
डा० भोलानाथ तिवारी ने भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को रउपग्रआम कहा है। एक वाक्य जितने पदों से बनता है, उनको तब तक विभाजित किया जाय जब तक उनके विभाजित अंश एक अर्थ स्पष्ट करते रहें। ऐसा सार्थक और लघुतम अंश रूपग्राम कहलाता है। इसे समझने के लिए एक वाक्य लेते हैं-राम के विद्यालय में एक समारोह होगा। इस वाक्य के पाँच रूप पद पर हैं- ‘राम के’, विद्यालय में, ‘एक’, ‘समारोह’ होगा? इन सभी के रूप में विभिन्नता है। राम के’ में ‘के’ परसर्ग है, ‘विद्यालय में’, पद ‘में’ कारक चिन्ह से युक्त है। ‘एक’ में इस प्रकार की कोई भी विभक्ति नहीं है। ‘समारोह’ में सम+आरोह में दो शब्द हैं। अब यदि देखा जाए कि इसमें कौन से रूप ऐसे हैं जिन्हें सार्थकता की दृष्टि से लघुतम रूप में विभाजित किया जा सकता है और कौन रूप ऐसे हैं जिन्हें और विभाजित किया जा सकता है तो हम देखेंगे कि ‘में’ तथा ‘एक’ को तो और विभाजित नहीं किया जा सकता है, पर ‘राम के’, ‘विद्यालय’, ‘समारोह’, ‘होगा’ इन चारों पदों को पुनः इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है-राम + के, विद्या + आलय, सम + आरोह, हो + ग +आ। इस प्रकार इस वाक्य में ग्यारह छोटे-छोटे टुकड़े हैं जिन्हें सार्थक कहा जायेगा। ये ही सार्थक टुकड़े रूपग्राम है।
रूपग्राम के भेद-
हर भाषा में रूप ग्रामों का प्रयोग होता है। इनकी संख्या भाषा में बहुत अधिक होती है। भावों की अभिव्यक्ति के लिये इन रूपों ग्रामों का विशेष महत्व है। रूप ग्राम का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है-
(1) प्रयोग के आधार पर, (2) रचना के आधार पर, (3) अर्थ तत्व एवं सम्बन्ध के आधार पर और (4) खण्डीकरण के आधार पर।
हिन्दी की रूप प्रक्रिया का स्वरूप
संस्कृत की ‘स’ ध्वनि फारसी में ‘ह’ के रूप में पाई जाती है, अतः संस्कृत का सिन्धु रूप फारसी में हिन्दी हो जाता है। प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी या हिन्दवी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में हिन्दी शब्दार्थ हिन्द से सम्बन्ध रखने वाला होता है। हिन्दी शब्द के अतिरिक्त ‘हिन्दु’ शब्द भी फारसी से आया है किन्तु इसका प्रयोग हिन्दी की भाषा का प्रयोग करने वाले के अर्थ में होता है। शब्दार्थ की दृष्टि से हिन्दी शब्द का प्रयोग हिन्दी या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिये हो सकता है। आजकल इसका प्रयोग हिन्दुओं की साहित्यिक भाषा के रूप में होता है।
रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद
डॉ0 कपिल देव द्विवेदी ने वाक्य रचना के दो प्रकार बताये हैं-(1) अन्तःकेन्द्रिक रचना तथा (2) बहिष्केन्द्रिक रचना अन्तः केन्द्रिक रचना यह रचना है जिसका केन्द्र अन्दर हो । इसको अन्तर्मुखी रचना भी कहते हैं। यदि रचना का पद-समूह (वाक्य-खण्ड) उतना ही काम करता है जितना उसके एक या अनेक निकटतम अवयव करते हैं, तो उसे अन्तः केन्द्रक वाक्यांश कहेंगे और ऐसी रचना को अन्तर केन्द्रक रचना कहेंगे। इसके अनेक भेद होते हैं- समवर्गी, आश्रितवर्गी। आश्रितवर्गी के दो भेद हैं-मुख्य और आश्रित।
बहिष्केन्द्रक रचना से तात्पर्य है-जिसका केन्द्र बाहर हो। इसको बर्हिर्मुखी रचना भी कह सकते हैं। यदि रचना का वाक्यांश अपने निकटतम अवयव के अनुरूप न कार्य करता हो तो उसे बहिष्केन्द्री वाक्यांश कहेंगे। यह रचना अन्तः केन्द्रक के विपरीत होगी।
वाक्य विज्ञान से क्या आशय
अथवा
वाक्य के प्रमुख भेद
ध्वनि विज्ञान और रूप विज्ञान के पश्चात भाषा विज्ञान की तीसरी महत्वपूर्ण शाखा वाक्य विज्ञान है। इस शाखा के अन्तर्गत वाक्य की संरचना, उसके आवश्यक उपकरण आदि का मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म अध्ययन होता है। यह अध्ययन करते समय भाषा में वाक्य प्रयोग की स्थिति और उसके अर्थ पर भी विचार किया जाता है।
वस्तुतः विविध पदों से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य विज्ञान के अन्तर्गत वाक्य का पद विन्यास सम्बन्धी अध्ययन एवं विवेचन होता है। वाक्य सार्थक होता है और सार्थक वाक्यों से भाषा की रचना होती है इस प्रकार किसी भी वाक्य के अन्दर दो मुख्य बातें निहित होती हैं जिन्हें हम उद्देश्य और विधेय के रूप में जान सकते हैं। वाक्य के अन्दर जो भाव विशेष निहित होता है अर्थात् जिसके विषय में वाक्य के द्वारा कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं और जिसके द्वारा इस उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे- “राम पुस्तक पढ़ता है।” इस वाक्य के अन्तर्गत किया जाता है जिससे वाक्य की संरचना और उसके अर्थ विशेष को समझने में सरलता रहती है।
वाक्य विज्ञान के अन्तर्गत वाक्य के विभिन्न भेदों का भी अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का आधार वैज्ञानिक होने के कारण वह पूर्ण सुस्पष्ट होता है। वाक्य के भेदों का अध्ययन करते समय जहां क्रिया के आधार पर वाक्य भेदों का अध्ययन किया जाता है वहीं रचना के आधार पर भी वाक्य के भेदों का विवेचन किया जाता है।
इस प्रकार वाक्य विज्ञान के अन्तर्गत वाक्य की रचना, पदों का महत्व, पदान्वय, वाक्य के भेद आदि का सम्यक, सूक्ष्म और पूर्ण अध्ययन एवं विवेचन होता है।
सम्बन्धदर्शी रूपिम
मुख्यतः ग्राम वाक्य में केवल सम्बन्ध तत्व को ही प्रदर्शित करते हैं इन्हें सम्बन्धदर्शी रूपिम कहते हैं। जैसे संस्कृत की सू, औ, जस, अम, औंट, शस्, आदि विभिक्तियाँ तिप्, तस, झि, यस, थ, निप्, वस, यस, ता, साता, झ आदि तिङ्त प्रत्यय आण, व्य, यञ, अञ, ईकक, यते, आदि तद्धित प्रत्यय, झीप, ष्फ, डीषु, चाप, ऊति स्त्री-प्रत्यय आदि, हिन्दी के ने, को से का, में पर आदि पर सर्ग अ, अक्कड़, आ, आइँद, झाऊ, आका, आइत, आड़ी, आला, ओत, ऐत, औता, टी, गा, ता आदि सम्बन्धदर्शी रूपिम है।
मुक्त रूप ग्राम का स्वरूप
मुख्यतः रूप ग्राम पूर्णतया स्वतंत्र अथवा मुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें ‘मुक्त रूप ग्राम कहते हैं। जैसे-मोहन रसोई घर में दूध पीता है। इस वाक्य में ‘मोहन’ और ‘दूध’ सर्वथा स्वतंत्र और मुक्त रूप ग्राम हैं क्योंकि इनका प्रयोग बिना किसी अन्य रूप ग्राम की सहायता के हुआ है। इनके अतिरिक्त ‘रसोई’ और ‘घर’ भी स्वतंत्र रूप ग्राम ही है। क्योंकि इनका प्रयोग भी वाक्यों में स्वतंत्र रूप से हो सकता है- जैसे रसोई बन रही है, घर साफ हो रहा है आदि।
बद्धरूपिम
मुख्य रूप से रूपग्राम अकेले न आकर वाक्य में सदैव किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें ‘बद्ध रूपग्राम’ कहते हैं। जैसे ‘लड़के घरों से निकलकर लड़ाई कर रहे है।’ इस वक्य में ‘लड़के’ में ‘ए’, ‘घरों’ में ‘ओ’, ‘लड़ाई’ में ‘आई’ आदि रूप ग्राम शब्दों से पूर्णतया बद्ध होकर आये हैं। अतएव ये ‘बद्ध रूपग्राम’ कहलाते हैं।
भाषा विज्ञान – महत्वपूर्ण लिंक
- भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाएँ | भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धति | भाषा विज्ञान का वर्णात्मक अध्ययन
- वैदिक भाषा की ध्वन्यात्मक विशेषतायें | स्वनिम भाषा की लघुत्तम इकाई है, कैसे? | स्वन विज्ञान का स्वरूप | स्वन का वर्गीकरण | स्वन के उच्चारणों में कोमल तालु | स्वर गुण
- स्वनिम विज्ञान का स्वरूप | स्वनिम की अवधारणा | अक्षर क्या है? | स्वन लोप क्या है? | स्वनिमिक विश्लेषण
- स्वन (ध्वनि) परिवर्तन के प्रमुख कारण | भाषिक स्वनों के उच्चारण में ओठों के प्रकार्य | सुर एवं बलाघात में अन्तर | अघोष एवं संघोष ध्वनियों में अन्तर
- रूपिम की अवधारणा | रूपग्राम के परिवर्तन के कारण
- रूपिम के विभिन्न प्रकार | रूपिम के प्रकार्यों की विवेचना | रूपग्राम के भेद अथवा रूपिम के भेद
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







