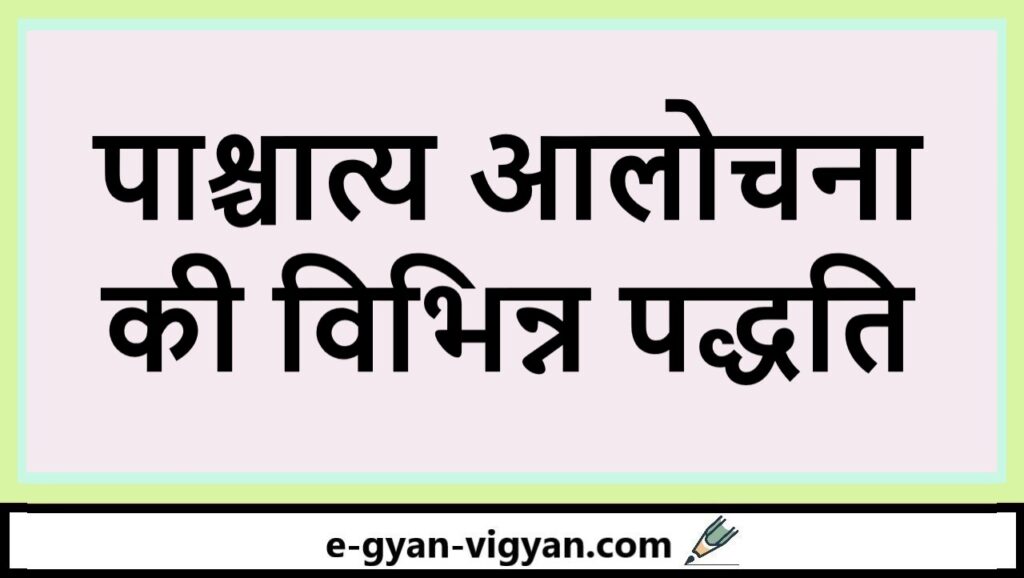
पाश्चात्य आलोचना की विभिन्न पद्धति
पाश्चात्य आलोचना की विभिन्न पद्धति
आत्मप्रधान या प्रभावात्मक आलोचना-
यह आलोचना का बड़ा ही स्वच्छन्द्र रूप है। इसमें आलोचक किन्हीं भी नियमों या सिद्धान्तों में बंधकर चलना नहीं चाहता। वह कृति के अध्ययन के उपरान्त अपने ऊपर पड़े प्रभाव का मौजपूर्वक विश्लेषण करता है। उसकी भावपूर्ण शैली होती है। आलोचना का यह रूप वैयक्तिक होता है। अतः कृति के मूल्य निर्धारण और पाठक के मार्ग निर्देशन एवं ज्ञानसंवर्धन में उसका अधिक योग नहीं रहता। इसमें आलोचना से अधिक रचनात्मक् विशेषताएँ रहती हैं। इसमें कल्पना और भाव-तत्व प्रधानतया कार्य करता है, विचार तत्व कम्। इसे हम एक प्रकार का भावात्मक साहित्यिक निबन्ध कह सकते हैं। यह आलोचना स्वच्छन्द होने से रूचिकर अधिक होती है। कभी-कभी इसमें वागाडम्बर मात्र होता है। उदाहरण नीचे दिया जाता
“वाह रे अन्धे कवि सूरदास, तुमने क्या कमाल किया है। तुमने तह रूप और भाव-सौन्दर्य अपनी बन्द आँखों से देख लिया जो लोग अपनी खुली आँखों से भी नहीं देख पाते। राधा और गोपियों का रंग-बिलास हृदय में एक गुदगुदी पैदा करता है और नटखट राज कृष्ण, तुम धन्य हो। तुम्हारी लीला का पार कौन पा सकता है? यह सब सूर का कमाल है। सूर के काव्य के आगे तो अमृत भी फीका लगता है।”
सैद्धान्तिक आलोचना –
अंग्रेजी में यह स्पेकुलेटिव क्रिटिसिज्म (Speculative Criticism) कहलाती है। इसके अन्तर्गत आलोचक व्यक्तिगत श्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन करते हुए व्यापक सिद्धान्तों की खोज करता रहता है, अतः कृतियों के अध्ययन और व्याख्या द्वारा इस प्रकार के सिद्धांतों को खोजना या उनका संकेत करना सैद्धान्तिक आलोचना है। इस आलोचना के अन्तर्गत सिद्धान और काव्यशास्त्र के प्रन्थ रखे जाते हैं। इसका सम्बन्ध काव्यशास्त्र से माना जाता है। मम्मट का ‘काव्यप्रकाश’, आनन्दवर्धन का ‘ध्वन्यालोक आरिस्टोटिल की ‘पोईटिक्स’, क्रोचे का ‘इस्थिटिक्स’ आदि ग्रन्य इसके अन्तर्गत रखे जाते हैं, परन्तु यदि सिद्धान्त निरूपण ही किसी पुस्तक में हुआ है तो उसे काव्य सिद्धान्त या काव्यशास्त्र के भीतर स्थान मिलना चाहिए, आलोचना के भीतर नहीं। आलोचना के भीतर तो किसी के अध्ययन करते समय सामान्य और व्यापक काव्य-सिद्धान्त की नवीन खोज या पूर्ववर्ती सिद्धान्त का विवेचन या विकास हो सकता है, पर पूरा काव्य-सिद्धान्त निरूपण नहीं, जो कि विवेचना का आधार बनता है, जिसका सम्बन्ध शास्त्र या दर्शन से अधिक है- आलोचना से नहीं। अतः दोनों में अन्तर है। इस आलोचना के द्वारा व्यापक सैद्धान्तिक विकास सम्भव होता है। हिन्दी में पण्डित रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना में हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे “साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है। पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहाँ साहित्य-ग्रन्थों में विवेचन नहीं हुआ है जैसे कोई क्रूर प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या दीन पर क्रोध की प्रबल व्यंजना कर रहा है तो श्रोता या दर्शक के मन में क्रोध का रसात्मक संचार न होगा, बल्कि क्रोध प्रदर्शित करने वाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा आदि का भाव जायेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शील- द्रष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक होगा। पर इसकी रसात्मकता को हम मध्यम कोटि का मानेंगे।
शास्त्रीय या निर्णयात्मक आलोचना –
अंग्रेजी में इसे जुडीशल क्रिटिसिज्म (Judicial Criticism) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत काव्य कला अथवा अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर किसी कृति अथवा रचना की आलोचना की जाती है। सैद्धान्तिक आलोचना का यह विलोम है। यह सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है। सिद्धांतों की कसौटी पर कठोरता से रचना को कसना इसका उद्देश्य है। प्रचलित सिद्धान्तों, जैसे-अलंकार, रस, रीति, ध्वनि, अभिव्यंजनावाद अथवा समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर हमें इस प्रकार की आलोचना पूर्ववर्ती युगों में खूब मिलती है। एक उदाहरण नीचे दिया जाता है –
जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति।
गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति।।
उपुर्यक्त छन्द विशेष ‘दोहा’ के नाम से भाषाकाव्य में प्रसिद्ध है। यह वर्णन स्वकीय नायिका का है। नायक और नायिका के आलम्बन से इसमें शृंगार रस है। सखी की सुनीति से रस की उद्दीप्ति होती है। गुरुजन की लाज से लज्जा संचारी का काम पूरा पड़ता है। प्रियतम की प्रीति से अनुभव की ओर अंगुतिनिर्देश है। नायिका नागर है, यह बात स्पष्ट ही है।
प्रसाद गुण, मधुरा वृत्ति एवं वैदर्भी रीति से दोहा विलसित होता है।
नायिका की सौति, सखी, गुरुजन, प्रियतम आदि अनेक जन अनेक प्रकार से जानते हैं, इस कारण यह उल्लेख अलंकार का प्रथम भेद हुआ।
सखी-सुनीति, प्रीतन- प्रीति में छेकानुप्रास है। नायिका को प्रियजन प्रेममात्र से और अप्रियजन से देखते हैं अर्थात् वह अपने व्यवहार से अनेक लोगों को अनेक गुणों से प्रभावित करती है, वह नागर नायिका है यह व्यंग्यार्थ हुआ। अतः व्यंजना शक्ति और यह अर्थ चमत्कारिक होने से ध्वनि (उत्तम) काव्य हुआ।
व्याख्यात्मक आलोचना-
इसमें न तो व्यापक सिद्धान्तों की कठोरता को ही स्वीकार करते हैं और न किसी गुण की चेतना को ही महत्व देते हैं। इसका प्रमुख ध्येय कृतियों की कवि के दृष्टिकोण में व्याख्या करना है। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक सिद्धान्तों और आदशों की ओर अधिक ध्यान न देकर कवि की अन्तरात्मा में प्रवेश करके उसके आदर्श और दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियों को समझाता है। कवि की प्रवृत्तियों का अध्ययन आधुनिक युग में महत्व का माना जाता है। आचार्य शुक्ल की सूर, तुलसी तथा जायसी सम्बन्धी आलोचनाएँ अधिकांश इसी प्रकार की हैं।
व्याख्यात्मक आलोचना यह स्वीकार करती है कि सभी कवि या साहित्यकार एक श्रेणी या प्रकृति के नहीं होते। अतएव किसी एक सिद्धान्त या नियम से उनको नापना असंगत है और इस बात में यह निर्णयात्मक आलोचना में सर्वथा भिन्न है। इसके अन्तर्गत आलोचक साहित्य को प्रकृति के अन्यृपदार्थो की भाँति विकासशील मानकर नूतन विकास तथा उसके कारणों को खोजने का प्रयास करता है। साहित्य को निर्जीव मानकर पूर्ण प्रतिष्ठित निर्जीव सिद्धान्तों द्वारा ही उसकी परीक्षा नहीं की जाती। साथ ही साथ इसमें व्यक्तिगत या आत्म प्रधान आलोचना का भी रूप नहीं रहता, क्योंकि इसमें आलोचक यह नहीं कहता है कि रचना मुझे कैसी लगी, वरन वह व्यक्तिगत अभिरुचि का परित्याग करके तटस्थ रूप से यह स्पष्ट करता है कि कवि या साहित्यकार ने इसमें क्या अभिव्यक्त किया है। वह उस कृति के परीक्षण में सदैव एक वैज्ञानिक अन्वेषक की भाँति नवीन सिद्धान्त नियम या विशेषताएँ खोजने में सजग रहता है। इस प्रकार व्याख्यात्मक आलोचना में साहित्यकार के साथ पूर्ण न्याय होने के साथ-साथ सजीवता और रोचकता भी बनी रहती है और नवीन नियमों एवं सिद्धान्तों का विकास प्रदान करने वाले तथ्यों की खोज होती रहती है, इसलिए इस आलोचना पद्धति को अधिक महत्व दिया जाता है यह आलोचना सैद्धान्तिक आलोचना का आधार बनती है इसका उदाहरण यह है- ‘जनक के परिताप’ वचन पर उग्रता और परशुराम के बातों के उत्तर में भी लक्ष्मण में जो चपलता हम देखते हैं, उसे हम बार-बार अवसर अवसर पर देखते चले जाते हैं। इसी प्रकार श्रीराम की जो धीरता और गम्भीरता हम परशुराम के साथ बातचीत करने में देखते हैं वह बराबर आगे आने वाले प्रसंगों में हम देखते आते हैं। इतना देखकर हम कहते हैं कि श्रीराम का स्वभाव धीर और गम्भीर था और लक्ष्मण का उम्र और चपल।
अतः इस संचारमात्र के लिए किसी मनोविकार की एक अवसर पर पूर्ण व्यंजना ही काफी है। पर किसी पात्र में उसे शील रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई अवसरों पर उसकी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। रामचरित मानस के भीतर कई ऐसे पात्र हैं जिनके स्वभाव की विशेषता गोस्वामी जी ने कई अवसरों पर प्रदर्शित भावों और आचरणों की एकरूपता प्रत्यक्ष की है।
तुलनात्मक आलोचना-
इसके अन्तर्गत दो या अधिक विभिन्न कवियों की समान विषयावाली रचनाओं की तुलना की जाती है। आलोचक अपने विषय के प्रतिपादनार्थ दोनों ही रचनाओं का अध्ययन कर उनके विविध अंगों पर प्रकाश डालता है। इस कोटि की आलोचना में मूल्य निर्धारण की भावना विद्यमान रहती है। इसके अन्तर्गत अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता है। यह पद्धति उन स्थलों पर उपयोगी होती है जहाँ हमें तुलनात्मक दृष्टि से किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध नहीं करना होता, वरन एक ही प्रकार की विशेषताओं, नियम और सिद्धान्तों के प्रभाव को स्पष्ट करना होता है। इस तथ्य को ध्यान में न रखने पर प्रायः इस आलोचना का परिणाम कटु विवाद होता है। हिन्दी में बिहारी और देव की आलोचना और उस सम्बन्ध में उत्पन्न विवादास्पद स्थिति इसका ज्वलन्त उदाहरण है। शान्तिप्रिय द्विवेदी और शाचीरानी गुर्टू के कुछ लेख इस आलोचना के भीतर आते हैं।
ऐतिहासिक आलोचना-
इसमें कर्ता और कवि की सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन और उनके सहारे रचना का मूल्यांकन किया जाता है। तत्कालीन युग में सामाजिक स्थिति क्या थी। साहित्यिक विचारधारा किस ओर जा रही थी, साथ ही साथ युग विशेष की राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति कहाँ तक सामूहिक रीति से साहित्य पर और उस व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकी, आदि बातों का विवेचन भी ऐतिहासिक आलोचना में रहता है।
सच तो यह है कि जितने भी हमारे प्राचीन कवि या कलाकार हैं, उनको जब तक हम उनके निजी युग के परिस्थितियों के प्रकाश में नहीं देखते तब तक उनका वास्तविक गौरव नहीं समझ सकते। किसी प्राचीन कवि को आज की कसौटी पर कसना और उसके सम्बन्ध में उसी आधार पर कोई निर्णय दे देना और उसे सर्वमान्य समझना, कवि या कलाकार के साथ अन्याय करना होता है। ऐतिहासिक आलोचना में इस प्रकार की सम्भावना नहीं। अतः उसका अपना स्थान है वह महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक आलोचना का किसी भी कवि या कृति के मूल्यांकन में बहुत बड़ा महत्व होता है।
मनोवैज्ञानिक आलोचना–
यह भी बहुत कुछ व्याख्यात्मक है। इसके अन्तर्गत कवि और कलाकार के अन्तस का अध्ययन किया जाता है और काव्य के मूल स्थित भावों और प्रेरणाओं का विश्लेषण इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें बाह्य परिस्थितियों से आन्तरिक भावनाओं पर होने वाली प्रतिक्रिया का विशेष रूप से अध्ययन होता है। कवि की रचनाओं को वैयक्तिक स्वभाव, उसकी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न उसकी प्रतिक्रिया के कोटि की आलोचना का उद्देश्य रहता है। आजकल हिन्दी में कुछ आलोचकों की आलोचनाओं में वैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषणात्मक पुट भी देखने में आने लगा है। व्याख्यात्मक में प्रधानतया कृतित्व का विश्लेषण रहता है और उसमें कवि की रुचि, परिस्थिति और अन्तर्वृत्तियों का ।
हिंदी साहित्य का इतिहास– महत्वपूर्ण लिंक
- हिंदी के जीवनी साहित्य | हिंदी के जीवनी साहित्य के उद्भव और विकास
- ललित निबन्ध और उसकी परम्परा | हिंदी नाटकों का उद्भव और विकास | हिन्दी नाटकों के विकास पर निबन्ध
- आधुनिक हिंदी गद्य की नवीन विधा | आधुनिक हिंदी गद्य की नवीन विधाओं का परिचय
- निबन्धकार के रूप में डॉ० नगेन्द्र | निबन्धकार के रूप में डॉ० नगेन्द्र का मूल्यांकन
- आलोचना का अर्थ | आलोचना विज्ञान है या कला | आलोचना को विज्ञान न मानने के कारण
- हिन्दी आलोचना का विकास | हिन्दी आलोचना का विकास क्रम | हिन्दी आलोचना का उद्भव और विकास
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







