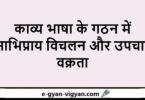कबीर की निर्गुण भक्ति भावना का मूल्यांकन | Evaluation of Kabir’s Nirguna Bhakti spirit in Hindi
कबीर की निर्गुण भक्ति भावना का मूल्यांकन
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का आरम्भ संवत् 1050 से मानकर उसे चार भागों में बाँटा है। उसके दूसरे काल को उन्होंने भक्तिकाल नाम दिया है। भक्ति का विभाजन शुक्लजी ने निर्गुण धारा और सगुण धारा नाम से दो भागों में किया है। बाद में उन्होंने निर्गुण धारा के भी दो भाग किये हैं – ज्ञानमार्गीय शाखा और प्रेममार्गीय शाखा। ज्ञानमार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास माने गये है। ज्ञानमार्गीय कवि ईश्वर को प्राप्त करने का अथवा मुक्ति मिलने का साधन ज्ञान मानते थे। आचार्यों ने ज्ञान को दर्शनशास्त्र से सम्बन्धित माना है। भारतीय दर्शन में जीव, ब्रह्म, माया, मुक्ति आदि के विषय में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनका प्रभाव साधु-संगति के रूप में कबीर पर पड़ा। कबीर ने उन दार्शनिक विचारों को अपनी कविता में स्थान-स्थान पर व्यक्त किया है। कबीर की कविता में प्राप्त होने वाले दार्शनिक विचार सहज ही समझे जा सकते है।
कबीर की दार्शनिक विचार एवं दार्शनिक सिद्धान्त के रूप – कबीर की कविता में प्राप्त होने वाले दार्शनिक विचार अथवा दार्शनिक सिद्धान्त प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं।
(1) ब्रह्म-
भक्ति मार्ग पर चलने वाले ईश्वर को सगुण साकार मानते हैं और उसके अवतारों की लीला का वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं। कबीर ने अपनी कविता में ब्रह्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कबीर का ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों रूपों से परे है –
निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारो ध्यान।
कबीर जिस ब्रह्म का ध्यान करते थे, वह न निर्गुण था और न सगुण था। कबीर ने अपने ब्रह्म को राम के नाम से भी सम्बोधित किया है।
दुलहिनी गावहु मंगलचार।
हम घर आये हो, राजा राम भरतार।
परन्तु कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। राम के साथ राजा विशेषण देखकर सन्देह हो सकता है, इसलिए इस पद के अन्तमें कबीर ने राम शब्द से ब्रह्म का तात्पर्य प्रकट करते हुए कहा है-
लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल।
लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गयी लाल।।
उस सर्वव्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला उसी ब्रह्म के समान हो जाता है। इसी को वेदान्तियों दे ‘सोऽहम्’ कहा है।
जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाने के लिए धागा कहीं बाहर से नहीं लाती, धागा अपने मुँह से निकालती है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी सृष्टि का निर्माण करने के लिए साधन कहीं बाहर से न लेकर अपने में से ही प्रकट करता है। मकड़ी जिस प्रकार जाले के धागे को अपने भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार प्रलय के समय यह सारा विश्व ब्रह्म में लीन हो जाता है। कबीर ने उसे संक्षेप में इस प्रकार कहा है-
आपण माँझे आप छिपाया।
(2) जीव-
फूलचन्द जैन सारंग के अनुसार कबीर के विचार जीव के विषय में इस प्रकार थे-
“कबीर ने अपनी वाणी में अनेक स्थलों पर जीव या जीवात्मा का विश्व निरूपण किया है। यह निरूपण भी अद्वैतवाद से प्रभावित है। कबीर ने अद्वैतवादियों की भाँति आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया है-
बीज मध्य ज्यो बिरछा दरसै, बिरछे मधि छाया।
परमातम में आतम तैसे, आतम मधे माया।।
आतम में परमातम दरसै, परमातम में झाई।
झाई में परछाई दरसै, लखै कबीरा साईं।”
शरीर में रहने वाला यह आत्म-तत्व न तो मनुष्य है, न देव है, न योगी है, न यती है, न अवधूत है, न माता है, न पुत्र है, न उदासी है, न राजा है, न रंक है, न ब्राह्मण है, न बढ़ई है, न तपस्वी है, और न शेख ही है, वह तो उस राम केवल एक अंश-रूप है। यह उसी प्रकार नहीं मिट सकता है। जैसे कागज के ऊपर से स्याही का चिह्न नहीं मिटता अर्थात् यह भी नित्य तथा निर्विकार हैं –
ना इहु मानुस ना यहु देउ। ना यहु जती कहावै सेउ॥
ना यहु जोगी न अवधूता। ना यहु माइ न काहू पूता।।
कहै कबीर यह राम को अंसु। जस कागद पर मिटैन मंसु॥
जीव संसार में जन्म लेकर उसी प्रकार ब्रह्म से अलग हो जाता है, जिस प्रकार बूंद सागर से अलग हो जाती है। मृत्यु के पश्चात् जीव ब्रह्ममें उसी प्रकार मिल जाता है, जिस प्रकार बूंद सागर में मिल जाती है। मृत्यु देखते-देखते ही हो जाती है। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। बूंद को सागर में और जीव को ब्रह्म में समाता हुआ देखकर कबीर आश्चर्य में भरकर कहते हैं-
हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हिराइ।
बूंद समानी समद में, सो कत हेरी जाइ॥
जीव में ब्रह्म के सभी तत्व अथवा विशेषताएँ रहती हैं, यह बात भी कबीर ने स्वीकार की है, क्योंकि जीव ब्रह्म का ही अंश है।
(3) माया-
तुलसीदासजी ने जीव को माया से आविष्ट ब्रह्म कहा हैं ब्रह्म और जीव में तुलसीदास के अनुसार इतना ही अन्तर है कि ब्रह्म माया से सर्वथा पृथक् है और जीव माया से आविष्ट होकर उसी प्रकार विकृत हो गया है, जिस प्रकार धरती पर गिरकर पानी मैला हो जाता है –
भूमि परत आ ढाबर पानी। जिमि जीवहिं माया लपटानी॥
कबीर ने माया को ऐसी नटी के रूप में स्वीकार किया है जो सबका मन मोह लेती है। वह माया बड़ी ठगिनि है। उसने सभी को ठग लिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उससे नहीं बच सके है। कबीर ने इस. माया का ठगिनी रूप जान लिया है –
माया महा ठगिनि हम जानी।
तिरगुन फाँस लिये कर डोले , बोलै मधुरी बानी।
पंडा के मूरति बनि बैठी, तीरथ में भई पानी।
विस्नु कै लछिमी है बैठी, सिब के भवन भवानी॥
कबीर ने माया को रमैया अर्थात् ब्रह्म की दुलहिन कहा है। इसी दुलहिन ने सारा बाजार अर्थात् संसार लूट लिया है। इसने ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को भी नहीं छोड़ा हैं-
रमैया की दुलहिन लूटा बाजार।
ब्रह्मा को लूटा, विस्नू को लूटा, सिवजी के परि गई पिछार।
कबीर सतगुरु की कृपा से माया के चक्कर से बच सके थे, नहीं तो माया उन्हें भी हँसी का पात्र बना देती-
माया ऐसी मोहिनी, जैसे मीठी खाँड।
सतगुरु की किरपा भई, नाहिं तो करती भाँड।
(4) जगत्-
जगत् के विषय में कबीर शंकराचार्य के मायावाद से प्रभावित है। जगत् को शंकराचार्य ने रस्सी मे साँप के भ्रमक के समान माना है। रस्सी न कभी सांप थी, न है और न होगी। इसी प्रकार संसार भी न कभी था, न है और न होगा। कबीर भी जगत् की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते। केवल माया के कारण जगत दृष्टिगोचर होता है। संसार मिथ्या है। नाम और रूप इस पर आरोपित कर दिये गये हैं, इसी कारण उसकी प्रतीति होती है। ब्रह्म ही जगत् का अधिष्ठान है। ब्रह्म से ही जगत् की उत्पत्ति होती है और उसी मे यह जगत् समा जाता है। जिस प्रकार सोने से भिन्न-भिन्न आकार के आभूष्क्षण बनाये जाते हैं और आभूषण रूप में तथा तोड़े जाने पर भी उनमें सोना तो सदा रहता है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते और उसी में समा जाते हैं। पहले का नाम सृष्टि और दूसरे का प्रलय है। कबीर ने जगत् के सम्बन्ध में यह मत निम्नलिखित शब्दों में कहा है-
जैसे बहु कँचन के भूषन, ये कहि गालि तवावहिंगे।
ऐसे हम लोक वेद के बिछुरे, सुन्निहि माँहि समावहिंगे।
कबीर ने पानी और बर्फ के माध्यम से भी संसार के स्वरूप का वर्णन किया है। संसार सृष्टि से पूर्व नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा अर्थात् संसार सृष्टि होने से पूर्व जैसा था, प्रलय के पश्चात् वैसा ही हो जायेगा। बर्फ तो बाद में बनती है, इससे पहले पानी था। बर्फ नष्ट नहीं होती, अपितु पिघलकर पानी हो जाती है। इस प्रकार प्रलय के द्वारा नष्ट कुछ भी नहीं हुआ, पानी ही हमारे पास रह गया –
पाणी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय।
कबिरा जोई था सोई भया, अब कछु कहा न जाय॥
बौद्ध धर्म के समान कबीर भी संसार को दुःखात्मक मानते हैं। यह संसार केवल आपात रमणीय है। ऊपर से देखने में ही यह सुहावना प्रतीत होता है। भोगने पर यह निराशा को जन्म देता है तथा दुःख का कारण बनता है। कंबीर ने संसार और संसारी मनुष्यों का वर्णन सैंवर के फूल औ तोता के माध्यम से किया है-
सेवर सुअना सेइया, दुइ डोंडी की आस।
डोंडी फूटि चटाक दे, सुअना चला निरास॥
इसी प्रकार मनुष्य संसार के पदार्थों के सौन्दर्य को देखकर उनसे सुख की आशा करता है। अन्त में वे सभी पदार्थ सुखहीन सिद्ध होते हैं, तो मनुष्य उनका निराश होकर त्याग कर देता है और उसी दुःख के साथ दुनिया से चला जाता है।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- कबीरदास के पद्यांशों की व्याख्या | कबीरदास के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या
- सूरदास के पद्यांशों की व्याख्या | सूरदास के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या
- जायसी नागमती के पद्यांशों की व्याख्या | जायसी नागमती के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या | सन्देश खण्ड के पद्यांशों की व्याख्या | सन्देश खण्ड के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या
- मीराबाई के पद्यांशों की व्याख्या | मीराबाई के निम्नलिखित पद्यांशों की संसदर्भ व्याख्या
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com