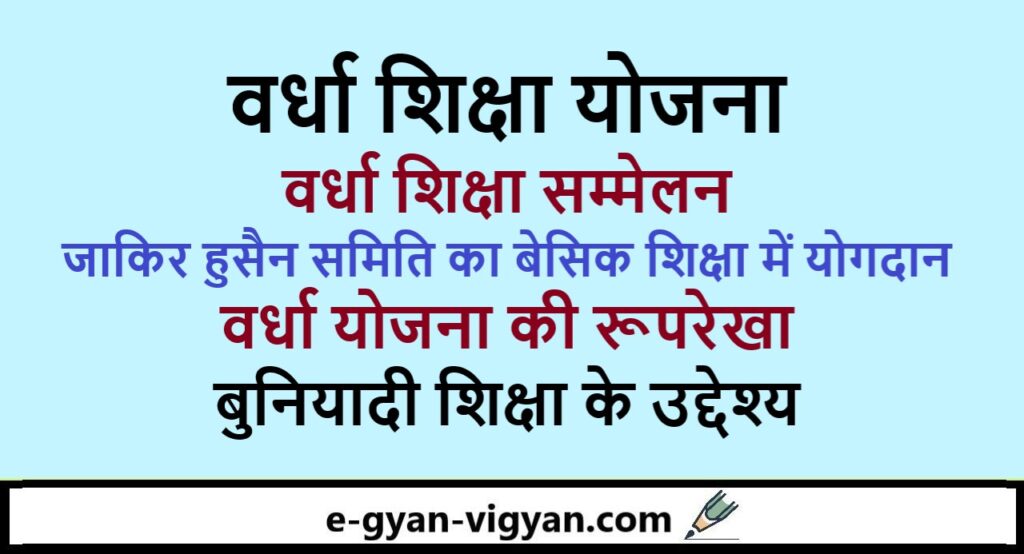
वर्धा शिक्षा योजना | वर्धा शिक्षा सम्मेलन | जाकिर हुसैन समिति का बेसिक शिक्षा में योगदान | वर्धा योजना की रूपरेखा | बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य
वर्धा शिक्षा योजना
वर्धा शिक्षा सम्मेलन (Wardha Educational Conference)
22-23 अक्टूबर सन् 1937 में वर्धा में मारवाड़ी हाईस्कूल का रजत जयन्ती समारोह होने वाला था। इस समय महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा सम्मेलन (इसे अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है) का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात शिक्षाविदों, समाज सुधारकों एवं राष्ट्रीय नेताओं इत्यादि ने भाग लिया।
इस सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने बेसिक शिक्षा की योजना को प्रस्तुत करते हुए कहा है-“देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रकार देश की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है, उससे देश का कर (टैक्स) देने वाला प्रमुख वर्ग विमुख रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात वर्ष का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान प्रदान किया जा सके लेकिन इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए। सर्वतोन्मुखी विकास के उद्देश्य से सम्पूर्ण शिक्षा यथासम्भव किसी उद्योग के द्वारा दी जाये, जिससे पढ़ाई का खर्च अदा हो सके। आवश्यक यह है कि सरकार उन बनाई हुई वस्तुओं को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले।’
इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की नींव डाली गई । इसलिए बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा-योजना भी कहलाती है। गाँधी जी के विचारों का उस सम्मेलन में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों ने स्वागत किया। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये-
(1) शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से प्रदान की जाये।
(2) राष्ट्र के समस्त बालकों को 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये।
(3)7 वर्ष की अवधि में शिक्षा का मध्य बिन्दु किसी प्रकार का हस्तशिल्प हो,जिससे कुछ लाभ हो सके।
(4) बालकों को शिक्षा केन्द्रीय हस्तशिल्प से सम्बन्धित प्रदान की जाये । हस्तशिल्प का चयन बालकों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाये।
(5) हस्तशिल्प केन्द्रित पद्धति से शनैः शनैः शिक्षकों के वेतन का ख़र्च भी निकल जायेगा, यह सम्मेलन ऐसी आशा करता है।
जाकिर हुसैन समिति का बेसिक शिक्षा में योगदान (Contribution of Zakirhusain Committee in Basic Education)
वर्धा शिक्षा सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को स्वीकार करने के उपरान्त इन प्रस्तावों के आधार पर एक व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु डॉ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया डॉ० जाकिर हुसैन के अध्यक्ष होने के कारण इस समिति को जाकिर हुसैन समिति कहते हैं। इस समिति ने गहन विचार-विमर्श करने के उपरान्त दिसम्बर, 1937 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
प्रथम रिपोर्ट में तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों,वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धान्तों,उद्देश्यों,शिक्षक-प्रशिक्षण, विद्यालयों का संगठन एवं प्रशासन, निरीक्षण, परीक्षा-नियमों तथा कताई-बुनाई को प्रमुख हस्तशिल्प मानकर उसके पाठ्यक्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन किया तथा बेसिक शिक्षा की द्वितीय रिपोर्ट में सभी विषयों के पाठ्यक्रमों और हस्तशिल्पों पर ध्यान दिया गया। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि हस्तशिल्पों का अन्य विषयों से सह-सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। जाकिर हुसैन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रथम रिपोर्ट को हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में (फरवरी 1938) प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन ने समिति की प्रथम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यही रिपोर्ट “वर्धा शिक्षा योजना” के नाम से प्रख्यात है तथा बुनियादी शिक्षा का आधार भी है।
इस योजना के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु अप्रैल 1938 में सेवा ग्राम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई। कांग्रेस के मंत्रिमण्डल ने भी इस योजना को अपने-अपने प्रान्तों में लागू करना आरम्भ कर दिया था।
वर्धा योजना (बेसिक शिक्षा योजना) की रूपरेखा (Outline of Wardha Project)
‘वर्धा योजना’ की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई-
(1) इसमें सम्पूर्ण शिक्षा किसी मूलभूत शिल्प से सम्बन्धित होती है।
(2) इस शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि सात वर्ष है।
(3) मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है।
(4) पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा का कोई स्थान नहीं है।
(5) बेसिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य है।
(6) बालकों की योग्यता एवं स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिल्प का चयन किया जाता है।
(7) इस शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है, जिससे बालक सीखे हुये शिल्प द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह कर सकें।
(8) शिल्प की शिक्षा बालकों को इस तरह दी जाती है कि वे उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व से भली-भाँति अवगत हो जाते हैं।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा की समय योजना गाँधी जी के विचारों का ही परिणाम है।
बेसिक या बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Basic Education)
बेसिक या बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
(1) गाँधी जी के अनुसार, “शिक्षा से मेरा आशय बालक तथा मनुष्य का समग्र शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है।” गाँधी जी के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखकर बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि जिससे बालकों की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास ठीक प्रकार से हो सके। इसीलिये इस शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हस्तशिल्प, बागवानी, कला, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों को समाविष्ट किया गया है।
(2) शिक्षार्थियों को देश का उत्तम नागरिक बनाना भी बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु बालकों में विभिन्न गुणों जैसे- देशप्रेम श्रम भावना सहयोग कर्तव्य पालन सदाचार,सत्यवादिता आदि का विकास किया जाता है और इस प्रकार के प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जिससे लोकतान्त्रिक पद्धति के अन्तर्गत बालक अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके।
(3) बुनियादी शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य है-शिक्षार्थियों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना। इसी कारण इस शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षार्थियों की नैतिकता पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। नैतिक शिक्षा के बारे में गाँधी जी का यह कहना था कि-“मैंने हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र के निर्माण को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सभी को समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी आयु एवं पालन-पोषण में कितना अन्तर है।” इसी कथन को ध्यान में रखकर बेसिक शिक्षा का अन्य उद्देश्य बालकों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना निर्धारित किया गया।
(4) यह बुनियादी शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस सम्बन्ध में गाँधी जी का यह कहना था कि मैं भारत में ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता हूँ जिसमें धन के स्थान पर श्रम का महत्व हो, जिसमें प्रेम एवं सहयोग का महत्व हो, घृणा एवं अलगाव का नहीं। इसी कारण बुनियादी शिक्षा बालकों को आत्म बलिदान, सहयोग, अपरिग्रह, त्याग इत्यादि भावनाओं को सिखाती है।
बेसिक शिक्षण विधि (Basic Teaching Method)
बेसिक शिक्षा हस्तकौशल केन्द्रित शिक्षा’ (Craft centred education) मानी जाती है क्योंकि इसमें किसी एक हस्तकला को शिक्षा का केन्द्र मानकर उसके चारों ओर अन्य विषयों को केन्द्रित करके उनकी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस दृष्टि से बेसिक शिक्षा अन्य शिक्षण-विधियों से पृथक है। पूर्व-बेसिक तथा उत्तर बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के अनुसार बेसिक शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत निम्नलिखित ‘शिक्षण-विधियाँ’ (Teaching method) का प्रयोग किया जाता है-
(1) क्रमानुसार शिक्षण विधि (Gradual Teaching Method)- सम्पूर्ण बेसिक शिक्षा सात-क्रमानुसार कक्षाओं’ (Seven gradual classes) में विभक्त है। गाँधीजी ने ‘बाल्यावस्था’ (Childhood) तथा’पूर्व-बेसिक शिक्षा’ (Pre-Basic Education) के महत्व पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि नहीं तालीम यह मानती है कि शिक्षा की इमारत अगर पक्की करनी है तो नींव गहरी होनी चाहिए। घर, स्कूल,एक गाँव के बच्चे के शरीर एवं मन का ‘सर्वांगीण विकास’ (Harmonious development) नागरिकता की पहली तैयारी है। नई तालीम योजना में पूर्व बुनियादी तालीम या बच्चों का शारीरिक पोषण, तन्दुरुस्ती की देखभाल,व्यक्तिगत और सामाजिक तालीम,काम और सेवा की सृजनात्मक व रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, भाषा, कला और संगीत में आत्म प्रकटन, सादा हिसाब,प्रकृति निरीक्षण आदि बच्चों की जिन्दगी से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातें शामिल हैं।” इस पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक समस्त विषयों की क्रमानुसार शिक्षा प्रदान की जाती है।
(2) अनुकरण विधि (Imitation Method)- बालक अपने स्वभाव से ही अनुकरणशील होते हैं और इसलिए वे दूसरों का अनुकरण शीघ्र ही कर लेते हैं। अत: बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत घर, समाज तथा विद्यालय का वातावरण उसके स्वाभाविक विकास के अनुकूल रखने पर विशेष बल दिया जाता है।
(3) सह-सम्बद्ध विधि (Co-relation Method)- बेसिक शिक्षा पद्धति में प्रत्येक विषय को ‘प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण’ (Natural and Social Environment) तथा ‘हस्त-कला’ (Craft) से सम्बन्धित करने का प्रयास किया जाता है। बालक अपनी-अपनी रुचि के अनुसार हस्तकला का चुनाव कर सकते हैं उसी के माध्यम से उन्हें अन्य विषयों को पढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो ज्ञान बालकों को दिया जाये उसका सम्बन्ध उनके ‘व्यावहारिक जीवन’ (Practical Life) से हो और वे उसका व्यावहारिक जीवन में प्रयोग भी कर सकें।
(4) क्रिया-विधि (Activity Method)- बेसिक शिक्षा पद्धति में बालकों को रचनात्मक क्रियाओं का अध्ययन करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। प्रारम्भ में उनसे छोटे-छोटे उपयोगी कार्य कराये जाते हैं। धीरे-धीरे वे खेल-खेल में हस्त-कार्यों में रुचि लेने लगते हैं और इनके माध्यम से वे अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
(5) निरीक्षण विधि (Observation Method)- यद्यपि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत बालक को केन्द्रीय स्थान प्रदान किया जाता है किन्तु बालक कहीं विशेष गलती न कर बैठे इस दृष्टिकोण से शिक्षक द्वारा उनके कार्यों का निरीक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। निरीक्षण विधि की सफलता सुशिक्षित अध्यापकों पर आज निर्भर है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- भारतीय शिक्षा आयोग 1882 | हण्टर आयोग | भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें
- सन् 1905 से 1921 के बीच भारत में शिक्षा संस्थाओं की प्रगति | Progress of Educational Institutions between 1905 to 1921 in India in Hindi
- राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन में गोखले का प्रयास | Gokhale attempts in national education movement in Hindi
- लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति | शिक्षा नीति 1904 का मूल्यांकन | लॉर्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक कार्य | लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष
- 1917 के सैडलर आयोग | भारतीय शिक्षा के विकास पर सैडलर आयोग प्रभाव
- राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन | शिक्षा में स्वदेशी आन्दोलन | ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन की रूपरेखा
- बेसिक शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धान्त | वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धान्त
- बेसिक शिक्षा की समस्यायें | Problems of Basic Education in Hindi
- बेसिक शिक्षा के गुण | बेसिक शिक्षा के दोष | Merits of Basic Education in Hindi | Demerits of Basic Education in Hindi
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







