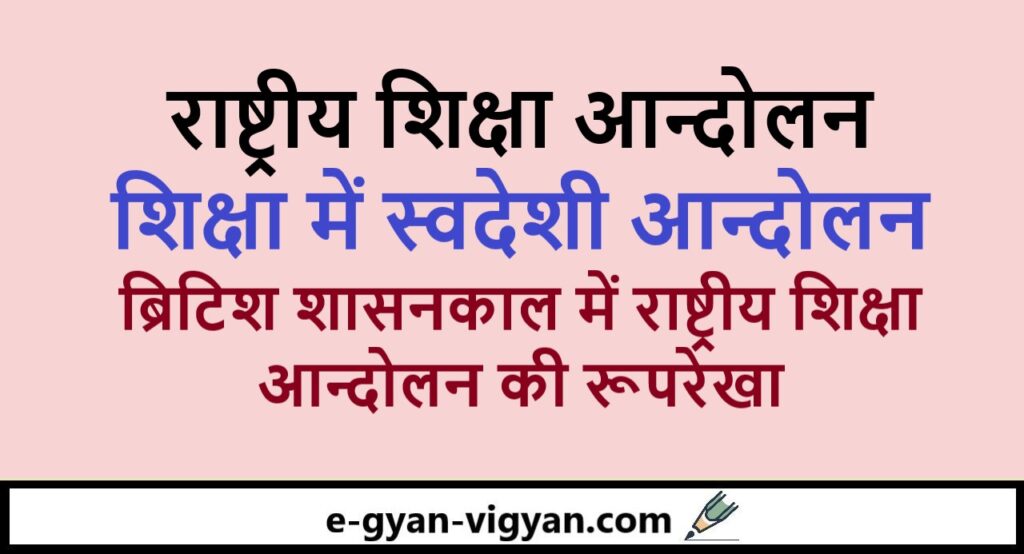
राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन | शिक्षा में स्वदेशी आन्दोलन | ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन की रूपरेखा
राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन (National Education Movement)
1813 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश सरकार से नया आज्ञा-पत्र (Charter Act, 1813) प्राप्त हुआ। इस आज्ञा पत्र से कम्पनी में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद खड़ा हो गया और बड़े मजे की बात यह है कि इस विषय पर भारतीय भी दो खेमों में बँट गए। एक वर्ग के लोग भारत में केवल भारतीय भाषा, साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के पक्ष में थे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में भारतीय भाषा, साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ यूरोपीय भाषा अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य और यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के पक्ष में थे। इनमें से प्रारम्भ में पाश्चात्यवादियों का पलड़ा भारी था। पाश्चात्यवादियों में राजा राम मोहनराय का नाम उल्लेखनीय है।
राजा राम मोहनराय बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। वे भारतीय संस्कृति के पुजारी होने के साथ-साथ पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक थे। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिन्दू कॉलिज’ की स्थापना की। 1819 में इन्होंने कलकत्ता में कलकत्ता विद्यालय समाज’ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने कलकत्ता में 115 ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जिनमें भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा एवं उसके साहित्य तथा यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की गई। राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर श्री जय नारायण घोसाल ने बनारस में ‘जय नरायण स्कूल’ की स्थापना की और उसमें प्राच्य भाषा, साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा, साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की। इसी प्रकार का एक कार्य आगरा में पं० गंगाधर शास्त्री ने किया। उन्होंने उस समय एक लाख पचास हजार रुपयों की एकमुश्त सहायता देकर आगरे के संस्कृत कॉलिज को ‘आगरा कॉलिज’ में बदलवा दिया। दूसरी ओर प्राच्यवादी भी सक्रिय रहे । इनका नेतृत्व किया स्वामी दयानन्द सरस्वती ने।
स्वामी दयानन्द सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने धर्म प्रचार के साथ-साथ हिन्दी भाषा, संस्कृत और संस्कृत साहित्य का प्रचार शुरू किया। उन्होंने यह कार्य 1863 से शुरू किया। ये भारतीयों के लिए भारतीय भाषा, साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की पूरी योजना भी प्रस्तुत की । ये जहाँ भी जाते थे वहीं धर्म प्रचार के साथ-साथ संस्कृत पाठशाला और गुरुकुलों की स्थापना की बात करते थे, हिन्दी का प्रचार करते थे और हिन्दी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की बात करते थे। दयानन्द जी के बाद देश में पुनः पाश्चात्यवादी शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। इस सन्दर्भ में गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर और स्वामी विवेकानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1892 में शिक्षार हेरफेर’ की रचना की और इसमें तत्कालीन शिक्षा के दोष उजागर करने के साथ-साथ अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1901 में शान्ति निकेतन में ‘बहाचर्य आश्रम की स्थापना की । प्रारम्भ में इसमें केवल 4 छात्र थे और गुरुदेव एकमात्र शिक्षक थे। आज यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित है । यह सच्चे अर्थों में विश्वविद्यालय है, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र है, गुरुदेव का कीर्ति स्तम्भ है ।
स्वामी विवेकानन्द का भी इस क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। 1893 में वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गए थे। वे वहाँ के वैभवपूर्ण जीवन को देखकर इस परिणाम पर पहुँचे कि हम भारतीयों के पिछड़ेपन के दो ही मुख्य कारण हैं—एक परतन्त्रता और दूसरा अशिक्षा । वे भारतीयों के लिए सामान्य शिक्षा के पक्षधर के साथ-साथ विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर थे। उन्हें यह जानने और समझने में देर नहीं लगी कि पाश्चात्य देशों की आर्थिक सम्पन्नता का मूल आधार विज्ञान है। इसकी शिक्षा तब अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जा सकती थी। इसलिए इन्होंने राजा राम मोहन राय और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का समर्थन किया। इन्होंने दीन-हीनों की सामान्य शिक्षा के लिए रामकृष्ण मिशन स्कूलों की स्थापना की और साथ ही अंग्रेजी माध्यम के प्राच्य पाश्चात्य दोनों ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। इन्होंने उद्घोष किया कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें आत्मनिर्भर बनाए, हमें अपने पैरों पर खड़ा करे एवं देश के विकास में सहायक हो। इन्होंने वेदान्त दर्शन को जीवन में उतारने का स्तुत्य प्रयास किया। यह देश ही नहीं पूरा संसार उनका चिर ऋणी रहेगा।
शिक्षा में स्वदेशी आन्दोलन (Swadeshi Movement in India)
शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वदेशी आन्दोलन शुरू किया गया। स्वदेशी आन्दोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। शिक्षा में स्वदेशी आन्दोलन से तात्पर्य था कि अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। अनेक राष्ट्रीय विद्यालय तथा संस्थाएँ खोली गईं। इन संस्थाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता एवं भारतीय संस्कृति पर बल दिया गया। दयानन्द ऐंग्लोवैदिक कॉलिज लाहौर, काशी विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विद्यालय, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ,गुजरात विद्यापीठ तथा अनेक अन्य संस्थाएँ स्थापित की गईं। यह संस्थाएँ शिक्षा में स्वदेशी आन्दोलन की प्रतीक हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। इन सभी संस्थाओं में देशी शिक्षा दी जाती थी। कालान्तर में इसी शिक्षा ने राष्ट्रीय शिक्षा का रूप धारण किया। अनेक विद्वान इसे राष्ट्रीय शिक्षा के नाम से ही सम्बोधित करते हैं।
शिक्षा में स्वदेशी आन्दोलन का विकास (1905-1921)
[Development of Swadeshi Movement in Education (1905-1921)]
राष्ट्रीय भावनाओं का विकास एवं शिक्षा
(Development of Nationalism and Education)
उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीय भावना जड़ पकड़ चुकी थी और इस बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही राष्ट्रीय शिक्षा का एक स्वरूप बनना प्रारम्भ हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में काफी जागृति हो चुकी थी। यूरोप के अनेक देशों में भी राष्ट्रीय भावना तथा चेतना का सूर्य उदय हो चुका था। उसका भी भारतीय विचारधारा पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने भी राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया। अत: कुछ राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। एक विद्वान् ने इनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है-
(1) इनका संचालन भारतीयों द्वारा किया जाता था।
(2) प्राचीन परम्पराओं और सभ्यता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता था।
(3) स्कूल-प्रबन्धकों और शिक्षकों में आत्म-त्याग तथा निःस्वार्थ सेवा की भावना थी।
(4) भारतीयों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में कुछ और विषय सम्मिलित कर दिए गए थे।
(5) धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी।
(6) विद्यार्थियों से कम शुल्क लिया जाता था।
(7) आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था।
राष्ट्रीय शिक्षा की माँग (Demand for National Education)
बंगाल के विभाजन के पश्चात् से राष्ट्रीय शिक्षा की माँग बहुत बढ़ गई थी।
स्मरण रहे कि श्रीमती ऐनी बेसेण्ट ने भारतीय शिक्षा के प्रांतीयकरण की अत्यधिक निन्दा करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रीय जीवन एवं राष्ट्रीय चरित्र को निर्बल बनाने के लिए भारतीय शिक्षा पर विदेशी प्रभुत्व से अधिक उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता है। लाला लाजपतराय ने कहा था-
“किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन को बदलने एवं उसके राष्ट्रीय चरित्र का विध्वंस करने के लिए वहाँ के युवकों को विदेशियों द्वारा नियन्त्रित एवं विदेशी विचारधारा की पोषक शिक्षा देना सबसे बड़ा हथियार है।”
गाँधी जी के विचार, गाँधी जी ने भी उस समय की शिक्षा की निन्दा की । एक विद्वान् के अनुसार उन्होंने इसमें निम्न दोष बतलाए-
(1) यह विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इससे पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया गया है।
(2) इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। वास्तविक शिक्षा, विदेशी माध्यम के द्वारा नहीं दी जा सकती है।
(3) इसका एकमात्र उद्देश्य मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है।
(4) यह अन्यायपूर्ण शासन से सम्बन्धित है।
राष्ट्रीय शिक्षा का ढांचा (The Structure of National Education)
प्रथम दो दशकों में जोरदार ढंग से राष्ट्रीय शिक्षा की माँग बढ़ती गई। स्वदेशी शिक्षा (राष्ट्रीय शिक्षा), जिन सिद्धान्तों पर आधारित थी वे इस प्रकार थे-
(1) शिक्षा में स्वदेश प्रेम की भावना- माँग ऐसी थी कि शिक्षा से देश-प्रेम की भावना का विकास हो। श्रीमती ऐनी बेसेण्ट ने तत्कालीन शिक्षा-पद्धति को सर्वथा अनुपयुक्त ठहराते हुए लिखा था, “छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनमें स्वदेश-प्रेम की भावना प्रस्फुटित हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला-कौशल और राजनीति आदि को सम्मिलित किया जाए।”
(2) अंग्रेजी का अन्त- गाँधी जी ने लिखा था अंग्रेजी का अध्ययन केवल व्यावसायिक और राजनैतिक काम के लिए किया जाता था। मनुष्य अच्छा राजपद और स्त्रियां उत्तम वर प्राप्त करने के विचार से अंग्रेजी का अध्ययन करते थे। समाज में अंग्रेजी का घुन लग गया था और यह दासता एवं पतन का प्रतीक था। साहित्य में रुचि रखने वाले भारतीय अंग्रेजी का अध्ययन तो करें, परन्तु एक भी भारतीय को अपनी मातृभाषा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
(3) पाश्चात्य विज्ञानों तथा पाश्चात्य ज्ञान का अध्ययन-भारतीय नेता पाश्चात्य सभ्यता, भाषा और विज्ञान के अध्ययन के विरुद्ध नहीं थे। लाला लाजपतराय का मत था, “यूरोपियन भाषाओं, साहित्य और विज्ञानों के अध्ययन को भारत में प्रोत्साहन न देना मूर्खता और पागलपन होगा। अभी हमें उनका यथेष्ठ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है।”
(4) दास्य भावनाओं का अन्त- अंग्रेजी शिक्षा में दास्य-भावना की झलक थी। ऐनी बेसेंट ने कहा, ‘ऐसी शिक्षा इंग्लैण्ड के लिए ठीक हो सकती है, भारत के लिए नहीं। भारत के लिए भारतीय आदर्श ही उचित हैं। ईश्वर ने भारत जैसी विशाल एवं अद्वितीय राष्ट्रीयता के अलावा इस संसार में अन्य कोई राष्ट्रीयता नहीं बनाई।
(5) व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाये- अंग्रेजों ने देश के आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। नेतागण चाहते थे कि देश का आर्थिक विकास हो और उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा हो । परन्तु इस विषय पर नेता लोग एकमत नहीं हो सके।
(6) शिक्षा पर भारतीय नियन्त्रण हो- भारतीय नेता तथा सुधारक हमारी शिक्षा पर इंग्लैण्ड का नियन्त्रण नहीं चाहते थे। स्वदेशी शिक्षा के महत्त्व पर बल देते हुए श्रीमती ऐनी बेसेंट ने कहा था, “भारतीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसका नियन्त्रण भारतीयों के पास हो, यह भारतीयों द्वारा चलाई जाए तथा भारतीयों के द्वारा ही इसका प्रारूप बनाया जाए। भारतीय धार्मिक भावना से सराबोर होते हुए भी साम्प्रदायिकता से पृथक् रहें और छात्रों के समक्ष भक्ति, ज्ञान एवं नैतिकता के भारतीय आदर्शों को उपस्थित करे।”
राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण (Formation of National Schools)
शिक्षा के स्वदेशीकरण की माँग के फलस्वरूप राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन जोर पकड़ता गया। असहयोग आन्दोलन के मध्य विद्यार्थियों ने विद्यालयों का बहिष्कार किया। इसलिए नेताओं ने अपनी संस्थाएं बनाईं । मौलाना मुहम्मद अली ने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। 1925 ई० में यह विद्यालय दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसी प्रकार के अन्य संस्थान यथा बिहार विद्यापीठ,काशी विद्यापीठ,बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और अन्य प्रकार के अनेक राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना की गई।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य गुण | उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के दोषों
- बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था | बौद्धकालीन शिक्षण विधियाँ
- बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य | बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ
- बौद्धकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य | Important facts of Buddhist education in Hindi
- शिक्षा में छनाई सिद्धान्त | शिक्षा में निस्यन्दन सिद्धान्त | Filtering Principles in Education in Hindi | Dissertation Principles in Education in Hindi
- एडम की रिपोर्ट | एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना | एडम की रिपोर्ट का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन
- लाभ वुड का घोषणा पत्र 1854 | वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें | वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन
- भारतीय शिक्षा आयोग 1882 | हण्टर आयोग | भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें
- सन् 1905 से 1921 के बीच भारत में शिक्षा संस्थाओं की प्रगति | Progress of Educational Institutions between 1905 to 1921 in India in Hindi
- राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन में गोखले का प्रयास | Gokhale attempts in national education movement in Hindi
- लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति | शिक्षा नीति 1904 का मूल्यांकन | लॉर्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक कार्य | लॉर्ड कर्जन के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







