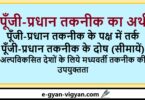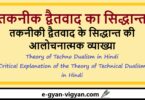भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण | भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क | बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क | राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वाणिज्य बैंकों की स्थिति | राष्ट्रीयकरण का मूल्यांकन | भारतीय बैंकिंग प्रणाली की प्रमुख समस्या
भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण
किसी देश के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान होत है क्योंकि राष्ट्रीय बचत की अधिकांश भाग जमा के रूप में उसके पास इकट्ठा होता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में इन संस्थाओं का महत्व और बढ़ जाता है। भारत बैंकिंग प्रणाली की दोषपूर्ण नीतियाँ एवं उनकी कार्यप्रणाली में अनेक प्रकार की कमियाँ होने के कारण इनके राष्ट्रीयकरण की माँग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही की जा रही थी। राष्ट्रीयकरण की इस मांग के परिणामस्वरूप ही 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का तथा 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। अन्य व्यवसायिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति अपनाई गई। लेकिन सामाजिक नियंत्रण की यह नीति असफल रही। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की लगातार माँग को ध्यान में रखकर ही 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके देश के प्रमुख 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं-
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
- बैंक आफ इण्डिया,
- पंजाब नेशनल बैंक,
- बैंक ऑफ बड़ौदा,
- यूनाइटेड कामर्शियल बैंक,
- केनरा बैंक,
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया,
- देना बैंक,
- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,
- इलाहाबाद बैंक,
- सिन्डीकेट बैंक,
- इण्डियन ओवरसीज बैंक,
- इण्डियन बैंक,
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
15 अप्रैल सन् 1980 को 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में इन बैंकों के शेयर होल्डरों को मुआवजा देने की व्यवस्था थी जिसे कि किस्तों में दिया जाना था।
भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क-
भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जोरदार स्वागत किया गया और यह आशा की गई कि वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो राष्ट्रीयकरण से पहले नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अग्रलिखित तर्क दिए गये हैं-
(1) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा- जनता अपनी बचतों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैंकों में जमा करती है लेकिन बैंकों द्वारा इस जमा को कभी-कभी दुरुपयोग करने के कारण कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि बैंकों को अपना कार्य बन्द करना पड़ता था और जनता का पैसा डूब जाता था। राष्ट्रीकरण से जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हो सकेगी।
(2) आर्थिक सत्ता का संकेन्द्रण- बैंकों का निजी स्वामित्व में रहना बड़े उद्योगों व बैंकों में गठबन्धन को प्रोत्साहित करता है। उद्योगपति बैंकों पर अधिकार जमा कर बैंकों के साधनों का अपने उद्योगों के लिए प्रयोग करने लगते हैं। इससे आर्थिक शक्ति कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है। राष्ट्रीयकरण से इसे रोका जा सकता है।
(3) आर्थिक विकास में सहयोग- बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के आर्थिक विकास के अनुरूप ही बैंक की नीतियाँ बनायी जा सकेंगी और देश का विकास होगा।
(4) बैंकिंग सेवाओं का नियोजित विकास- राष्ट्रीयकरण से देश में बैंकिग व्यवस्था का समुचित रूप से विकास किया जाएगा। ग्रामीण तथा छोटे-छोटे कस्बों में भी बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क-
कुछ लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। इसके लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गये हैं-
- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को व्यावसायिक बैंकों के नियंत्रण के सम्बन्ध में पहले से बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त है अर्थात बैंक की स्थापना, निरीक्षण तथा उनके विस्तार के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को काफी अधिकार प्राप्त है। अतः राष्ट्रीयकरण उचित नहीं है।
- व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इनकी कुशलता में कमी आयेगी। इस प्रकार का तर्क जीवन बीमा निगम तथा अन्य राजकीय संस्थाओं की कुशलता को देखते उचित प्रतीत होता है।
- कुल जमा का बहुत बड़ा भाग पहले से ही राजकीय क्षेत्र (स्टेट बैंक के पास) विद्यमान है। अतः यह तर्क कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को बड़ी मात्रा में धन आर्थिक विकास की योजनाओं में विनियोग करने के लिए उलब्ध हो सकेगा, निराधार प्रतीत होता है।
- यह कहना भी सत्य नहीं है कि व्यावसायिक बैंक केवल अपने संचालकों तथा इनसे सम्बन्धित कम्पनियों को ही कर्ज तथा अग्रिम प्रदान करते हैं। 1986 में निजी क्षेत्र के 20 प्रमुख अनुसूचित बैंकों के कुल जमा धन का केवल 11 प्रतिशत भाग संचालकों को तथा इनसे सम्बन्धित कम्पनियों में था जबकि राजकीय क्षेत्र के बैंकों द्वारा 26% भाग उनके संचालकों तथा उनसे सम्बन्धित कम्पनियों को दिया गया था।
- राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य छोटे किसानों, उत्पादकों तथा निर्यातकर्ताओं के लिए बैंक के दरवाजे खोलना है, परन्तु यह संदेहपूर्ण बताया जाता है कि ये लोग बड़ी संख्या में इन दरवाजों में घुस पायेंगे और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे।
राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वाणिज्य बैंकों की स्थिति-
भारत के प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है-
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय 1969 में बैंकों के कार्यालयों की कुछ संख्या 8321 थी जो 30 जून, 1984 को बढ़कर 40705 हो गयी है।
- राष्ट्रीयकरण से बड़े-बड़े व्यावसायियों के अतिरिक्त किसानों, लघु उद्योगपतियों एवं फुटकर व्यापारियों को ऋण सुविधायें प्राप्त होने लगेंगी।
- राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का काफी विस्तार हुआ। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1969 में ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखाओं की संख्या 1860 थी जो 197 में बढ़कर 13333 हो गई।
- 1969 में 65 हजार जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय था परन्तु 1979 में 17 हजार के लिए 1 बैंक कार्यालय हो गया।
- राष्ट्रीयकृत के पश्चात् सहकारी क्षेत्र के बैंक अपने आपको देश के लिए विकास का एक मुख उपकरण समझने लगे।
राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा प्राथमिकता वाले बैंकों की ऋण सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है। 19 जुलाई, 1969 में लघु उद्योग के लिए दिए गये ऋण की राशि 239.3 करोड़ रुपये थी जो 30 जून, 1982 में बढ़कर 4209 करोड़ रुपये हो गयी। कृषि ऋण जो 1969 में कुल दिए गए ऋण को 8.1% थी 1982 में बढ़कर 16.3% हो गयी।
राष्ट्रीयकरण का मूल्यांकन-
राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति का अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में काफी विकास हुआ है। लेकिन फिर बैंकों की जमाराशियों में संतोषजनक है वृद्धि नहीं हुई है। जैसे इस समय हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 14 प्रतिशत जमाराशियों के रूप में है जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में 41% तथा 69% है। इसके अतिरिक्त बैंकों की सेवा विस्तार में गिरावट एवं जमाराशियाँ प्राप्त करने में प्रतियोगिता तथा कीमत वृद्धि को रोकने की असफलता इत्यादि राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलता के प्रतीक हैं। बैंकों की सफलता के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं-
(1) किसानों तथा अन्य प्रकार के छोटे ऋणियों को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से बैंक की वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार किया जाये।
(2) बैंकों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाय।
(3) बैंकिंग नीति बनाते समय देश में नियोजित ढंग से विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखा जाय।
(4) बैंकों में श्रम सम्बन्धों को मधुर बनाया जाय। अर्थात् कर्मचारी एवं प्रबन्ध के मध्य अनेक प्रकार के विवादों को सरल तथा माधुर्य वातावरण में सुलझाया जाना चाहिए।
(5) बैंकों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इसे राजनीतिक हस्तक्षे से दूर रखना आवश्यक है।
(6) बैंकिंग से सम्बन्धित विषयों पर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए जाने चाहिए।
राष्ट्रीयकृत बैंकों के सफल संचालन के सम्बन्ध में बैंकिंग आयोग ने मुख्यतः पाँच पहलुओं से सम्बन्धित सुझाव दिये हैं- (1) संस्थागत ढाँचा, (2) वाणिज्य बैंकों का पुनर्गठन, (3) बैंकों की कार्य प्रणाली, प्रबन्ध व्यवस्था एवं कार्यकुशलता, (4) वैधानिक सुधार, (5) बैंकिंग से सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान। इन सुझाव के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता ह और इनका देश के आर्थिक विकास में अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- बैंक का उद्गम एवं विकास | बैंक की परिभाषा | बैंकों के प्रकार
- व्यापारिक बैंकों के कार्य | Functions of commercial banks in Hindi
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वर्तमान सुधार | बैंकिंग सुधार के दौर | बैंकिंग सुधार का प्रथम दौर
- साख निर्माण | साख निर्माण के प्रकार | साख निर्माण की प्रक्रिया | साख सृजन के उद्देश्य | साख सृजन की सीमाएँ
- बैंकिंग संगठन | इकाई बैंकिंग | इकाई प्रणाली के गुण | इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोष | शाखा बैंकिग | शाखा बैंकिंग की विशेषताएँ | शाखा बैंकिंग के गुण | शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com