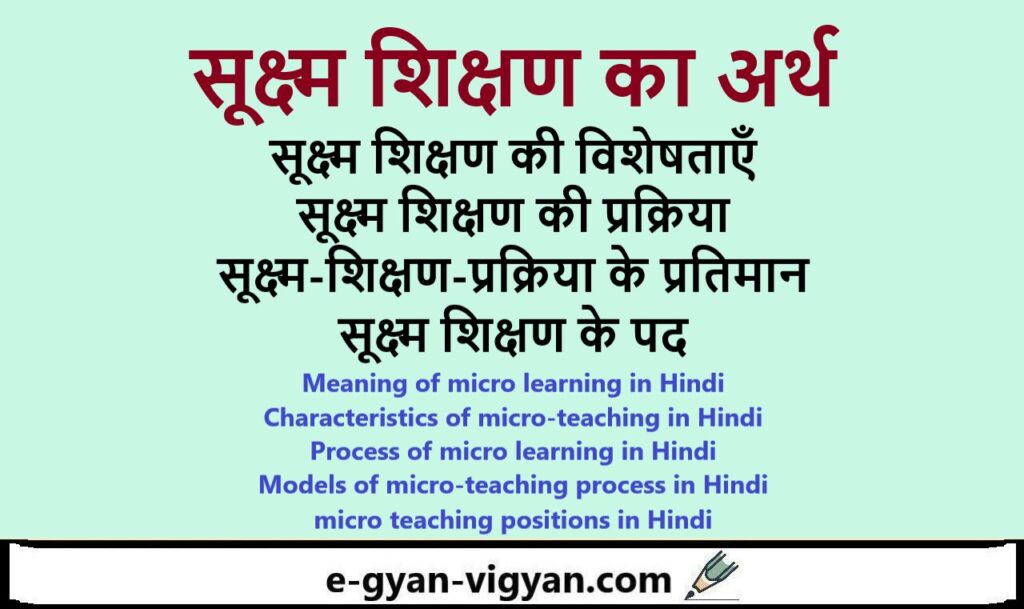
सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ | सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ | सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया | सूक्ष्म-शिक्षण-प्रक्रिया के प्रतिमान | सूक्ष्म शिक्षण के पद | Meaning of micro learning in Hindi | Characteristics of micro-teaching in Hindi | Process of micro learning in Hindi | Models of micro-teaching process in Hindi | micro teaching positions in Hindi
सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ-
सूक्ष्म शिक्षण व्यावहारिक शिक्षण की प्रयोगशास्त्रीय एवं वैश्लेषिक प्रविधि है। यह प्रविधि छात्र शिक्षक में शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है और सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताएँ दूर करने में प्रयुक्त होती है। इसमें शिक्षण को अनेक छोटी इकाइयों में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण अभ्यास की एक नूतन प्रविधि है, जिसके माध्यम से छात्र शिक्षकों को शिक्षण अभ्यास के लिए एक ऐसी प्रविधि प्रस्तुत की जाती है जो कक्षा की सामान्य जटिलताओं को कम करती है और जिसमें छात्र शिक्षक अपने शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया है-
शिक्षा शब्दकोश में सूक्ष्म-शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है-“सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण समागम है, जिसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसके कार्य हैं-
(अ) शिक्षण में प्रारम्भिक अनुभव और अभ्यास के रूप में।
(ब) नियंत्रित दशाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के प्रभाव को खोजने के एक शोध साधन के रूप में।
(स) अनुभवी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण उपकरण के रूप में, जो सामान्यतया 5 मिनट की अवधि के लिए हो, जिसमें 8 छात्रों से अधिक सम्मिलित न हों और बहुधा विश्लेषण के लिए वीडियो टैप अंकित किया गया हो।
डी.डब्ल्यू एलन सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, “सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है, जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है।”
एलन एवं ईव के कथनानुसार- “सूक्ष्म शिक्षण को नियंत्रित अभ्यास की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो नियंत्रित दशाओं के अन्तर्गत शिक्षण अभ्यास तथा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान केन्द्रित करने को सम्भव बनाता है।”
पासी एवं ललिता के शब्दों में- “सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है, जो छात्र शिक्षकों से कम से कम छात्रों को विशिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके केवल एक सम्प्रत्य के शिक्षण की उपेक्षा करती है।”
सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट होता है। कि इस शिक्षण प्रविधि में शिक्षण के सभी पक्षों को लघु अंशों या छोटे से छोटे भागों में विश्लेषित करके शिक्षण का पूर्वाभ्यास कराया जाता है। इसके शिक्षण की प्रभावकारिता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उदाहरणस्वरूप यदि किसी छात्राध्यापक में गणित के सम्बन्ध में शिक्षण कौशल का विकास करना है तो, उसमें निम्नलिखित तथ्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि वह गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाना इत्यादि में निपुण हो। दशमलव का ज्ञान रखता है। लिखावट साफ-सुथरी हो। जोड़-घटाना के क्रमिक पहलुओं के ज्ञान से भिन्न हो। गणित सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियों को रखता हो। इसी तरह अन्य कौशलों का विकास किया जा सकता है।
सूक्ष्म शिक्षण की पूरी क्रियाविधि अत्यन्त सीमित समय में बंधी होती है। उपलब्ध समय के आधार पर शिक्षण की पूरी व्यवस्था नियोजित की जाती है। प्रायः इसमें विषयवस्तु का आकार बहुत छोटा होता है तथा सम्बन्धित विषयवस्तु पर शिक्षण देने की अवधि लगभग 10 मिनट होती है। इसके अलावा छात्र संख्या भी बहुत कम (5 से 10) रहती है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्राय: एक शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। अतएव सूक्ष्म शिक्षण एक नियंत्रित परिस्थिति में लघु शिक्षण देने सम्बन्धी अभ्यास है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी परिसीमाओं से अवगत होते हैं, तदुपरान्त दोषों का निराकरण करके शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण के यथार्थ अर्थ को जानने के लिए विभिन्न शिक्षाविदों की परिभाषाओं से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अतएव प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं निम्नवत् दी गयी हैं- 1. इन साइक्लोपिडीया आफ एजुकेशन- “सूक्ष्म शिक्षण यथार्थ में एक संचरित एवं मिश्रित क्रिया है जिसका इस्तेमाल शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है।”
- एलेन (Allen)- “सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण सम्बन्धी क्रियाओं को छोटे-छोटे भागों में विभक्त करता है।”
- बुश (Bush)- “सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी अध्यापन शैक्षिक तकनीकी है जिसमें छात्रों के एक छोटे से समूह को 5 से 10 मिनट के निश्चित समय में क्रमबद्ध, सुनियोजित अध्यापक क्रिया से तैयार पाठ पढ़ाया जाता है तथा यह स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों को प्रयोग में लाने का मौका देती है, प्राय: वीडियो टेप पर इसका परिणाम देखने का मौका भी मिलता है।”
- मैकनाइट- “सूक्ष्म शिक्षण लघुतम पद वाली वे शिक्षण स्थितियाँ हैं, जिसकी योजना परम्परागत कौशलों में परिमार्जन और नवीन कौशलों के विकास के लिए की जाती है।”
सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ-
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण अभ्यास की नवीन प्रविधि है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
- इसमें कक्षा सीमित होती है। कक्षा में छात्र संख्या 5 से 10 तक होती है।
- शिक्षण अवधि 5 से 10 मिनट तक होती है।
- एक कलांश में एक ही कौशल के शिक्षण पर बल दिया जाता है।
- इसमें छात्राध्यापक की प्रतिपुष्टि तुरन्त ही प्राप्त होती है।
- इसमें अभ्यास प्रक्रिया अधिक नियंत्रित रहती है।
- इसमें छात्राध्यापक को अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, जब तक कि वह उस शिक्षण कौशल के प्रयोग में पारंगत प्राप्त न हो जाये।
सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया-
यह शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगशास्त्रीय प्रविधि है, जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताएँ दूर की जाती है। इसमें एक छात्र-शिक्षक एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए संक्षिप्त विषयवस्तु पर सूक्ष्म पाठ-योजना बनाकर 5 या 10 सहपाठी छात्र-शिक्षकों की छोटी कक्षा को पढ़ाता है। 5 से 7 मिनट तक पढाने के उपरान्त छात्र-शिक्षक पढ़ना बन्द कर देता है। उसे विविध स्रोतों-निरीक्षक या सहपाठी या टेप रिकॉर्डर या वीडियो-टेप आदि से प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के पश्चात् छात्र शिक्षक प्रदत्त सुझावों के आधार पर अपनी पाठ-योजना में संशोधन करके पुनः पाठ नियोजन करता है। तदुपरान्त संशोधित पाठ को अन्य सहपाठी छात्रों (5 या 10) को पुनः पढ़ाता है। इसमें भी पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार एक प्रकार का सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूर्ण हो जाता है।
सूक्ष्म शिक्षण चक्र
पाठ नियोजन → शिक्षण → प्रतिपुष्टि
↑ ↓
पुनः प्रतिपुष्टि ← पुनः शिक्षण ← पुनः पाठ नियोजन
यदि पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पर छात्र-शिक्षक अपने शिक्षण में कमी पाता है, तो पुनः प्रतिपुष्टि में प्रदत्त सुझावों के आधार पर पाठ पुनः पढ़ा सकता है। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलाया जाता है, जब तक कि छात्र-शिक्षक प्रयुक्त शिक्षण कौशल के प्रयोग में दक्ष नहीं हो जाता है। सामान्यतः एक शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए दो सूक्ष्म शिक्षण चक्र एक परम्परागत पाठ के बराबर माना जाता है। एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र 16 मिनट का समय लेता है, जबकि एक परम्परागत पाठ 40 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण में विषयवस्तु का सम्यक ज्ञान देना अथवा विषयवस्तु की किसी इकाई को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है वरन् किसी शिक्षण कौशल को सीखना या दक्षता प्राप्त करना होता है।
सूक्ष्म-शिक्षण-प्रक्रिया के प्रतिमान-
सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रतिमान प्रचलन में हैं-
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित प्रतिमान इस प्रकार हैं-
शिक्षण चरण- 5 मिनट
मूल्यांकन चरण- 10 मिनट
पुनः पाठ निर्माण चरण- 15 मिनट
पुनः शिक्षण चरण- 5 मिनट
पुनः मूल्यांकन- 10 मिनट
कुल समय– 45 मिनट
भारतीय प्रतिमान- हमारे देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, एम. एस. युनिवर्सिटी, बड़ौदा और इन्दौर विश्वविद्यालय के कृत प्रयोगों से सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया है। जो इस प्रकार हैं-
- पाठ नियोजन
- शिक्षण- 6 मिनट
- प्रतिपुष्टि- 6 मिनट
- पुनः पाठ नियोजन- 12 मिनट
- पुनः शिक्षण- 6 मिनट
- पुनः प्रतिपुष्टि- 6 मिनट
योग– 36 मिनट
अन्य विशेषताएँ-
- इसके एक समूह में अधिकतम संख्या 10 तक होती है।
- इसमें पर्यवेक्षक एक या दो होते हैं।
- इसमें शिक्षक अथवा सहपाठी द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है।
- इसमें वीडियो, टेप, क्लोज सर्किट टी.वी. आदि के स्थान पर सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिपुष्टि दी जाती है।
- इसमें सूक्ष्म-शिक्षण प्रक्रिया संरचित परिस्थितियों में सम्पन्न होती है। संरचित कक्षा बी.एड. के छात्राध्यापकों की होती है।
सूक्ष्म शिक्षण के पद-
देश के माध्यमिक विद्यालयों हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यावहारिक प्रशिक्षण के अभ्यास हेतु सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि की संस्तुति की गयी है। अत: इस प्रविधि के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न शिक्षण कौशलों में कम-से-कम 5 शिक्षण कौशलों में प्रत्येक छात्र-शिक्षक को दक्षता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है-
- (अ) सूक्ष्म शिक्षण की समुचित जानकारी- सर्वप्रथम छात्र-शिक्षक को सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, विशेषताएँ, प्रक्रिया एवं गुण-दोष की समुचित जानकारी करायी जाती है। इसे प्रस्तावना पद कहा जाता है।
(ब) समालोचना करने की विधि का ज्ञान- पाठ की समालोचना करने के लिए प्रत्येक छात्र-शिक्षक को विभिन्न शिक्षण कौशलों के अलग-अलग निरीक्षण प्रपत्र तथा मूल्यांकन प्रपत्र प्रदान किये जाते हैं तथा उन्हें उनके समुचित उपयोग का ज्ञान भी करा दिया जाता है।
- प्रमुख शिक्षण कौशलों का ज्ञान- इसके उपरान्त प्रमुख शिक्षण कौशलों के अर्थ, उनके मनोवैज्ञानिक आधार, उनके प्रमुख घटकों का ज्ञान कराया जाता है।
- आदर्श सूक्ष्म पाठ प्रस्तुतीकरण- तत्पश्चात् छात्र-शिक्षकों के समक्ष आदर्श सूक्ष्म पाठ प्रस्तुत किया जाता है। आदर्श सूक्ष्म पाठ प्रस्तुत करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं-
(i) शिक्षक प्रशिक्षक स्वयं आदर्श सूक्ष्म पाठ छात्र-शिक्षकों को समक्ष पढ़ाकर दिखा सकता है।
(ii) शिक्षक प्रशिक्षक एवं आदर्श पाठ छात्र-शिक्षकों को पढ़कर सुना सकता है।
(iii) आदर्श सूक्ष्म पाठ की प्रतियाँ छात्र शिक्षकों को दिखाई जा सकती है।
(iv) शिक्षक प्रशिक्षक आदर्श सूक्ष्म पाठ का टेप रिकार्डर पर बजाकर छात्र-शिक्षकों को सुना सकता है।
(v) आदर्श सूक्ष्म पाठ वीडियो-टेप पर रिकार्ड करके टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है।
- सूक्ष्म पाठ योजना की तैयारी- आदर्श सूक्ष्म पाठ योजना का डिमोन्सट्रेशन एवं निरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने और उनके उपयोग की विधि समझ लेने पर प्रत्येक छात्र-शिक्षक को आदर्श सूक्ष्म पाठ पर आधारित किसी एक शिक्षण कौशल पर सूक्ष्म पाठ योजन तैयार करने को कहा जाता है।
शैक्षिक तकनीकी – महत्वपूर्ण लिंक
- प्रयोजना विधि | प्रयोजना विधि का अर्थ एवं परिभाषा | प्रायोजना विधि के सिद्धान्त | प्रायोजना के प्रकार | प्रायोजना विधि के गुण | प्रायोजना विधि के दोष | प्रायोजना विधि का सोपान
- समस्या समाधान विधि | समस्या समाधान विधि की परिभाषाएँ | समस्या समाधान विधि के सिद्धान्त | समस्या समाधान विधि के गुण | समस्या समाधान विधि के दोष | समस्या समाधान विधि के सोपान | समस्या समाधान व प्रायोजना विधि में अन्तर
- पर्यवेक्षित अध्ययन विधि | पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का अर्थ एवं परिभाषा | पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण | पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के दोष | पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान
- व्याख्यान विधि | व्याख्यान विधि के गुण | व्याख्यान विधि के दोष | व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाये
- शिक्षण प्रतिमान | व्यवहारवाद और ज्ञानात्मक अधिगम के उपगमन का संश्लेषण | व्यवहारवादी और ज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धान्तों में अन्तर
- शिक्षण की प्रकृति | शिक्षण की विशेषताएँ | शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







