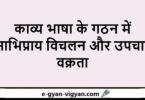रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धान्त | रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धान्त का विश्लेषण
रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धान्त
आई० ए० रिचर्ड्स आधुनिक काव्य-शास्त्रीय परम्परा के प्रतिष्ठित विचारक हैं। इन्होंने अपनी वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि को साहित्य समीक्षा में प्रवाहित कर एक नई आभा को विकीर्ण किया है। ये मनोविज्ञान से साहित्य क्षेत्र में आए हैं, अतः इनकी समीक्षा-दृष्टि मनोवैज्ञानिक तर्कों पर आश्रित है। वैज्ञानिक उन्नति एवं भौतिक समृद्धि के कारण कविता का अवमूल्यन ही नहीं हुआ अपितु उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ा हुआ आभासित होने लगा। कतिपय विद्वानों ने कविता की इस अन्धकारपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान दिया, जिनमें से रिचर्ड्स का स्थान महत्त्वपूर्ण है। रिचर्ड्स ने मानव सभ्यता एवं उसके मानसिक सन्तुलन के लिए कविता की अनिवार्यता घोषित की और यह प्रतिपादित किया कि आज मूल्य-विघटन युग में कविता ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा कर सकती है।
डॉ० भागीरथ मिश्र के अनुसार, ‘रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैण्ड के चेशायर में सन् 1893 ई० में हुआ था। इनकी शिक्षा क्लिफ्टन और कैम्ब्रिज़ में हुई थी। इन्हें कैम्ब्रिज और पेकिंग (चीन) के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति मिली थी। कुछ समय कार्य करने के उपरान्त ये 1944 से 1963 ई० तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर रहे। इनके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्यापन का बड़ा प्रभाव पड़ा। इनके अध्यापन में मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान का विशेष योगदान था। इन्होंने यद्यपि अनेक ग्रन्थ लिखे, पर उनमें से प्रमुख हैं- प्रिंसिपल्स ऑफ रिटोरिक (1936), हाउ टू रीड ए पेज (1942)। रिचर्ड्स ने आधुनिके जीवन में कविता की सन्दर्भता प्रकाश डाला और सम्पूर्ण तथा स्वस्थ मानव-जीवन में काव्य के महत्त्व और मूल्य पर भी विचार किया है। इनका व्यक्तित्व मूलतः एक महान शिक्षक का था। ये सुप्रसिद्ध समालोचक, कवि एवं भाषाविद् थे। इनका निधन 1979 ई० में हुआ था।’
मूल्य सिद्धान्त
रिचर्ड्स के अनुसार मूल्य का मानक मानवीय क्रियाओं के सामान्य मानों से पृथक् नहीं होता। साहित्य एक मानवीय प्रक्रिया है, अतः उसका मूल्य निर्धारण करनेवाले तत्त्व या मान भी वे ही हैं, जो मानवीय क्रियाओं के लिए अपेक्षित हैं। इनके अनुसार काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है। (Art are the supreme form of the communicative activity.) जितनी अधिक संप्रेषणीयता किसी रचना में होगी, वह रचना उतनी ही उत्कृष्ट कोटि की मानी जायगी। इस प्रकार काव्य उसकी प्रभाव क्षमता पर निर्भर है।
मन का अर्थ है—मनोवेगों की क्रियाशीलता। उनकी मान्यता है कि मानव-मन विभिन्न वृत्तियों एवं ऐषणाओं का व्यवस्थित क्रम है। (Mind is a system of impulses.) वहाँ मानवीय वृत्तियाँ उत्तेजना का कार्य भी करती हैं, जिससे सन्तुलन भंग हो जाता है। जब अनेक वृत्तियाँ एकसाथ उत्तेजित होकर मन को मथकर उसे अनुप्रेरित करती हैं, तब मन कार्यरत होकर अधिक मूल्यवान वृत्तियों को तुष्ट करता है तथा पुनः संतुलन की स्थिति को प्राप्त होता है। रिचर्ड्स के अनुसार मन के सन्तुलन की आदर्श. स्था वही होगी, जब आवेग व्यवस्थित होकर एक स्वर हो जायें। मानव-मन में ऐसे समतोलन और असमतोलन बराबर होते रहते हैं। काव्य और कला का मूल्य इसी में है कि वह आवेगों में सन्तुलन स्थापित कर, उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान कर सके।
रिचर्ड्स ने साहित्य में मनोवेगों की महत्ता स्वीकार करते हुए मूल्य विषयक मान्यताओं को भी उन्हीं मनोवेगों के सन्दर्भ में प्रतिपादित किया है। इन्होंने मनोवेगों के दो प्रकार माने-
- प्रवृत्तिमूलक- इसे अनुकूल आकांक्षा भी कहा गया। इसके अन्तर्गत भूख, प्यास वासना, कल्याण, दया आदि।
- निवृत्तिमूलक- इसे प्रतिकूल आकांक्षा भी कहा गया। इसके अन्तर्गत घृणा, विस्तृष्णा तथा पापाचार आदि आते हैं।
मन का स्वभाव है-
अनुकूल आकांक्षाओं की तुष्टि के लिए कार्यरत रहना। इस प्रकार आवेग या आकांक्षाओं की तुष्टि करनेवाली सभी वस्तुएँ मूल्यवान हैं बशर्ते वे महत्त्वपूर्ण आकांक्षाओं को न कुचलें। जो भूख या तृष्णा को सन्तुष्ट कर सके वह अधिक मूल्यवान कहा जायगा। किसी माँग की सन्तुष्टि न होने से अन्य माँगों में विक्षुब्धि उत्पन्न होती है; रिचर्ड्स ने इसी आधार को माँग की महत्ता का सूचक माना है। इन मांगों की संगति एवं व्यवस्था ही जीवन के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के मूल्य को निर्धारित करती है। साहित्य में भी ठीक यही दशा होती है। भावों को उत्पन्न करना ही साहित्य का ‘मूल्य’ नहीं है। उनकी संगति एवं सन्तुलन ही उसका मूल्य है। रिचर्ड्स के अनुसार, ‘कला का मूल्य भी उसी बात में है कि वह हमारे आवेगों में संगति और सन्तुलन स्थापित करे, हमारी अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए।’ संक्षेप में रिचर्ड्स के अनुसार मूल्य सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण मान्यताएं हैं-
- कला अन्य मानव-व्यापारों से सम्बद्ध है, उससे पृथक् अथवा भिन्न नहीं है।
- मानव-क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान है।
- किसी भी मानव-क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह कहाँ तक मनोवेगों में सन्तुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है; वह कहाँ तक हमारी अनुक्रियाओं का उन्नयन करती है, हमारी अभिवृत्तियों का निर्माण करती है।
- कला के द्वारा घटित आवेगों का सन्तुलन कलास्वाद के क्षणों तक ही सीमित नहीं रहता। कला से प्राप्त मुक्त अनुक्रियाओं का परिणाम आगे भी बना रहता है।
जीवनानुभव-
रिचर्ड्स की धारणा है कि जब विभिन्न मानसिक क्रियाएं उथल-पुथल मंचाती हैं तो मन एक विलक्षण जीवनानुभव करता है। इस अवस्था में ही मन सन्तुलित अवस्था की ओर बढ़ता है। कविता इसी मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति मानी जाती है। इसी कारण कविता में कवि स्वेच्छा से विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता, वरन् वह तो किसी निश्चित अवसर पर अपने जीवनानुभव को ही व्यक्त करता है। अतः रिचर्ड कवि के विचारों को महत्त्व न देकर, उसके जीवनानुभव को ही महत्त्व देते हैं, क्योंकि पाठक कवि के विचारों में उलझना नहीं चाहता, वह उसके जीवनानुभव से सहज रूप से जुड़ जाता है, साधारणीकृत हो जाती है। वे सर्जक मस्तिष्क की प्रक्रिया का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण नहीं मानते।
सौन्दर्य-
रिचर्ड्स के अनुसार सौन्दर्य एक विशेष प्रकार का मूल्य है, जिसे वे निरपेक्ष मानते हैं। उनके अनुसार सौन्दर्य विषयनिष्ठ है। इन्होंने बस्तु में सुन्दरता न मानकर व्यक्ति की दृष्टि में सुन्दरता की कल्पना की है। किसी वस्तु को सुन्दर कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी मनःस्थिति का उस पर प्रक्षेपण या आरोप करते हैं। शायद इसी कारण रिचर्ड्स ने सौन्दर्य शब्द के स्थान पर ‘अनुभूति का मूल्य’ शब्द का प्रयोग किया है और इस मूल्य की सत्ता उद्दीपन में न मानकर अनुक्रियाओं में मानी है।
मानव-मन में निरन्तर आवेग उत्पन्न होते रहते हैं। उनमें से कुछ परस्पर सम्बद्ध और अनुकूल होते हैं, जैसे-हर्ष और गर्व, किन्तु कुछ विरोधी और प्रतिकूल होते हैं, जैसे- भय । सौन्दर्य के प्रभाव से इन सभी प्रकार के मनोवेगों में पारस्परिक सामन्जस्य सम्भव होता है-
परन्तु सौन्दर्य विषयक इनकी मान्यता की आलोचना करते हुए परवर्ती विद्वानों ने उसे विषयनिष्ठ घोषित किया है। इनका तर्क है कि काव्य-वस्तु का चयन सौन्दर्य की विषयनिष्ठता को प्रमाणित करता है। अर्थात् विषयगत स्थिति में विषय का महत्त्व ही जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त सुन्दर वस्तु उपभोक्ता पर अपना अमिट प्रभाव डालती है, यह भी सौन्दर्य की वस्तुनिष्ठता का प्रमाण है। फिर भी सौन्दर्य को पूर्णतः विषयनिष्ठ अथवा पूर्णतः वस्तुनिष्ठ मानना उचित नहीं है। दोनों का सत्य एकांगी है।’
कल्पना-
रिचर्ड्स ने कल्पना को कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं माना। उन्होंने इस क्षेत्र में कॉलरिज की मान्यता को ही स्वीकार किया। जहाँ कॉलरिज के अनुसार कल्पना एक ऐसी संयोगिक शक्ति है जो विपरीत और विस्वर गुणों को सन्तुलित करती हैं, रिचर्ड्स के अनुसार वह विभिन्न और विपरीत मनोवेगों तथा अनुभवों में व्यवस्था तथा सन्तुलन उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त रिचर्ड्स ने कल्पना का सर्वोत्कृष्ट रूप उसी को माना है, जिससे विरोधी और अनमेल गुणों का सन्तुलन या विरोध-परिहार होता है। कॉलरिज ने इस रूप को संगीतात्मक आनन्द का बोध करानेवाली कल्पना कहा है—‘The sense of musical delight is a gift of imagination.
रिचर्ड्स ने उस कलाकृति को सर्वोत्कृष्ट माना है, जो विरोधी भावों को व्यवस्थित करने वाली हो।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रिचर्ड्स ने साहित्य का मूल्य अन्य मानव-क्रियाओं के समान माना है। साहित्य का प्रयोजन, उनके अनुसार, न तो मन में शून्य की स्थिति उत्पन्न करना है और न उसे उत्तेजित ही करना है। उसका प्रयोजन तो ऐसी मनःस्थिति है जो सन्तुलित एवं संयोजित होती है।
हिन्दी – महत्वपूर्ण लिंक
- जिस लाहौर देखा ओ जम्याई नई’ का कहानी चित्रण
- उत्सर्ग एकाकी की व्याख्या | रामकुमार वर्मा की एकाकी उत्सर्ग
- तौलिए एकाकी की व्याख्या | उपेन्द्र नाथ ‘अश्क’ की एकाकी तौलिए
- एक वैवाहिक विडम्बना एकाकी की व्याख्या | भुवनेश्वर- श्यामा की एकाकी एक वैवाहिक विडम्बना
- अलंकार सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय | अलंकारवादी आचार्य | काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार सम्प्रदाय की व्याख्या
- डॉ० रामविलास शर्मा की समीक्षा दृष्टि | हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में डॉ० राम विलास शर्मा का योगदान
- रिचर्डस का सम्प्रेषण सिद्धान्त | प्रेषणीयता का अर्थ है | अनुभूति की सम्प्रेषणीयता | सम्प्रेषण की दशा | सम्प्रेषण के तत्त्व | सम्प्रेषण में बाधक तत्त्व
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी | आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि पर विचार
- आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी | स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के सम्बन्ध में आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी की मान्यता | स्वच्छंदतावादी समीक्षा के विकास में आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी के योगदान
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com