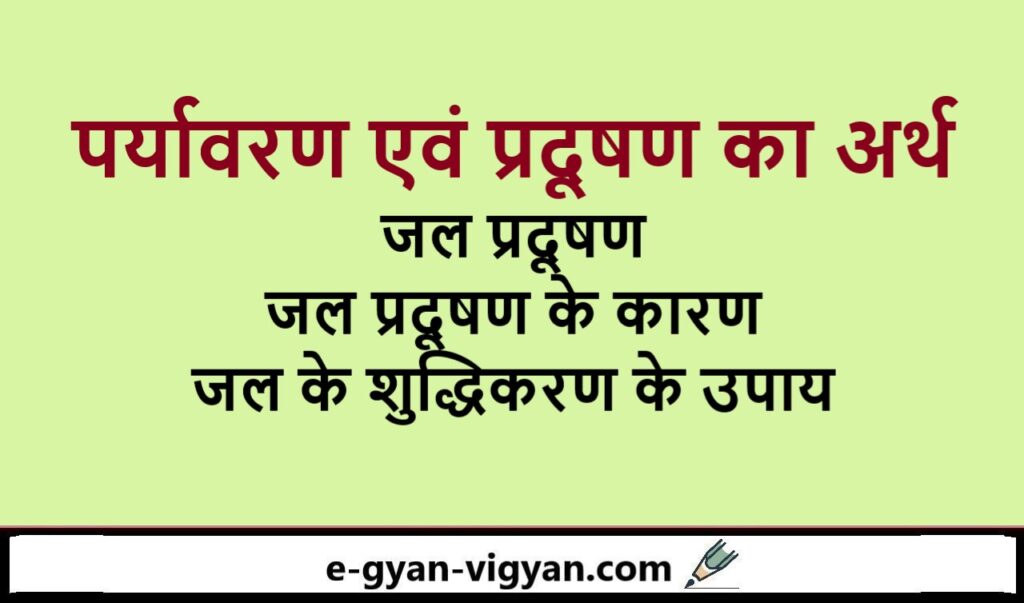
पर्यावरण एवं प्रदूषण का अर्थ | जल प्रदूषण | जल प्रदूषण के कारण | जल के शुद्धिकरण के उपाय | Meaning of environment and pollution in Hindi | Water pollution in Hindi | Causes of water pollution in Hindi | ways to purify water in Hindi
पर्यावरण एवं प्रदूषण का अर्थ
पर्यावरण- पर्यावरण यानि परि+आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ एवं आवरण का अर्थ है किसी चीज से ढके होना। अब दोनों शब्दों के अर्थ को मिलायें-चारों तरफ से ढके होना। अर्थात् वे एभी दिशाएं जो एक व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं तथा चारों ओर से घेरे हुए होती हैं उसका पर्यावरण कहलाती हैं।
मैकाइवर एण्ड पेज ने पर्यावरण को निम्न प्रकार परिभाषित किया है-“भौगोलिक पर्यावरण उन एभी दिशाओं से मिलकर बना है जो प्रकृति ने मानव को दी हैं।’’
प्रदूषण- वातावरण में विभिन्न गैसें निश्चित् अनुपात में उपस्थित रहती हैं परन्तु कभी-कभी वायुमण्डल में एक अथवा अनेक गैसें आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है अथवा कम हो जाता हैं इस कारण वातावरण दूषित हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने पर हमें ऑक्सीजन उचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती है। इस वातावरण के दूषित हो जाने को वायु प्रदूषण कहते हैं।
इसी प्रकार जल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, गैसें, जले हुए शव इत्यादि मिल जाने पर जल दूषित हो जाता है इसे जल प्रदूषण कहते हैं।
इस प्रकार जब प्राकृतिक चीजों में किसी ऐसी चीज को मिला दिया जाता है जिससे वह दूषित हो जाय तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं।
जल प्रदूषण –
जल प्रदूषण के कारण
प्राकृतिक जल जो कि हमें नदी, तालाबों, झरनों आदि से प्राप्त होता है, उसे मनुष्य स्वयं ही दूषित करता रहता है। कूड़ा-करकट, मल, अधजले शव, पशु-शव, औद्योगिक संस्थानों के व्यर्थ पदार्थ आदि बहाने से जल दूषित हो जाता है। इस व्यर्थ पदार्थों में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिन्हें साधारण आंख से नहीं देखा जा सकता है। ये जल को संदूषित कर देते हैं। ऐसा जल स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है।
औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले निरर्थक पदार्थ रासायनिक अवशेषों से भरपूर होते हैं। इनमें अम्ल, क्षार, लवण, तेल, चर्बी तथा अन्य विषैले पदार्थ होते हैं जो जल को दूषित एवं मलिन कर देते हैं। इसी प्रकार शक्कर मिल, कागज मिल, कपड़ा मिल, शराब भट्टियों, चमड़ा तैयार करने तथा रंगने वाले कारखानों आदि के अवशेष पदार्थ और दूषित जल, जल को संदूषित करते हैं।
कीटनाशक औषधियां जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, वे भी जल का दूषित करता हैं।
जल को दूषित होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि सभ्य प्राणी होने के नाते मनुष्य स्वयं में ही विवेकशीलता पैदा करें और जल को दूषित होने से बचायें।
जल और बीमारियाँ-
जहां एक ओर जल जीवन के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर अशुद्ध जल विभिन्न रोगों को फैलाने का सशक्त माध्यम भी है। दूषित जल से उत्पन्न रोगों से प्रतिवर्ष अनेकों व्यक्ति मर जाते हैं। जल से होने वाले प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं-
(क) साधारण गण्डमाला (Simple Goitre)- यह रोग आयोडीन लवण का कमी से होता है। जहां जल में आयोडीन की कमी होती हैं, वहां के निवासियों में यह रोग देखा जाता है। भारतवर्ष के उत्तरी भागों, बिहार तथा गण्डूक नदी के आस-पास बसने वाले व्यक्तियों में यह विशेष रूप से देखा जाता है1
(ख) सीसा धातु विषाक्तता (Lead Poisoning)- जल में सीसा नहीं पाया जाता है लेकिन यदि जल को सीसे के बने पात्रों में लम्बे समय तक संग्रहित किया जाता है तो जल में सीसा घुल जाता है जो जल को विषैला कर देता है। सीसायुक्त जल अस्वाथ्यकर होता है। यह स्नायु-तंत्र को प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति पक्षाघात (Paralysis) का शिकार हो सकता है।
(ग) सल्फेट और पाचन विकार-कठोर जल में सल्फेट लवण की उपस्थिति होता है। इसका नियमित सेवन पाचन विकारों को जन्म देता है।
(घ) ज़ल और जीवाणु तथा कृमिजनित रोग-
(i) एककोशीय: जीवाणुजनित रोग (Protozoal Discases).
एमेबिक डिसेण्ट्री (Amebic Dysentry)
(ii) पराश्रयी कृमिजनित रोग : राठण्ड वर्म (Round Wom).”
थ्रेड वर्म (Thread Wonn)
पिन वर्म (Pin Worm)
(iii) जीवाणुजनित रोग : हैजा,
टायफाइड और पेराटायफाइड,
पेचिश।
(iv) वाइरसजनित रोग (Viral) : संक्रामक यकृत सम्बन्धी रोग
(Infective Hepatitis).
पोलियो,
माइलाइटिस (Polio Myclitis).
जल और जीवाणु- जल में अनेक प्रकार के जीवाणु पाये जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे टायफाइड, अतिसार, परजीवी कृमि, हैजा, पोलियो-माइलाइटिस, आमाशयिक आंत्र शोध अमोबिक पेचिश आदि उत्पन्न करते हैं। जल में पाये जाने वाले जीवाणु और उनसे उत्पन्न रोग निम्नलिखित हैं-
(1) हैजा-विब्रिओं कोलरा (Vibrio Cholera).
(2) बायफाइड-बैसिलस सालमोनेल्ला टायफोसा (Becillus Salmonella Typhosa).
(3) अमीबिक पेचिश
(4) पोलियों माइलाटिस वायरस (Virus),
(5) परजीवी कृमि-थ्रेड वर्म, राउण्ड वर्म, पिन वर्म (Tireadworm. Roundworm. Pinworm).
जल-प्रदूषण निवारण अथवा जल का शुद्धिकरण
(Purification of Water)
अशुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसका नियमित सेवन विभिन्न रोगों को जन्म देकर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अतः पीने योग्य जल का शुद्ध होना परम आवश्यक है। जल के शुद्धिकरण के लिए प्रमुख से दो विधियां प्रयोग में लायो जाती हैं-
(1) प्राकृतिक विधि (Natural Method).
(2) कृत्रिम विधि (Artificial Method).
प्राकृतिक विधि- इस विधि में जल प्राकृतिक रूप से स्वत: ही शुद्ध होता रहता है। जल के विशुद्धीकरण को प्राकृतिक विधियां निम्नलिखित हैं।
(a) वाष्पीकरण (Evaporation)- प्राकृतिक रूप से जल वाष्पीकरण क्रिया द्वारा स्वतः ही शुद्ध होता रहता है। वर्षा का जल वाष्पीकरण का हो उदाहरण है। समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर ही बादल बन जाता है और वर्षा के रूप में शुद्ध होकर पृथ्वी पर आ जाता है।
(b) स्थरीकरण (Sedimentation) – जब जल को किसी बर्तन में भरकर स्थिर रख दिया जाता है तो अशुद्धियां धीरे-धीरे नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर का जल शुद्ध हो जाता है।
(c) ऑक्सीकरण (Oxidation)—वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भी जल को शुद्ध करने का अत्यन्त उत्तम साधन है। वर्षा नदी, तालाब, कुएं सभी का जल निरन्तर वायु के द्वारा ऑक्सीजन के सम्पर्क में आता रहता है। ऑक्सीजन में जीवाणुओं के नष्ट करने की क्षमता होती है जिससे जल की शुद्धि होती है।
(d) स्वतः शुद्धिकरण (Self Purification)- बहते हुये जल में रुके हुए जल की तुलना में अशुद्धियों कम होती हैं। नदियों, झरनों आदि का जल निरन्तर प्रवाहित होता रहता है जिससे अशुद्धियां एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो पाती हैं। अतः निरन्तर प्रवाह से जल स्वत: ही शुद्ध होता रहता है।
(e) भूमि द्वारा (By Soil)- वर्षा के जल का लगभग 25% भाग पृथ्वी द्वारा सुख लिया जाता है। नीचे पहुंचते-पहुंचते या पृथ्वी की विभिन्न परतों से छिन जाता है। अतः भूमिगत जल स्वच्छ होता है।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- शैक्षिक तकनीकी | तकनीकी क्या है | शैक्षिक तकनीकी का अर्थ | शिक्षा तकनीकी की अवधारणायें | शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएँ
- शैक्षिक तकनीकी का स्वरूप | शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएँ | शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य
- शैक्षिक तकनीकी के प्रकार | कठोर उपागम | कोमल उपागम | प्रणाली विश्लेषण
- शैक्षिक तकनीकी का महत्व | भारत में शैक्षिकी प्रौद्योगिकी अभियान | शैक्षिक तकनीकी का शिक्षक के लिए लाभ
- तकनीकी प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन सारणी | Comparative Study Table of Technical Types in Hindi
- शैक्षिक तकनीकी के रूप | व्यवहार तकनीकी | अनुदेशन तकनीकी | शिक्षण तकनीकी | अनुदेशन की रूपरेखा | Types of Educational Technology in Hindi
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







