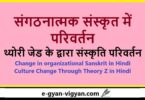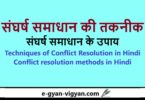परिवर्तनों के प्रतिरोध के कारण | परिवर्तन प्रतिरोध के प्रमुख स्रोत | Reasons for resistance to change in Hindi | Major sources of resistance to change in Hindi
परिवर्तनों के प्रतिरोध के कारण
(Causes of Resistance to Changes)
सांगठनिक परिवर्तन के प्रतिरोध के मुख्य स्रोत उपक्रम के कर्मचारी होते हैं जो वैयक्तिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से परिवर्तन का विरोध करते हैं। परिवर्तन का विरोध मूल रूप से यथास्थिति को बनाये रखने के लिये किया जाता है। पॉल एल० लारेन्स (Paul L- Lawrence) के अनुसार, उत्पादन में निरन्तर गिरावट, संस्था को छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि, स्थानान्तरण हेतु की जाने वाली प्रार्थनायें, लम्बे अर्से से चल रहे विवाद, अनुशासनहीनता, औद्योगिक विवाद आदि परिवर्तनों के प्रतिरोध को को प्रकट करने वाले स्वरूप हैं।
जे० डब्ल्यू० लॉर्च (J.W. Larsch) का कहना है कि व्यक्ति धीरे-धीरे संगठन के साथ एक मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है और कोई भी परिवर्तन जो उस स्थापित सम्बन्ध को तोडता है अथवा तोड़ने की सम्भावना रखता है, व्यक्तियों को अनिश्चितता के वातावरण में खड़ा कर देती है। जे० डब्ल्यू० लॉच (J.W. Larsch) ने परिवर्तनों के प्रतिरोध के निम्नलिखित तीन कारण बतलाये हैं-
(1) मनौवैज्ञानिक सम्बनधों का टूटना- लॉर्थ के मतानुसार, कर्मचारी का संगठन के साथ स्थापित मनोवैज्ञानिक सम्बन्धों का टूटना परिवर्तनों के प्रतिरोध को जन्म देता है। यह मनौवैज्ञानिक सम्बन्ध उस समय टूटा हुआ माना जाता है जब परिवर्तनों को लागू करने से कर्मचारियों को किसी प्रकार का लाभ न पहुंचता हो और न ही कोई लाभ पहुंचने की सम्भावनायें हो। इसके विपरीत सांगठनिक परिवर्तनों से उन्हें किसी प्रकार का लाभ होता हो अथवा लाभ होने की सम्भावनायें हो तो वे प्रतिरोध शक्ति को समाप्त करने में मदद करने लगते हैं और ऐसा परिवर्तनों का समर्थन करते हैं।
(2) योग्यता, दक्षता एवं क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता- लॉर्च का माना है कि कई प्रस्तावित परिवर्तन कर्मचारियों के समक्ष अतिरिक्त योग्यता, दक्षता एवं क्षमता को विकासित करने की आवश्यकता को प्रकट करते हैं। जिससे परिवर्तनों को अपनी वर्तमान योग्यताओं, व्यक्तियों एवं स्थापित कार्य प्रणालियों के विरुद्ध मानते हैं और उनका विरोध करना प्रारम्भ कर देते हैं।
(3) अनिश्चितता के वातवरण की उत्पत्ति- लॉर्च का कहना है कि परिवर्तन की माँग व्यवाहरिक दृष्टि से कर्मचारियों को अनिश्चितता के वातावरण में ला खड़ा करती है जिससे वे परिवर्तनों का प्रतिरोध करना प्रारम्भ कर देते हैं इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी अनिश्चितता कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं से वांचित करने की सम्भावनाओं को प्रकट करती है।
परिवर्तन प्रतिरोध के प्रमुख स्रोत
रिचर्ड के० एलन (Richard K. Allen) की मान्यता है कि संगठन में परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध कहीं भी पैदा हो सकता है जो अनैच्छिक स्वीकृति से लेकर विद्रोह तक के रूप में किसी भी तरह प्रकट हो सकता है। एलन के अनुसार, प्रतिरोध के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं-
(1) स्थायित्व के प्रति रूझान- एलन का कहना है कि व्यक्ति यथा स्थिति को बनाये रखना चाहता है। यथास्थिति को बनाये रखने के पीछे ‘सुरक्षा’ की भावना काम करती है। कर्मचारी यह सोचते हैं कि कहीं परिवर्तन के कारण से वर्तमान में उपलब्ध सुविधायें हमसे छीन नहीं ली जायें। परिवर्तनों का विरोध करने वाले कर्मचारी यह भी कहते है कि संगठन का निर्वाध रूप से सफलता के साथ संचालित करने हेतु उसमें स्थायित्व (Stability) का होना आवश्यक है। वास्तव में यह विचार प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रति नकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं और प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है।
(2) अत्यधिक केन्द्रित शक्ति- जिस संगठन में शक्ति का केन्द्रीयकरण अत्यधिक मात्रा में होता है, वहाँ अधीनस्थों की भागिता के अभाव में परिवर्तन एवं नवाचार सम्बन्धी निर्णय भी उच्च स्तर से ही संगठन में प्रवेश करते हैं। परिणामस्वरूप अधीनस्थ उनका विरोध करने लगते हैं और प्रबंधकों पर यह आरोप लगाते हैं कि परिवर्तन लागू करने से पहले उन्हें पूछा तक नहीं गया।
(3) नवाचार क्रियान्विति की योग्यता का अभाव- एलन के मतानुसार, नवाचारों की क्रियान्विति की योग्यता का अभाव अथवा परिवर्तनों के कारण सांगठनिक असफलता का भय भी परिवर्तनों के प्रतिरोध का स्रोत कारण हो सकता है।
संगठनात्मक व्यवहार – महत्वपूर्ण लिंक
- सीखने की विचारधाराये | सीखने के विभिन्न सिद्धान्त | Theories of Learning in Hindi | different theories of learning in Hindi
- सीखने की परिभाषा | सीखने के संघटक | सीखने के निर्धारक
- सीखने के भेद या प्रकार | सीखने को प्रभावित करने वाले घटक | सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक
- समूह से आशय | समूह की संरचना एवं विशेषतायें | समूह की क्रिया | समूह निर्माण क्यों होता है?
- कार्य समूह का महत्व | कार्य-समूहों का निर्माण कैसे होता है? | कार्य-समूहों का निर्माण क्यों होता है?
- समूह गत्यात्मकता की परिभाषा | समूह गत्यात्मकता की अवधारणा | समूह के विभिन्न वर्ग
- परिवर्तनों के प्रबन्ध की आवश्यकता | सांगठनिक परिवर्तनों के प्रकार
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com