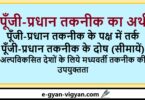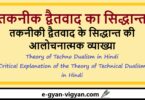दादा भाई नौरोजी के सामान्य आर्थिक विचार | General Economic Thoughts of Dadabhai Naoroji in Hindi
दादा भाई नौरोजी के सामान्य आर्थिक विचार
दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितम्बर, 1825 को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और उनको देश की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं में विशेष रुचि थी। नौरोजी पहले भारतीय थे जिनकी नियुक्ति एलफिन्सटन कालेज, बम्बई में प्रोफेसर के पद पर हुई, जिन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं की नींव डाली, जिनको इंग्लैण्ड की संसद में स्थान प्राप्त हुआ और जो रायल कमीशन के सदस्य थे। सन् 1855 में वे एक व्यापारिक कम्पनी के प्रतिनिध होकर इंग्लैण्ड गये। सन् 1856 में लन्दन यूनिवर्सिटी कालेज में उन्हें गुजराती भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 10 वर्ष तक कार्य किया। वे इंग्लैण्ड में भारतवासियों को एक निवास स्थान प्रदान करने हेतु रुके थे ताकि वे स्वतन्त्रतापूर्वक वहाँ जाकर इण्डियन सिविल सर्विस तथा अन्य सेवाओं में भाग ले सकें। इंग्लैण्ड में विभिन्न ब्रिटिश संस्थानों की कार्य प्रणाली के अध्ययन के पश्चात् उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि ब्रिटिश अपनी परम्पराओं के अनुसार कार्य करें तो वे अवश्य ही भारतवासियों को समान स्तर तथा न्याय प्रदान करेंगे।
अंग्रेजी तथा भारतीयों को भारत से सम्बन्धित विषय पर विचार-विनिमय हेतु एक स्थान पर एकत्र करने के लिए उन्होंने डब्ल्यू० सी० बनर्जी के सहयोग से लन्दन इण्डियन सोसायटी की स्थापना की। दिसम्बर सन् 1886 में उन्होंने ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की नींव रखी। तत्पश्चात् उन्होंने राजनीति में भाग लेना आरम्भ किया और भारत की ओर अंग्रेजों के कर्तव्यों की चर्चा की। ब्रिटिश संसद में अपने भाषणों तथा अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दोषों की ओर ब्रिटिश जनता का ध्यान आकर्षित किया और पूरे उत्साह, देश-प्रेम की भावना, उद्देश्यों की विशुद्धता, पूरी लगन तथा जिज्ञासा से कार्य किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत को वैयक्तिक न्याय प्रदान करने के लिए आवाज उठायी और सन् 1885 में उनके प्रयत्न सफल हुए। जबकि इस विषय पर एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया। इस आयोग ने भी भारत को आशातीत न्याय प्रदान नहीं किया। सन् 1847 में वे बड़ौदा रियायत के प्रधान मन्त्री नियुक्त किये गये और सन् 1892 में वे ब्रिटिश संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। सन् 1886 तथा 1906 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनके आर्थिक विचार हमें उनकी पुस्तक ‘Poverty and Un. British Rule in India’ से प्राप्त होते हैं। ब्रिटिश जनता को उनसे बहुत लगाव था और उन्हें ‘भारत का महान् वृद्ध पुरुष’ (Grand old Man of India) कहते थे। उसके आर्थिक विचार निम्न प्रकार हैं:
निर्धनता की समस्या-
नौरोजी के अनुसार भारत की मुख्य समस्या भारतवासियों की निर्धनता थी। विभिन्न बातों से भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि भारत दिन-प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा था। उदाहणार्थ देश को निम्न आर्थिक आय, निम्न आयात एवं निर्यात, निम्न जीवन-स्तर, सरकार की निम्न आय, ऊँची मृत्यु-दर और निरन्तर उत्पन्न होने वाले अकाल। उनके अनुसार भारत की निर्धनता का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य था। उन्होंने हिसाब लगाया था कि ब्रिटिश इण्डिया की कुल प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष थी और सम्पूर्ण देश में प्रति व्यक्ति जीवन- निर्वाह लागत 34 रुपये थी। उन्होंने आवश्यक आँकड़े एकत्र किये और उनके आधार पर लिखा कि ‘ऐसे भोजन और कपड़े के लिए भी जो कैदी को दिया जाता है, एक अच्छे मौसम में पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता, थोड़ी सी विलासिता और सभी सामाजिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं……. तथा बुरे समय के लिए व्यवस्था करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता…भारतीय जनता की ऐसी स्थिति है। उनको जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी प्राप्त नहीं होता। उनके विचार में भारत की निर्धनता इसी कारण था कि उसका पिछला धन नष्ट हो चुका था और यूरोपीय सेवाओं तथा राष्ट्रीय ऋण पर भी अधिक खर्च किया जा चुका था। उनके अनुसार यह एक ऐसी नाली थी जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था को खाली कर रही थी।
नौरोजी ने बताया कि जो भी युद्ध अंग्रेजों ने 1858 ई० के बाद भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर लड़ा, उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के हितों को सुरक्षित रखना था। इसलिए भारत में ब्रिटिश फौज तथा अन्य सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसमें ब्रिटेन को अपना उपयुक्त हिस्सा देना चाहिए। भारत में रेलों की स्थापना का उदाहरण लेते हुए उन्होंने बताया कि जब इंग्लैण्ड में रेल मार्ग स्थापित किये गये थे तो उनसे प्राप्त सम्पूर्ण आय ब्रिटिश खजाने में जमा होती थी। रेलों के संचालन के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किये गये थे वे अंग्रेज थे और प्रकार रेलों पर किया गया व्यय ब्रिटिश जनता को ही वापस मिल जाता था। अत: अंग्रेजों को ही रेलों के सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हुए थे। किन्तु भारत में स्थिति बिलकुल उलटी है। भारतीय रेलों की स्थापना के सम्बन्ध में जो उच्च अधिकारी नियुक्त किये गये वे इंग्लैण्ड में रहते थे और उनका सारा खर्चा भारतीय रुपये से पूरा किया जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतनों तथा भत्तों का भुगतान भी भारतीय धन में से किया जाता था। केवल थोड़े-से भारतीय ही निम्न पदों पर नियुक्त किये गये थे। इस प्रकार रेलों से भारत को बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ था जबकि विदेशी ऋणों का सम्पूर्ण भार भारत को सहन करना पड़ता था।
विदेश गमन सिद्धान्त-
नौरोजी की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली भारतीयों के लिए विनाशकारी और ब्रिटेन के लिए हितकारक थी। इसी को ‘विदेश गमन सिद्धान्त’ (the drain theory) कहते हैं। इस सिद्धान्त का मुख्य सार यह है कि भारतीय जनता की निर्धनता मुख्यतः ब्रिटिश शासन के कारण है क्योंकि व्यक्तियों पर भारी कर लगा दिये गये थे। यदि करों से प्राप्त होने वाली आय को उसी देश में खर्च कर दिया जाय जिसमें वह एकत्र की गयी है तो धन उसी देश के व्यक्तियों के हाथों में घूमता रहता है आर्थिक क्रिया को बढ़ावा मिलता है और व्यक्तियों की सम्पन्नता में वृद्धि होती है। यदि यह आय किसी अन्य देश को भेज दी जाय तो वह उस देश के लिए सदैव ही नष्ट हो जाता है जिसमें इसको एकत्र किया गया था। इसके करदाता देश में उद्योग तथा व्यापार भी प्रोत्साहित नहीं होते। उनका अनुमान था कि सन् 1900 तक 260 लाख पौण्ड से अधिक धन भारत से बाहर जा चुका था। परिणामत: देश में पूंजी का निर्माण नहीं हो सका था। यही नहीं, उसी धन को वापस लाकर अंग्रेजों ने महत्त्वपूर्ण उद्योगों तक सम्पूर्ण व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इसलिये नौरोजी का विचार था कि यदि देश का सम्पूर्ण उत्पादन देश में नहीं लगाया जाता तो पुनरुत्पादन कठिन हो जायेगा। और उत्पादन की प्रचलित दर पर वार्षिक उत्पादन में से कुछ न कुछ अवश्य ही कम होता चला जायेगा। यह एक प्रकार की दोधारी तलवार के समान थी अर्थात् एक ओर तो पूंजी का हास होता चला जाता है और दूसरी ओर उत्पादन की दर कम होती जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नौरोजी विदेशी पूँजी के उपयोग के विरुद्ध थे। किन्तु यह सत्य नहीं है। वे विदेशी पूँजी का उपयोग कुछ सीमाओं के अन्तर्गत करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि अन्य देशों में अंग्रेज पूँजीपतियों ने केवल अपना धन ही उधार दिया है। ऋणी देश के निवासियों ने उस पूंजी का उपयोग किया और उससे लाभ प्राप्त किये और पूँजीपतियों को ब्याज अथवा लाभ का भुगतान किया। भारत की स्थिति बिलकुल भिन्न थी। अंग्रेजी पूँजीपतियों ने केवल धन ही उधार नहीं दिया बल्कि पूँजी के साथ-साथ देश पर आक्रमण भी किया।
ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की आलोचना-
नौरोजी ने ब्रिटिश शासन-व्यवस्था को कटु आलोचना की। ब्रिटिश संसद में अपने भाषणों द्वारा उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शासन- व्यवस्था के दोषों पर प्रकाश डाला और बताया कि कम्पनी देश के अन्दर व्यापार को नष्ट कर रही थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज देश के विभिन्न मामलों की व्यवस्था अंग्रेजी कर्मचारियों द्वारा कर रहे थे और भारतीयों को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा था। सर विलियम हण्टर ने स्वयं इस तर्क के बल को स्वीकार किया और कहा कि अपने देश के शासन-प्रबन्ध में भारतीयों को अधिकांश जिम्मेदारी देनी चाहिए। नौरोजी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि ब्रिटिश शासन सेकट की कटुता को तीव्र कर रहा था। उनके अनुसार भारत के शरीर पर पिछले आक्रमणकारियों ने जो घाव लगाये थे वे ब्रिटिश शासन-व्यवस्था से और भी गहरे हो गये थे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों का यह दावा कि भारत ने उसके शासन काल में उन्नति की थी, उचित नहीं था। सच तो यह है कि उनके कारण देश नष्ट हो गया था। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यह समझना कि भारत की निर्धनता प्रकृति के प्रकोप के कारण थी, गलत था। वास्तव में, यदि प्रकृति के नियम संचलित होते तो भारत दूसरा इंग्लैण्ड बन गया होता। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ‘यदि भारत में अंग्रेजों के अधीन उन्नति नहीं की तो भारत में उनके अस्तित्व का कोई औचित्य नही है।’ निर्धनता की समस्या को सुलझाने के लिए नौरोजी ने निम्न सुझाव दिये थे।
(1) भारत और इंग्लैण्ड को अपने-अपने देशों में काम करने वाले देशवासियों के वेतनों का भुगतान करना चाहिए। जो अंग्रेज भारत में नौकर हैं और जो भारतीय इंग्लैण्ड में नौकर हैं उनके सम्बन्ध में दोनों देशों की बीच उचित अनुपात निर्धारित होना चाहिए।
(2) क्योंकि अंग्रेजों को अच्छे वेतन दिये जा रहे हैं इसलिए उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
(3) क्योंकि कोई भी देश भारत पर समुद्र से आक्रमण नहीं कर सकता इसलिए भारत को इण्डियन नेवी पर किये गये व्यय में कोई योगदान नहीं देना चाहिए।
भारत की राष्ट्रीय आय-
राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक घटनाओं की व्याख्या के लिए नौरोजी के एकरूपी सिद्धान्त की आवश्यकता पर बल दिया था। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की और उसमें विभिन्न समूहों के हिस्सों को निर्धारित किया। उन दिनों राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े The Indian Economist’ में ही प्रकाशित होते थे। नौरोजी के अनुसार ये आँकड़े अपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इण्डिया से सम्बन्धित प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी अनुमान प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने चाहिए। उनके अनुसार सही स्थिति वह होती जब कुल वास्तविक वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय और अच्छे प्रकार से काम करने की स्थिति में रहने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की वास्तविक गणना की जाती। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 1867-70 ई० के वर्षों में बम्बई प्रेसीडेन्सी में प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताया था। उन्होंने यह भी बताया कि साधारण भारतीयों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 34 रुपयों की आवश्यकता थी: इन आँकड़ों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि धनी तथा मध्य वर्ग के व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त हो रहा था और निर्धन जनता को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भर के लिए भी पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो रही थी। अपनी गणना को नौरोजी ने कृषि उत्पत्ति तथा उद्योगों की उत्पत्ति के मूल्य को सभी व्यक्तियों में बराबर- बराबर अनुपात में विभाजित किया और इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि कृषि उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों में जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनकी वास्तविक संख्या भिन्न-भिन्न थी। इण्डिया आफिस के एक कर्मचारी एफ० सी० डेनवर्स ने इस बात के लिए नौरोजी की आलोचना की। नौरोजी ने देश के कुल उत्पादन की गणना करते समय सेवाओं के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया था। डा० राव ने भी नौरोजी की इस विधि की आलोचना की है। उसके अनुसार नौरोजी का राष्ट्रीय आय सम्बन्धी विचार ‘प्रकृतिवादियों के आय की भौतिकता सम्बन्धी विचार’ पर आधारित था। डा० राव के अनुसार उत्पादक तथा गैर-उत्पादक सामग्रियों सम्बन्धी नौरोजी के विचार अंग्रेज परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के समान है। नौरोजी का विश्वास था कि किसी भी देश का आर्थिक भविष्य उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्रीय आय बढ़ाना आवश्यक है। उनके अनुसार, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, भारत की कुल वास्तविक भौतिक वार्षिक आय कितनी है; दूसरे, सभी प्रकार के व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएँ और साधारण आवश्यकताएँ क्या हैं; और तीसरे, भारत की आय इन आवश्यकताओं के बराबर है या उससे कम अथवा अधिक।
कई स्थानों पर नौरोजी के विचार गत्यात्मक प्रतीत होते हैं। ब्रिटिश संसद में उन्होंने अपने एक भाषण में, वास्तव में, किसी देश के आर्थिक विकास में अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों से सम्बन्धित सिद्धान्त की सम्पूर्ण व्याख्या कर दी थी। उनके अनुसार औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों का हित इसी बात में निहित है कि वे पिछड़े हुए राष्ट्रों की सहायता करें। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के गुणक प्रभाव के सम्बन्ध में उनके विचार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों के समान प्रतीत होते हैं। अन्त में, हम कह सकते हैं कि नौरोजी को उचित ही भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा गया है। ब्रिटिश संसद में अपने भाषणों, इयनोलोजिकल सोसाइटी ऑफ लन्दन तथा ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की सभाओं में उन्होंने भारत तथा भारतीयों की मर्यादा को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया। एक अर्थशास्त्री की हैसियत से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी देश को राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के साधनों को उत्पादकता पर निर्भर करती है। वह पहला भारतीय था जिसने राष्ट्रीय आय की गणना प्रति व्यक्ति के आधार पर की थी। उन्होंने देश की अर्थ- व्यवस्था के लिए राज्य की नीतियों के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला। विदेशी ममन सिद्धान्त उनका मुख्य योगदान था। उन दिनों जबकि साहित्यिक विधियाँ पूर्ण नहीं थीं और विभिन्न आँकड़ें सन्तोषजनक नहीं थे, नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना करके सराहनीय कार्य किया था। एक राष्ट्रवादी, भारतमाता के सुपुत्र और व्यावहारिक अर्थशास्त्री, जिसके सामने देश की समस्याओं का स्पष्ट चित्र था, के रूप में नौरोजी का नाम राष्ट्र के इतिहास में सदैव ही स्मरणीय रहेगा।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- सेन्ट साइमन के आर्थिक विचार | रोबर्ट ओवन के आर्थिक विचारों
- रॉडबर्टस का समाजवाद | रॉडबर्टस के प्रमुख आर्थिक विचार | रॉडबर्टस के विचारों की आलोचना
- पियरे जोसेफ प्रोधों | पियरे जोसेफ प्रोधों के मुख आर्थिक विचार
- कार्ल मार्क्स | मार्क्स का श्रम मूल्य सिद्धान्त | मूल्य सिद्धान्त की आलोचनाएँ
- मार्क्सवाद समाजवाद | मार्क्स एक मौलिक विचारक के रूप में | मार्क्सवाद की विशेषताएँ
- कौटिल्य के आर्थिक विचार | प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएँ
- प्रो० जे०के० मेहता के आर्थिक विचार | प्रो० जे०के० मेहता की पुस्तके | प्रो० जे०के० मेहता द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा | प्रो० जे०के० मेहता की परिभाषा की आलोचनाएँ | Economic ideas of Prof. J.K. Mehta in Hindi
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com