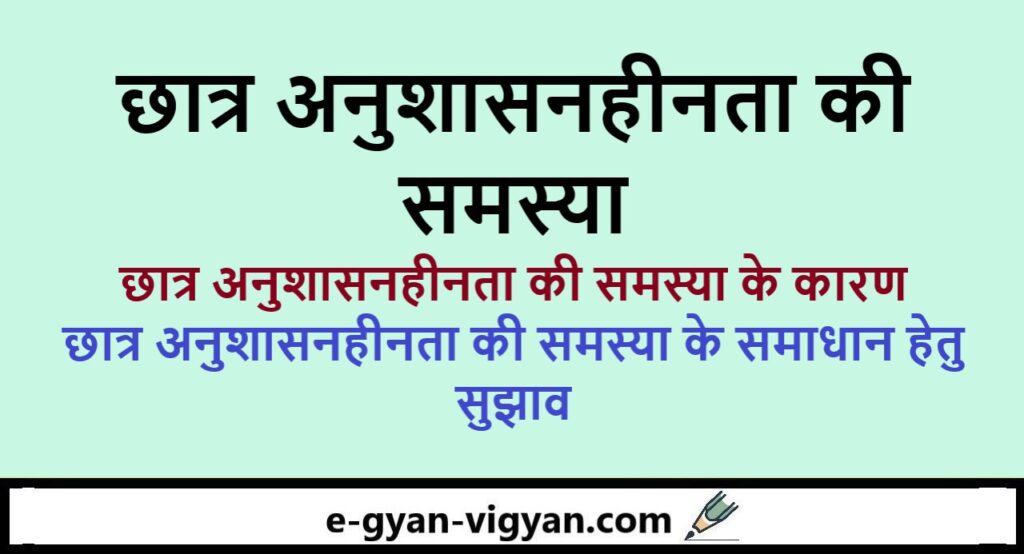
छात्र अनुशासनहीनता की समस्या | छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के कारण | छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान हेतु सुझाव
छात्र अनुशासनहीनता की समस्या
(Problem of Student Indiscipline)
सामान्यतः छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थाओं के नियमों का पालन न करना छात्र अनुशासनहीनता माना जाता है, परंतु अपने वास्तविक अर्थ में इसके अन्तर्गत व्यवहार मानदण्डों और शासन के नियम एवं कानून का न मानना भी सम्मिलित होता है। आज अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्र शिक्षण संस्थाओं के नियमों का न पालन नहीं करते, कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते, कक्षा में शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और छात्राओं के साथ छेड़-छाड़ करते हैं। आए दिन प्रदर्शन, अनशन, हड़ताल और तोड़-फोड़ करते हैं और पुलिस बीच में आती है तो पथराव करते हैं, मरने-मारने को उतारू हो जाते हैं। छात्रों की आपसी दलबन्दी और मारपीट भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता के इतने अधिक रूप हैं कि यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता। समय रहते हुए यदि इस समस्या का समाधान न किया गया तो देश में और अधिक अराजकता फैल जाएगी।
छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के कारण
(Causes of Problem of Student Indiscipline)
स्वतन्त्रता के बाद इस समस्या पर सर्वप्रथम विस्तार से विचार किया ‘राधाकृष्णन कमीशन’ (1948-49) ने। उसने उच्च शिक्षा स्तर पर छात्र अनुशासनहीनता के कारणों को चार वर्गों में अंकित किया-सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक। इसके बाद मुदालियर कमीशन (1952-53) और कोठारी कमीशन (1964-66) ने भी इस समस्या पर विस्तार से विचार किया। इस बीच राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के कारणों और निदान पर विचार करने हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया। कई बार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलनों में भी इस समस्या पर विचार हुआ। इन सबने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता के कारण खोजे उन्हें निम्नलिखित वर्गों में देखा-समझा जा सकता है-
(1) शैक्षिक कारण- अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थाओं का साधन सम्पन्न न होना, शिक्षकों का पूरी तैयारी के साथ शिक्षण कार्य न करना, छात्रों की भारी भीड़, शिक्षक-शिक्षार्थियों में निकट के सम्बन्धों का अभाव, छात्रवृत्तियाँ योग्यता और आर्थिक स्थिति के स्थान पर जाति और धर्म के नाम पर और प्रायोगिक परीक्षाओं में पक्षपात आदि । इससे छात्रों में असन्तोष फैलता है, असन्तोष आक्रोश को जन्म देता है और आक्रोश प्रायः अनुशासनहीनता में बदल जाता है।
2) राजनैतिक कारण-राजनैतिक दबाव से जगह-जगह उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनमें सभी को प्रवेश, उच्च शिक्षा संस्थाओं में राजनैतिक दलों का हस्तक्षेप, उच्च शिक्षा छात्रों का सक्रिय राजनीति में दुरूपयोग, विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा और राज्य सभा में हंगामे की संस्कृति, ये सभी छात्र अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हैं।
(3) प्रशासनिक कारण- उच्च शिक्षा का अनावश्यक विस्तार, लोकतन्त्र के नाम पर खुली प्रवेश नीति यहाँ तक कि अवांछित तत्त्वों को भी प्रवेश। कुलपतियों, प्राचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति का राजनैतिक आधार।
(4) सामाजिक कारण- आज पूरे समाज में अनुशासनहीनता फैली है-परिवार में, पास-पड़ोस में, बैंक और अन्य कार्यालयों में, इस सबका प्रभाव युवक छात्रों पर पड़ता ही है। घर-घर टेलीविजन और टेलीविजन पर यौन एवं मारकाट प्रधान सीरियलों और चलचित्रों का प्रसारण और सर्वत्र हंगामे की संस्कृति आदि भी इस समस्या के मुख्य कारण है।
(5) अन्य कारण- अन्य कारणों में मुख्य कारण हैं- छात्र संघों का निर्माण, शिक्षक संघों का निर्माण, पढ़ने-पढ़ाने के माहौल की कमी और ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठा की कमी।
छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान हेतु सुझाव
(Suggestions for solving the Problem of Student Indiscipline)
प्रायः सभी आयोगों और समितियों तथा तत्सम्बन्धी संगोष्ठियों और सम्मेलनों ने इस समस्या के कारणों के ऊपर विचार के साथ-साथ इसके समाधान के उपाए भी सुझाए हैं । जो निम्न प्रकार हैं-
(1) उच्च शिक्षा संस्थाओं को साधन सम्पन्न किया जाए, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित की जाए, उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने-पढ़ाने का उचित माहौल बनाया जाए। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर की जाए। परीक्षाओं में होने वाले पक्षपात को रोका जाए और यह तभी सम्भव होगा जब प्राइवेट ट्यूशन पर बैन लगाया जाए और अत्यधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की दूसरे पैनल द्वारा परीक्षा की व्यवस्था की जाए।
(2) पूरे समाज में अनुशासनहीनता फैली है परन्तु शिक्षा संस्थाओं में नहीं फैलनी चाहिए। यदि हमने बच्चों को यहाँ अनुशासित कर दिया तो वे समाज में भी अनुशासित रहेंगे और यह तभी सम्भव है जब इनमें केवल मेधावी, योग्य एवं परिश्रमी छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाए और इनमें पढ़ने-पढ़ाने की उचित व्यवस्था हो, उचित माहौल हो। यह भी आवश्यक है कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाए, सबको एक दृष्टि से देखा जाए।
(3) उच्च शिक्षा में खुली प्रवेश प्रणाली के स्थान पर चयनात्मक प्रवेश प्रणाली को अपनाया जाए और केवल मेधावी, योग्य एवं परिश्रमी छात्रों को प्रवेश दिया जाए। शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात 1 : 15 हो जिससे इन दोनों के बीच निकट के सम्बन्ध स्थापित हो सकें । कुलपतियों और प्राचार्यों की नियुक्ति उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ प्रशासनिक कुशलता के आधार पर की जाए।
(4) उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्र संघों के निर्माण पर बैन लगाया जाए, केवल परिषदों का निर्माण हो और परिषदों के माध्यम से साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन हो और समाज सेवा कार्य सम्पादित हों। तब छात्रों के पास अन्यथा आचरण के लिए कोई समय ही नहीं होगा।
(5) शिक्षक और शिक्षार्थियों के सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर बैन लगाया जाए। राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे छात्रों को गन्दी राजनीति में न घसीटें । यदि उच्च शिक्षा संस्थाओं में केवल मेधावी, योग्य और परिश्रमी छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा तो उन पर इन राजनैतिक दलों का प्रभाव ही नहीं होगा, इनकी रैलियों और आन्दोलनों में प्रायः सामान्य छात्र और अवांछित तत्त्व ही भाग लेते हैं।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- नवोदय विद्यालय | नवोदय विद्यालय के उद्देश्य | Navodaya Vidyalaya in Hindi
- भारत में उच्च शिक्षा की प्रगति | ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा का विकास | स्वतन्त्रता के पश्चात् उच्च शिक्षा का विकास
- उच्च शिक्षा में मुख्य समस्यायें | उच्च-शिक्षा की समस्याओं का समाधान
- उच्च शिक्षा का प्रशासन व संचालन | विश्वविद्यालय का आन्तरिक प्रशासन
- उच्च शिक्षा में चुनाव तथा प्रवेश की समस्या | Problem of Selection and Admission in Higher Education in Hindi
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | यू०जी०सी० के कार्य | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य-क्षेत्र
- उच्च शिक्षा के शैक्षिक स्तर की समस्या | उच्च स्तर पर शिक्षा का स्तर गिरने के कारण | शैक्षिक मानकों को ऊँचा उठाने के उपाय
- उच्च शिक्षा के उद्देश्य | उच्च शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व
- उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या | उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या के समाधान हेतु सुझाव
- शिक्षित बेरोजगारी की समस्या | शिक्षित बेरोजगारी के कारण | शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के उपाय
- खुला विश्वविद्यालय | खुले या मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषताएँ व उद्देश्य | खुले या मुक्त विश्वविद्यालयों के लाभ | खुले या मुक्त विश्वविद्यालयों का विकास
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







