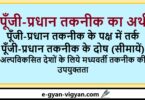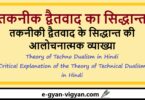भारत में मुद्रा पूर्ति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण | Perspectives on Money Supply in India in Hindi
भारत में मुद्रा की पूर्ति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण-
सुखमय चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट (1985) भारत के सन्दर्भ में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा पर विस्तृत प्रकाश डालती है। रिजर्व बैंक के एक कार्यकारी समूह (Working group) ने 1961 में अपनी रिपोर्ट मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा के सम्बन्ध में दी। इस कार्यकारी समूह द्वारा दी गयी मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा को मुद्रा पूर्ति के शुद्ध बैकिंग सिद्धान्त’ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कुल सम्पत्ति = कुल दायित्व की समता पर आधारित है। इसकी व्याख्या इसके पूर्व हम लोगों ने की। रिजर्व बैंक के इस कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार जो 1964 में प्रकाशित हुयी, मुद्रा की पूर्ति को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है।
Ms=C+D+R जिसमें C= करेंसी, D= व्यापारिक बैंक के साथ माँग जमा तथा R=रिजर्व बैंक के पास संचित कोष।
(क) C या जनता में प्रचलित नकद नोट तथा सिक्के (राजकीय कोषागार तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में रखे हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास के नकद नोट तथा सिक्कों क छोड़कर अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों के नकद तथा मौद्रिक सिक्कें भी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के नकदी कोष को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये नकदी कोष उनके प्रशासनिक कार्यों के फलस्वरूप एकत्रित होते हैं, व्यापारिक कार्यों के फलस्वरूप नहीं उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंकों के पास जो नकदी के रूप में मुद्रा, नोट आदि होते हैं उन्हें मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके जो कोष रिजर्व बैंक में होते हैं उन्हें मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके जो कोष रिजर्व बैंक में होते हैं मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि इन्हें तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाता जब तक कि बैंकों के पास माँग जमा (demand deposits) रहता है, ये कोष बैंकों की तरलता की स्थिति को बनाये रखने के लिए निष्क्रिय रूप में रहते हैं।
(ख) D= अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंकों के बीच जमा तथा सरकारी बैंकों के मॉग जमा-इस सम्बन्ध में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं (1) अनुसूचित बैंक बैक हैं जिनकी प्रदत्त पूँजी तथा कोष 5 लाख रूपये या इससे अधिक है तथा इससे कम पूँजी तथा कोष वाले बैक अनुसूचित बैंक कहे जाते हैं। (ii) दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि मुद्रा पूर्ति के अन्तर्गत माँग जमाओं (ऐसे जमा जिन्हें किसी समय माँग करने पर निकाला जा सकता है) को ही सम्मिलित किया जाता है। सावधि जमा को (fixed deposits) इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योकि (हम देख चुके हैं) माँग जमा ही साख सृजन के आधार होते हैं सावधि जमा इसके आधार नहीं होते। पर आजकल सावधि जमाओं को भी मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया जाने लगा है। (iii) अप्रयुक्त ओवरड्राफ्ट को भी मुद्रा की पूत्रि में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि वास्तविक रूप में ये मुद्रा का कार्य नहीं करते हैं।
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाता नं. 2 में नकदी आदि जो रिजर्व बैंक में रखे रहते हैं , उन्हें निवल रूप में (आय-व्यय के अवशेष) मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया जाता है।
रिजर्व बैंक के इस कार्यकारी समूह के दृष्टिकोण को लोगों ने अत्यन्त ही संकुचित दृष्टिकोण के रूप में लिया। इसके सम्बन्ध में और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए 1977 में एक दूसरे समूह को गठित किया गया। इस समूह ने मुद्रा की पूर्ति का निम्नांकित दृष्टिकोण अपनाया।
जिसमें M1=C+D+R (जैसा 1964 वाली रिपोर्ट में लिया गया था।)।
M2= M1+ डाकघरों तथा व्यापारिक बैंकों के साथ बचत जमायें।
M3= M1+ सभी व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों की समय बचतें।
M4= M3+ डाकघरों तथा बचत संघटनों की सम्पूर्ण जमायें।
अर्थशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- उत्पादन लागत का अर्थ | उत्पादन लागत का महत्व | उत्पादन लागत के प्रकार
- एकाधिकार का आशय | एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण | एकाधिकार के परिणाम
- सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त | सिद्धान्त की मान्यताएँ | सीमान्त उत्पादकता का अर्थ
- लगान की परिभाषा | लगान के रूप | कुल लगान के अंग | आर्थिक लगान एवं ठेका लगान में अन्तर
- रिकार्डो के लगान सिद्धान्त | लगान का स्वभाव | सिद्धान्त की आलोचनाएँ | रिकार्डों के लगान सिद्धान्त का मूल्यांकन
- लगान के आधुनिक सिद्धान्त | आधुनिक सिद्धान्त का आधार | लगान के उदय होने के कारण | रिकार्डियन व आधुनिक लगान सिद्धान्त में तुलना
- वितरण के आधुनिक सिद्धान्त | सिद्धान्त की मान्यताएँ | साधन की माँग | साधन की माँग को प्रभावित करने वाले घटक | साधन की पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक
- नगद मजदूरी एवं असल मजदूरी | असल मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में अन्तर | वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाले तत्व
- मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त | श्रम संघों का मजदूरी पर प्रभाव
- लाभ क्या है? | लाभ के प्रमुख सिद्धान्त | कुल लाभ के अंग | कुल लाभ | शुद्ध लाभ
- कीन्स का ब्याज सिद्धान्त | ब्याज का परम्परावादी सिद्धान्त | ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धान्त
- आधुनिक ब्याज सिद्धान्त | बचत विनियोग वक्र | तरलता पसन्दगी-द्रव्य मात्रा वक्र | ब्याज दर का निर्धारण
- ब्याज का अर्थ | ब्याज के निर्धारण की विधि | ब्याज के निर्धारण के तत्व | ब्याज दरों में भिन्नता के प्रमुख कारण | ब्याज के प्रमुख प्रकार | शुद्ध एवं सफल ब्याज में भेद
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com