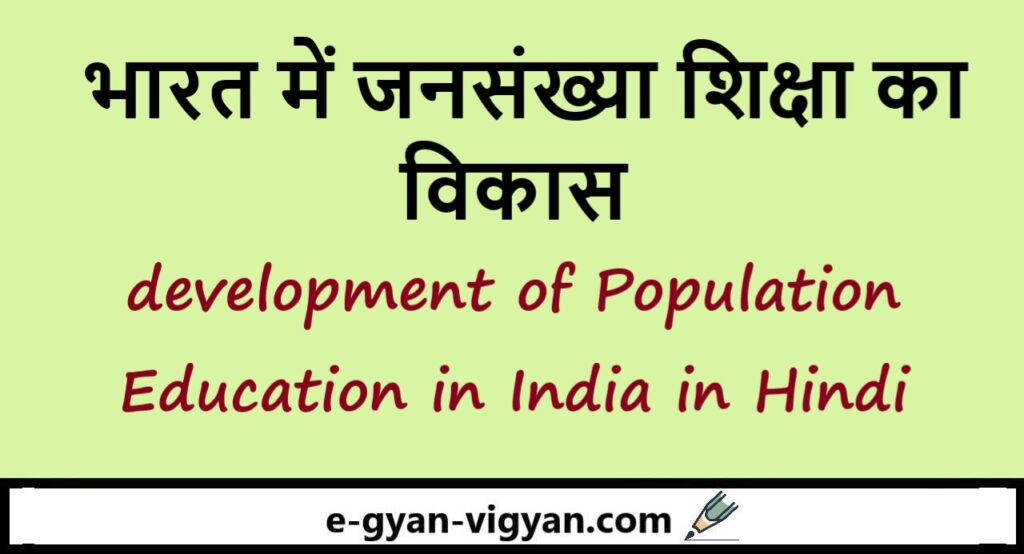
भारत में जनसंख्या शिक्षा का विकास | development of Population Education in India in Hindi
भारत में जनसंख्या शिक्षा का विकास
(Development of Population Education in India)
इस ओर सर्वप्रथम ध्यान 18वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के एक पादरी माल्थस का गया था। उनके बाद अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या का अध्ययन शुरू किया और यह अर्थशास्त्र की विषयवस्तु बन गया। पर जब संसार की जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़नी शुरू हुई तो उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। अतः अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ राजनीतिज्ञों का ध्यान भी जनसंख्या नियन्त्रण की ओर गया। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के छठे दशक में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और शिक्षा आयोजकों ने कदम रखा। उन्होंने जनसंख्या नियन्त्रण के लिए बच्चों को प्रारम्भ से ही जनसंख्या सम्बन्धी ज्ञान कराने और उनमें जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति अभिवृत्ति का विकास करने पर बल दिया। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्लोन आर वेलैण्डेन ने इसे जनसंख्या शिक्षा की संज्ञा दी।
जहाँ तक भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात है, प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के दौरान 1952 में हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम (Family planning Programme) शुरू किया गया। 1961 की जनगणना ने सरकार को और सावधान कर दिया और उसने परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार कार्य को गति देना शुरू किया। पर जनसंख्या नियन्त्रण के लिए जनसंख्या शिक्षा पर सर्वप्रथम विचार 1969 में ‘फैमली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया’ द्वारा मुम्बई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। इस सम्मेलन में जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव सामने आए-
(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) में जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ (Population Education Cell) का गठन किया जाए जो पूरे देश के लिए जनसंख्या शिक्षा के स्वरूप और उसकी कार्यविधियों को निश्चित करे और इस क्षेत्र में केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों का मार्ग-निर्देशन करे।
(2) यह शिक्षा इस प्रकार की हो कि बालक यह समझें कि छोटा परिवार सुख का सार होता है, परिवार के आकार को निश्चित किया जा सकता है और परिवार, समुदाय, राष्ट्र और समूचे संसार के हित के लिए परिवार का आकार छोटा होना आवश्यक है।
(3) सभी स्तर की विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में जनसंख्या-शिक्षा को स्थान दिया जाए।
(4) जनसंख्या-शिक्षा की सामग्री तैयार की जाए, पुस्तकें तैयार की जाएँ और उसके पढ़ाने तथा मूल्यांकन की विधियाँ विकसित की जाएँ।
इस सम्मेलन के सुझाव पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद में जनसंख्या प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इस प्रकोष्ठ ने 1971 में जनसंख्या-शिक्षा पर दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिए गए-
(1) प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक बच्चे पढ़ते हैं, इन्हें सुखी परिवार के बारे में सामान्य जानकारी दी जाए। यह जानकारी भाषा और सामाजिक विषयों में तत्सम्बन्धी प्रकरण जोड़कर दी जा सकती है।
(2) माध्यमिक स्तर पर बच्चों को भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और गणित विषयों के साथ-साथ जनसंख्या-शिक्षा दी जाए।
(3) उच्च प्राथमिक स्तर पर आते-आते बच्चे और समझदार हो जाते हैं। इस स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विषयों के साथ-साथ जीव विज्ञान में भी तत्सम्बन्धी प्रकरण जोड़े जाएँ और बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए।
(4) विद्यालय से बाहर के युवकों को जनसंख्या के प्रति सचेत करने हेतु विद्यालय सामुदायिक केन्द्रों के रूप में कार्य करें।
(5) सभी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में जनसंख्या-शिक्षा की पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों का समावेश किया जाए और एम. एड. स्तर पर इसे विशेष अध्ययन के रूप में जोड़ा जाए।
(6) विभिन्न प्रान्तों के माध्यमिक बोर्डों को भी इस कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहिए।
(7) एन. सी. ई. आर. टी. को इस सबके लिए शीघ्रातिशीघ्र पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए और प्रान्तीय शिक्षा संस्थानों (SIES) के सहयोग से उसे सभी प्रान्तों में लागू करना चाहिए।
और तभी से हमारे देश में जनसंख्या-शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होने लगा। 1974 में एन. सी. ई. आर. टी० ने जनसंख्या-शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया और उसे केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों के पास भेजा। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इसे अपनी सुविधानुसार लागू भी किया । 1980 में एन. सी. ई. आर. टी. ने इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण कराया और यह पाया कि कुछ प्रान्तों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और गृह विज्ञान के साथ कुछ ऐसे प्रकरण जोड़ दिए गए हैं जिनसे बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।
1980 में जनसंख्या-शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वित्तीय सहायता और यूनेस्को की तकनीकी सहायता से राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा परियोजना (National Population Education Plan, NPEP) शुरू की गई। इस समय यह योजना एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है। प्रारम्भ में तो जनसंख्या-शिक्षा स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में ही जोड़ी गई, लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान इसे अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा से भी जोड़ दिया गया। प्रारम्भ में केवल 12 विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा केन्द्र खोले गये उसके बाद अन्य कई विश्वविद्यालयों में खोले गए।
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- खुला विश्वविद्यालय | खुले या मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषताएँ व उद्देश्य | खुले या मुक्त विश्वविद्यालयों के लाभ | खुले या मुक्त विश्वविद्यालयों का विकास
- पर्यावरण शिक्षा का अर्थ | पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य | पर्यावरण शिक्षा : आवश्यकता एवं महत्व | पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र
- छात्र अनुशासनहीनता की समस्या | छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के कारण | छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान हेतु सुझाव
- विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की समस्या | विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की समस्या के कारण | विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की समस्या के समाधान हेतु सुझाव
- छात्र आक्रोश की समस्या | छात्र आक्रोश की समस्या के कारण | छात्र आक्रोश की समस्या के समाधान हेतु सुझाव
- उच्च शिक्षा में अन्तर विद्या अभिगमन की धारणा | भारतीय शिक्षा पद्धति की असमर्थता | शैक्षिक असमर्थता को दूर करना | अन्तर विद्या अभिगमन का सम्प्रत्य | अन्तर विद्या अभिगमन कार्यक्रम
- पर्यावरण शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य | भारत में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता
- पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम के आधारभूत बिन्दु | पर्यावरण शिक्षा : पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक आधार
- पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु | subject matter of environment education curriculum in Hindi
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







