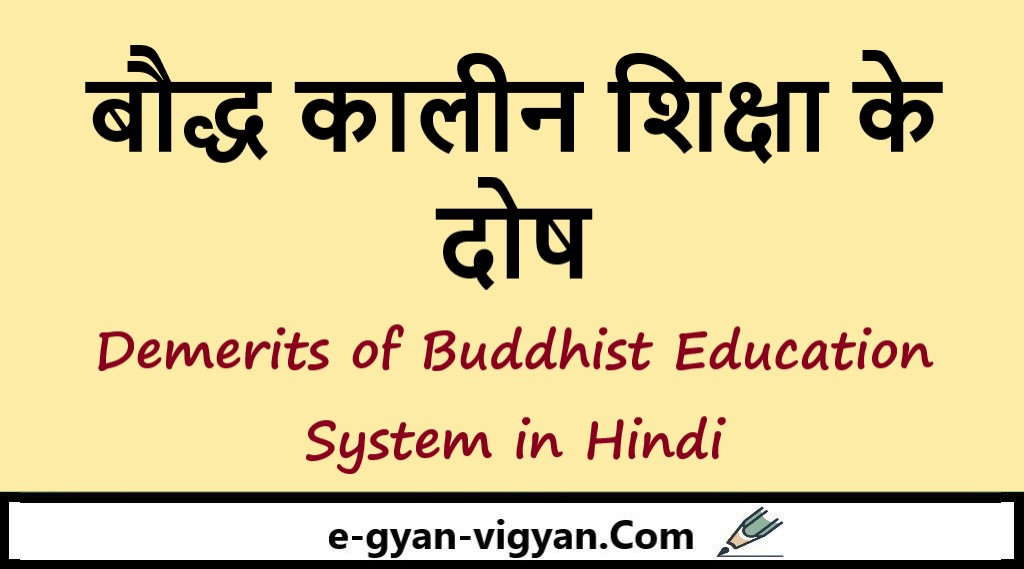
बौद्ध कालीन शिक्षा के दोष | Demerits of Buddhist Education System in Hindi
बौद्ध कालीन शिक्षा के दोष (Demerits of Buddhist Education System)
बौद्धकालीन शिक्षा में उत्पन्न दोषों का उल्लेख निम्न प्रकार है-
(1) हस्तकार्यों की अवहेलना-
बौद्ध काल में शिक्षा का आधार धर्म होने के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रमुखतः धार्मिक शिक्षा को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों को समाविष्ट किये जाने पर भी, इन विषयों की प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक शिक्षा का विकास इस युग में नहीं हो सका था। इसलिए इस काल की शिक्षा आर्थिक दृष्टि से समुन्नत समाज के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे सकी । इसलिए उन्नतशील समाज हेतु बौद्धयुगीन शिक्षा अरुचिकर एवं आकर्षणविहीन हो गई,जबकि वास्तविकता यह थी कि इस काल में शिक्षार्थियों को शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् अनिवार्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना होता था। इसलिए शिक्षार्थियों को अपने परिश्रम से अर्जित धन की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जनसामान्य की आर्थिक विकास की दृष्टि से इसमें कोई रुचि एवं आकर्षण नहीं था। डॉ० एम० सी० सिंघल के शब्दों में हस्तकार्यों को निम्न समझा जाने लगा, जिससे उच्चवर्गीय व्यक्तियों ने इसे पूर्णतः छोड़ दिया। इस तरह परिश्रम की महत्ता की भावना का विकास हुआ।”
(2) धार्मिक विचारों का बाहुल्य-
बौद्धयुगीन शिक्षा का आधार धर्म था। अतः इस काल में बौद्ध धर्म दर्शन एवं साहित्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। इसलिए भौतिक विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। बौद्ध काल में शिक्षार्थियों का मुख्य कर्त्तव्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं तथा उपदेशों का श्रवण,मनन एवं पालन करना था । इसके अतिरिक्त इस युग में शिक्षार्थियों की स्वतन्त्र चिन्तन करने की शक्ति का भी ह्रास हुआ।
(3) बौद्ध मठों का पतन-
बौद्ध काल में मठ ही शिक्षा के केन्द्र थे। इन मठों का संचालन केन्द्रीय सत्ता द्वारा होता था। प्रारम्भ में बौद्ध धर्म अत्यन्त सरल था लेकिन कालान्तर में इसमें अनेक दोष आ गये थे। धर्म सरलता के स्थान पर जटिलता, मिथ्याचार ओर में आडम्बर का साम्राज्य स्थापित हो गया था। महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया था । परन्तु कालान्तर में उनके अनुयायी व्यभिचारी और चरित्रहीन हो गये । बौद्ध मठ व्यभिचार के केन्द्र बन गये। भिक्षुणियों के विहारों में रहने से विहारों की पवित्रता नष्ट हो गई। यह विहार विषय-वासना और विलासप्रियता के केन्द्र बन गये। इसका शिक्षा पर गहन प्रभाव पड़ा। विषय-वासना एवं विलासप्रियता में लुप्त रहने के कारण भिक्षुगण शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में अक्षम हो गये।
(4) सैनिक एवं विज्ञान शिक्षा की अवहेलना-
अहिंसा प्रधान धर्म होने के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने युद्ध की कल्पना करनी भी छोड़ दी। इसलिए इस युग में सैनिक एवं विज्ञान शिक्षा की अवहेलना की गई। यह इसी का परिणाम था कि पाँचवीं शताब्दी में हूण जाति के राजाओं ने बौद्ध मठों में आग लगा दी तथा बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला । हूणों के पश्चात् मुसलमानों ने भारत पर लगातार आक्रमण किये और भारत की प्रगति को गहरा धक्का पहुँचाया।
(5) स्त्री शिक्षा की अवहेलना-
बौद्ध युग में स्त्री-शिक्षा का दायित्व भिक्षुणियों का था। ये भिक्षुणियाँ स्त्री-शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम बनाने में असफल रहीं। इसी के फलस्वरूप शिक्षा केवल धनी एवं कुलीन वर्ग की स्त्रियों तक ही सीमित रही। डॉ० अल्तेकर के अनुसार स्त्रियों में संघ में प्रवेश करने की आज्ञा ने नारी शिक्षा को विशेषतः समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों की नारियों की शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया।” सामान्य वर्ग की स्त्रियों को शिक्षित करने हेतु बौद्ध मठों ने किसी भी प्रकार का प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। कालान्तर में बौद्ध मठ व्यभिचार, विषय-वासना और विलासप्रियता के केन्द्र बन गये और स्त्री शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना हो गई। डॉ० अल्तेकर के शब्दों में-“बौद्ध धर्म में नारी शिक्षा को किसी तरह की प्रेरणा प्राप्त न हो सकी।”
(6) सांसारिक जीवन की उपेक्षा-
बौद्धकालीन शिक्षा में सांसारिक जीवन की पूर्ण उपेक्षा की गई। इस दिशा में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत धार्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के विषयों को समाविष्ट किया गया था। लेकिन फिर भी बौद्धकालीन शिक्षा धर्म प्रधान थी जिसका उद्देश्य था-शिक्षार्थियों को निर्वाण (मोक्ष) एवं बौद्ध धर्म का प्रसार-प्रचार करने योग्य बनाना। इस काल की शिक्षा में लौकिक जीवन से सम्बन्धित विषयों को व्यापक एवं व्यावहारिक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बौद्धयुगीन शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत 20 वर्ष की आयु में शिक्षार्थी का उपसम्पदा संस्कार किया जाता था। इस संस्कार के सम्पन्न होने के पश्चात शिक्षार्थी आजीवन भिक्षु के रूप में बौद्ध संघ में रहने लगता था। इस सम्बन्ध में डॉ० एफ० ई० केई ने लिखा हैकि-“बौद्ध धर्म ने जीवन का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जिसमें इस नश्वर संसार हेतु घृणा थी तथा इस धर्म ने शिक्षा द्वारा व्यक्ति को दूसरे संसार हेतु तैयार किया।”
शिक्षाशास्त्र – महत्वपूर्ण लिंक
- प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य | आधुनिक भारत में वैदिक शिक्षा के उद्देश्य
- वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था | वैदिक काल में शिक्षण विधियां | वैदिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
- वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य सम्बन्ध | Teacher-Student Relation in Vedic Period in Hindi
- प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली | वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र
- उत्तर वैदिककालीन शिक्षा | ब्राह्मणकालीन शिक्षा के उद्देश्य | उत्तर वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं
- वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख तत्व | वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं
- वैदिककालीन और उत्तर वैदिककालीन शिक्षा की तुलना
- प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा | Vocational Education in Ancient India in Hindi
- उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य गुण | उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के दोषों
- बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था | बौद्धकालीन शिक्षण विधियाँ
- बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य | बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ
- बौद्धकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य | Important facts of Buddhist education in Hindi
- वैदिक शिक्षा प्रणाली एवं बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण
- बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा केन्द्र | Buddhist major education center in Hindi
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







