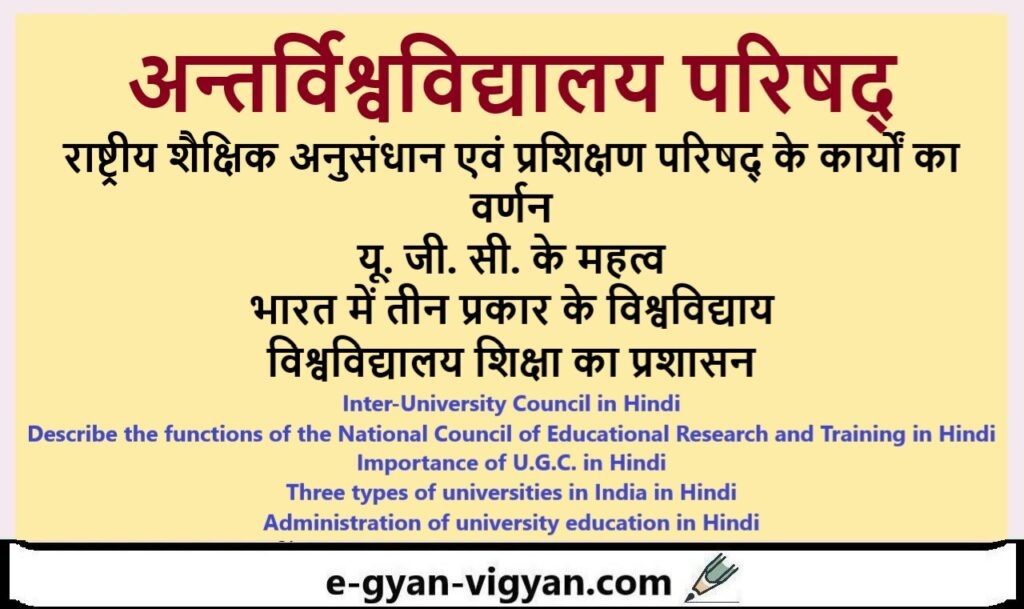
अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद् | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्यों का वर्णन | यू. जी. सी. के महत्व | भारत में तीन प्रकार के विश्वविद्याय | विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन | Inter-University Council in Hindi | Describe the functions of the National Council of Educational Research and Training in Hindi | Importance of U.G.C. in Hindi | Three types of universities in India in Hindi | Administration of university education in Hindi
अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद्
अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद् सन् 1924 में शिमला में स्थापित किया गया था। इस परिषद् को भारतीय विश्वविद्यालय संघ भी कहा जाता है। यह परिषद् विश्वविद्यालयों में कुछ स्तरों तथा आचरण संहिता के प्रवर्तन एवं समस्याओं के निराकरण हेतु, मंच उपस्थित करता है। यह परिषद् निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है।
- यह परिषद्ः विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी सरकार तथा जनता तक पहुंचाता है।
- यह परिषद् विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को विचार-विमर्श करने हेतु मंच का निर्माण करता है।
- इस परिषद् का प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सरकार को सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श करने हेतु स्त्रोत प्रदान करना है।
- इस परिषद् का दूसरा प्रमुख कार्य विश्वविद्यायों के स्तर निर्माण एवं निर्धारण हेतु नियमों का निर्माण करना और उन्हें संचालित करना है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्यों का वर्णन
इस परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं-
- यह परिषद् विद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय को परमर्श देता है।
- यह परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से निकटतम सम्पर्क बनाये रखता है। जिससे शिक्षा सम्बन्धी अनेक समस्यओं को हल करने में सुविधा रहती है।
- यह परिषद् शिक्षा विभागों के माध्यम से विद्यालयीय शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अत्यधिक विस्तार का कार्य करती हैं।
- इस परिषद् का मुख्य कार्य विद्यालयीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों में तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना है।
- इस परिषद् का एक दूसरा प्रमुख कार्य स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधानों की जनता को जानकारी देने के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा साहित्य को प्रकाशित करना है।
- यह परिषद् शिक्षा मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालित भी करता है।
परिषद् के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे एक ऐसे एजेन्सी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो विद्यालयीय शिक्षा में सुधार हेतु राष्ट्रीय विद्यालय तथा राष्ट्रीय स्तर शिक्षा बोर्डों के शिक्षा विभागों तथा राज्य शिक्षण संस्थानों जैसे ऐजेन्सियों के साथ मिलकर उनके माध्यम से कार्य करें।
यू. जी. सी. के महत्व
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का महत्व- वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से विश्वविद्यालय शिक्षा की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। अयोग ने अध्यपकों के वेतनक्रम पर सुधार कर नवीन वेतनक्रम कर सुझाव दिया है। आयोग छात्रावासों तथा अध्यापकों के निवास सम्बन्धी समस्या के हल के लिए भी अनुदान देने के पक्ष में है। वास्तव में आयोग की स्थापना उच्च शिक्षा के लिए वरदान है।
भारत में तीन प्रकार के विश्वविद्याय हैं-
- केन्द्रीय विश्वविद्यायल (Central University)- इस प्रकार के विश्वविद्यालय केन्द्र शासित होते हैं तथा इनके प्रबन्ध एवं व्यय का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर होता है। इनकी संख्या 10 है।
- राज्य विश्वविद्यालय (State University) – ये विश्वविद्यालय राज्य शासित होते हैं और इनके प्रबन्ध एवं व्यय का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर होता है।
- विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएँ (Institutions of Deemed to be University)- भारत में इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना विश्वविद्यालय की अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत की गयी है। वर्तमान सयम में इस प्राकर की संस्थाओं की संख्या 28 है तथा 89 डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाएँ भी हैं।
विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन
विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन सीनेट या कोर्ट द्वारा होता है। सीनेट के सदस्य मनोनीत पदेन या निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्यों की पूर्ति प्रादेशिक शासन कालेजों के प्रधानाचार्यों तथा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के अध्यापक अपने-अपने निर्वाचन से सदस्यों का चुनाव करते हैं। सभी प्रकार के सदस्य एक निश्चित संख्या में रहते हैं।
इसके बाद प्रशासन की दूसरी कड़ी में एकेडेमिक काउन्सिल तथा सिन्डीकेट होते हैं। इसका सम्बन्ध शैक्षिक संस्थाओं से होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज या विभिन्न पाठ्यक्रम की सतितियाँ होती हैं।
प्रकाशन, परीक्षा खोज, शारीरिक शिक्षा, युवा कल्याण खेलकूद, पुस्तकीय, छात्रावास आदि की समस्याओं पर विचार करे के लिए समितियाँ गठित की जाती हैं।
विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति होता है। कुलपति के बाद दूसरा स्थान उपकुलपति का होना है।
शैक्षिक तकनीकी – महत्वपूर्ण लिंक
- शिक्षण प्रतिमान | व्यवहारवाद और ज्ञानात्मक अधिगम के उपगमन का संश्लेषण | व्यवहारवादी और ज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धान्तों में अन्तर
- शिक्षण की प्रकृति | शिक्षण की विशेषताएँ | शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक
- सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ | सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ | सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया | सूक्ष्म-शिक्षण-प्रक्रिया के प्रतिमान | सूक्ष्म शिक्षण के पद
- सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति | सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख सिद्धान्त | शिक्षण कौशल | सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य | सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा एवं महत्त्व
- विद्यालयी कम्प्यूटर साक्षरता | अध्ययन परियोजना | रेखीय एवं अरेखीय कम्प्यूटर | कम्प्यूटर के लाभ | कम्प्यूटर सहअनुदेशन की विशेषताएँ | कम्प्यूटर सहअनुदेशन की शैक्षणिक उपयोगिता | शिक्षा में कम्प्यूटर | कम्प्यूटर सह-अनुदेशन के रूप में | कम्प्यूटर सह-अनुदेशन में आवश्यक विशेषज्ञ | कम्प्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया
- यू. जी. सी. की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | यू. जी. सी. की स्थापना एवं संगठन | यू. जी. सी. की वर्तमान संरचना
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका
Disclaimer: e-gyan-vigyan.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है। हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है। यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- vigyanegyan@gmail.com







